यह लेख 2003 में विनायक दामोदर सावरकर के पोट्रेट के अनावरण पर है, पहले भारतीय संसद के परिसर में और फिर, दो महीने बाद, महाराष्ट्र विधानसभा में। इसे कम्युनलिज्म कॉम्बैट में अप्रैल 2003 में प्रकाशित किया गया था। जाने-माने इतिहासकार अनिल नौरिया द्वारा लिखित यह लेख व्यक्ति और उसकी राजनीति दोनों के बारे में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
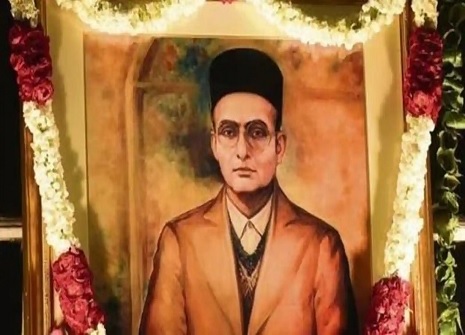
पोर्ट्रेट एज़ मिरर (अप्रैल 2003 वर्ष 9, संख्या 86, कम्युनलिज्म कॉम्बैट)
फरवरी 2003 में यह भारतीय संसद थी; अब,अप्रैल 2003 में, यह महाराष्ट्र राज्य विधानसभा है। इन दोनों पवित्र परिसरों में अब विनायक दामोदर सावरकर का चित्र लटका हुआ है। एक व्यक्ति जिसका महात्मा गांधी की हत्या में हाथ था, वह भारत के पूर्व उप प्रधान मंत्री और गृह मंत्री सरदार पटेल से की बराबरी पर था; एक ऐसा व्यक्ति जिसका भारत के लिए सपना एक ऐसे सैन्यीकृत हिंदू राष्ट्र का था जो प्रतिशोध और बहिष्कार की राजनीति से गढ़ा गया था। हम यहां मेनलाइन मीडिया के दो लेखों को पुन: प्रस्तुत कर रहे हैं जो इस अत्यधिक परेशान करने वाले घटनाक्रम पर गंभीर सवाल उठाते हैं। इस मुद्दे पर अधिक विस्तृत प्रलेखन के लिए, पाठकों से अनुरोध है कि हमारी वेबसाइट www.sabrang.com पर विजिट करें)।
26 फरवरी को राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा वीडी सावरकर के एक चित्र का संसद में अनावरण किया गया। दरअसल सत्ता पक्ष, केंद्र सरकार और इस प्रकरण में शामिल संवैधानिक पदाधिकारियों की मुश्किलें अभी शुरू ही हुई होंगी। निहितार्थ भारत में सरकार के भविष्य के पाठ्यक्रम को छूते हैं। इस मुद्दे का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ वर्गों की भूमिका पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चित्र प्रकरण ने उनके लिए भी एक दर्पण के रूप में काम किया है।
महात्मा गांधी की हत्या में सावरकर की संलिप्तता और कुछ अन्य मुद्दों पर तथ्यों को सार्वजनिक डोमेन में लाने के बाद, अधिकारियों के पास तीन विकल्प थे। पहला था माफ़ी माँगना और उस रास्ते से लौट जाना जिस पर वे चल पड़े थे। दूसरा समारोह को स्थगित करना और तथ्यों को सत्यापित करना था। तीसरा खुद को शर्मिंदा करना था। उन्होंने तीसरा चुना। इसे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के वर्गों के अस्तित्व से सुगम बनाया गया था, जो श्रमसाध्य और स्वतंत्र जांच के बजाय पार्टी के हैंडआउट्स पर पल-पल जीते हैं और फलते-फूलते हैं। सत्तारूढ़ दलों द्वारा किए गए दावों की बारीकी से जांच करने की परंपरा, जो भी हो, ऐसा लगता है कि भुला दिया गया है।
एनडीए के सहयोगियों की राजनीतिक अप्रभावीता को देखते हुए, यह भाजपा-आरएसएस और शिवसेना हैं, जो एक साथ मिलकर प्रभावी सत्तारूढ़ गठबंधन बनाते हैं। भाजपा और आरएसएस के प्रवक्ताओं ने जोर देकर कहा कि उन्हें कांग्रेस, प्रमुख विपक्षी दल, या किसी अन्य से प्रशंसापत्र की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, उन्होंने इंदिरा गांधी, सी राजगोपालाचारी और महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध कम्युनिस्ट द्वारा 1966 में सावरकर की मृत्यु पर दिए गए बयानों का हवाला दिया।
तथ्य यह है कि 27 फरवरी, 1948 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखा गया सरदार पटेल का पत्र मई 1973 में सार्वजनिक हुआ, जब पटेल के पत्राचार का खंड 6 प्रकाशित हुआ। पत्र में, पटेल, जो उप प्रधान मंत्री और गृह मंत्री थे, ने गांधी को मारने की साजिश के बारे में लिखा: "यह सीधे सावरकर के अधीन हिंदू महासभा का एक कट्टर विंग था जिसने साजिश रची और इसे पूरा किया।" (पृष्ठ 56)।
अब डॉ. कलाम ने सत्ताधारी गठजोड़ के इशारे पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद के सेंट्रल हॉल में इसी व्यक्ति की तस्वीर का अनावरण किया है। और यह सत्तारूढ़ गठबंधन की वाहवाही के लिए किया गया है। यह आश्चर्य की बात है कि मीडिया के बड़े हिस्से ने अभी तक इस घटना के अर्थ को स्वीकार नहीं किया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ वर्गों ने महाराष्ट्र में सावरकर की दावा की गई स्थिति को पर्याप्त औचित्य के रूप में पेश किया।
पटेल को खुफिया रिपोर्ट की जानकारी थी। कपूर जांच आयोग द्वारा "महात्मा गांधी की हत्या की साजिश" में कई खुफिया रिपोर्टों का भी उल्लेख किया गया है। इस आयोग ने 1969 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के भाग II के पृष्ठ 318 में हत्यारों के साथ सावरकर की संलिप्तता स्पष्ट रूप से दर्ज है। हालांकि हत्या के मुकदमे में सावरकर को दोषी नहीं ठहराया गया था, लेकिन इसका हत्या के लिए उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी से बहुत कम लेना-देना था। साजिश के लिए सावरकर की कानूनी जिम्मेदारी के संबंध में भी, यह "कोई सबूत नहीं" का मामला नहीं था। सरकारी गवाह दिगंबर बैज ने सावरकर का नाम लिया था। ट्रायल कोर्ट ने विशिष्ट बैरिस्टर, केएल गौबा के रूप में, अपनी पुस्तक महात्मा गांधी की हत्या के पृष्ठ 220-221 में रिकॉर्ड किया, कि अनुमोदक के साक्ष्य की पुष्टि की आवश्यकता है।
इस प्रकार सावरकर का गांधी हत्याकांड में स्पष्ट रूप से नाम आया था। हालांकि साक्ष्य प्रक्रिया के अनुसार कानूनी जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से साबित नहीं हुई थी, उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी पेटेंट है। यही कारण है कि हत्या की जांच के दौरान भी सावरकर ने बीमारी की दलील दी और जैसा कि उनकी आदत थी, एक वचन दिया। उन्होंने 22 फरवरी, 1948 को पुलिस आयुक्त को दिए एक बयान में कहा: "नतीजतन सभी संदेहों को दूर करने और प्रतिनिधित्व का समर्थन करने के लिए मैं सरकार को एक वचन देने की इच्छा व्यक्त करना चाहता हूं कि मैं इसमें भाग लेने से बचूंगा।अगर मुझे उस शर्त पर रिहा किया जाता है तो सरकार को किसी भी अवधि के लिए किसी भी सांप्रदायिक या राजनीतिक गतिविधि की आवश्यकता हो सकती है।" (केएल गौबा, पृष्ठ 209)। जाहिर है, वचन देने वाला अपने खिलाफ सबूतों को लेकर आशंकित था।
सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रवक्ताओं ने यह सुझाव देने की कोशिश की है कि तस्वीर के संबंध में अपने विरोध में कांग्रेस को उन लोगों द्वारा गुमराह किया गया है, जिन्हें कुछ "वामपंथी" और "जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के इतिहासकार" के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि, आरसी मजूमदार किसी भी श्रेणी में नहीं आते थे। उनकी कृति, पेनल सेटलमेंट इन द अंडमान से पता चलता है कि सावरकर का पहले का रिकॉर्ड जिसके कारण उन्हें अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में सेल्युलर जेल में रखा गया था, दूषित हो गया है।
जेल से उन्होंने ब्रिटिश राज के लिए दया याचिकाओं को संबोधित किया। 14 नवंबर, 1913 की उनकी दया याचिका आरसी मजूमदार की किताब के पेज 211-214 में प्रकाशित है। याचिका में सावरकर ने लिखा है: "अब कोई भी व्यक्ति भारत और मानवता की भलाई के लिए आँख बंद करके उन कंटीले रास्तों पर नहीं चलेगा, जिन्होंने 1906-1907 में भारत की उत्तेजित और निराशाजनक स्थिति में हमें शांति और प्रगति के मार्ग से भटका दिया था। इसलिए, यदि सरकार अपने अनेक उपकारों और दया के साथ मुझे रिहा करती है तो मैं संवैधानिक प्रगति और अंग्रेजी सरकार के प्रति निष्ठा का कट्टर हिमायती होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, जो उस प्रगति की सबसे पहली शर्त है।"
इस वचन के अनुसार सावरकर ने इसके बाद कभी भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया। गौरतलब है कि यह दया याचिका भी 1975 में सार्वजनिक डोमेन में आई, जब आरसी मजूमदार की किताब भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई थी। 1911 में सावरकर ने जो पहले की याचिका दायर की थी, वह अभी तक प्रकाश में नहीं आई है, लेकिन 1913 की याचिका में इसका उल्लेख किया गया है।
जैसा कि पहले ही विपक्षी दलों द्वारा बार-बार जोर दिया जा चुका है, सावरकर राष्ट्रीयता के विचार के साथ तालमेल से बाहर थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र में है और जो भारत के संविधान को रेखांकित करता है। उदाहरण के लिए, 15 अगस्त, 1943 को, सावरकर ने घोषणा की: "मुझे मिस्टर जिन्ना के द्वि-राष्ट्र सिद्धांत से कोई झगड़ा नहीं है। हम हिंदू अपने आप में एक राष्ट्र हैं और यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं।" (इंडियन एनुअल रजिस्टर, 1943, खंड 2, पृ.10)। उन्होंने 1939 में इसी तरह का बयान दिया था, जिसमें हिंदुओं को एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित करने की मांग की गई थी। यह भारतीय राष्ट्र का काम नहीं है कि वह उन लोगों को विशेष सम्मान प्रदान करे जो इसके मूलभूत मूल्यों को भी नहीं मानते।
हम यहाँ से कहाँ जायेंगे? जहां तक सत्ताधारी गठजोड़ का सवाल है, उसने अपनी एक सटीक तस्वीर खींची है. केंद्र में वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद पहली बार, और शायद पहली बार जनसंघ और फिर भाजपा की स्थापना के बाद, सावरकरवाद को हिंदू सांप्रदायिकता की परिभाषित विशेषता के रूप में स्थापित किया गया है। भाजपा गठबंधन ने देश और दुनिया को जो आत्म-चित्रण दिया है, उसे देखते हुए उसके एनडीए सहयोगियों को यह विचार करने की जरूरत है कि वे इसके साथ अपनी खिलवाड़ को कहां तक ले जाने को तैयार हैं। यह एक महंगा डालियान रहा है। सावरकरवाद, जैसा कि पटेल ने उल्लेख किया था, केवल हिंदू महासभा के "कट्टरपंथी विंग" की विचारधारा थी। गुजरात 2002 के एक साल बाद, यह आधिकारिक हो गया है।
जिन संवैधानिक अधिकारियों ने इसे सुगम बनाया और इस उद्देश्य के लिए अपना कार्यालय दिया, वे दुनिया के सामने जवाबदेह हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं थी। हालांकि, निष्पक्ष होने के लिए उन्हें चेतावनी दी गई थी, चेतावनी पर्याप्त जल्दी नहीं आई थी। हमें शायद इस आक्रोश के लिए तैयार रहना चाहिए था जब शिवसेना के एक उम्मीदवार को लोकसभा अध्यक्ष चुना गया था। कुछ समय के लिए यह भी स्पष्ट हो गया है कि भारतीय राष्ट्रीयता की सभी चुनौतियों के प्रति सतर्क रहने के लिए अकेले राजनीतिक दलों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। संबंधित सभी व्यक्तियों से क्षमा याचना की अपेक्षा करना बहुत अधिक हो सकता है। सोमनाथ चटर्जी एक सम्माननीय अपवाद हैं।
लेकिन सरदार पटेल द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियों और अन्य सामग्री के आलोक में, इसमें शामिल सभी संवैधानिक अधिकारी, चाहे वे कोई भी हों और चाहे वे कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हों, उन्हें अपनी अंतरात्मा का सामना करने और अपनी फिटनेस के बारे में कठिन सवाल पूछने की जरूरत है। उनके कब्जे वाले कार्यालयों को पकड़ो। वे न केवल अपनी प्रतिष्ठा के बल्कि गणतंत्र की प्रतिष्ठा के संरक्षक हैं। हम सभी को उन भूमिकाओं के बारे में समान प्रश्न पूछने की आवश्यकता है जिन्हें हम करने का दावा करते हैं। यह देश, उसके मीडिया और उसके लोगों के लिए रुकने और विचार करने का समय है। समर्पण, संप्रदायवाद और हत्या की राजनीति का महिमामंडन भारतीय स्व-परिभाषा का हिस्सा नहीं हो सकता।
hinduonnet.com में ज्योतिर्मय शर्मा का यह लेख भी पढ़ने योग्य है। इसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है: मूल लेख यहां पढ़ा जा सकता है।
सावरकर की बदले की राजनीति
BY JYOTIRMAYA SHARMA
14 नवंबर, 1913 को भारत सरकार के गृह सदस्य को दोषी संख्या 32778 की याचिका को केवल आत्म-संरक्षण के कार्य के रूप में देखा जाना चाहिए। इस मामले में दोषी संख्या 32778, विनायक दामोदर सावरकर था। 'शक्तिशाली' अंग्रेजी सरकार से 'दयालु' होने की उनकी अपील संसद के सेंट्रल हॉल में उनके चित्र को लटकाए जाने के विरोध के योग्य नहीं है। और भी कारण हैं।
धनंजय कीर की सावरकर की जीवनी एक घटना की बात करती है जब 12 वर्षीय सावरकर ने गांव की मस्जिद पर पथराव करने के लिए अपने स्कूल के साथियों का नेतृत्व किया। इस घटना के बारे में सावरकर का अपना वृतांत उनके और उनके दोस्तों के खुशी से नाचने की बात करता है। वे जब भी उन्होंने हिंदुओं को प्रतिशोध के रूप में मुसलमानों को मारने के बारे में सुनते हैं तो आनंदित होते हैं।
एक मस्जिद को तोड़ना हिंदू धर्म के संरक्षण और राष्ट्रीय सम्मान की स्थापना में उनका योगदान था। इस घटना के बारे में सावरकर का वर्णन महत्वपूर्ण है। सावरकर कहते हैं, "हमने जी-जान से मस्जिद को तहस-नहस कर दिया और उस पर अपनी वीरता का परचम लहराया। हमने शिवाजी की युद्ध-नीति का पूरी तरह पालन किया और अपना काम पूरा करके वहां से भाग खड़े हुए।"
गांव के मुस्लिम लड़कों ने जवाबी हमला किया। सावरकर के धर्मवीर योद्धाओं के बैंड ने चाकू, पिन और फुट रूलर्स के साथ चुनौती का सामना किया। सावरकर इस धर्मयुद्ध में हिंदुओं की जीत को याद करते हैं। इसलिए, हर दृष्टि से सावरकर प्रतिशोध और प्रतिकार की भाषा के जनक हैं, ये सभी प्रतिशोध के पर्यायवाची हैं। भाजपा, शिवसेना, विहिप, बजरंग दल, नरेंद्र मोदी और प्रवीण तोगड़िया सावरकर के उत्तराधिकारी हैं।
सावरकर और उनकी आध्यात्मिक संतति को बेहतर ढंग से समझने के लिए, 1857 पर उनके लंबे निबंध को फिर से पढ़ना उपयोगी होगा। सावरकर की राष्ट्रवाद की धारणा कभी भी मैजिनी की नकल करने से आगे नहीं बढ़ी। 1857 के उनके वृतांत के बारे में जो चिढ़ाने वाला है, वह है अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों द्वारा एक साथ छेड़े जा रहे राजनीतिक जिहाद शब्द का प्रयोग। इस राजनीतिक जिहाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी हिंसा पर निर्भरता थी।
जबकि राष्ट्रवादी उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में हिंसा की प्रभावकारिता पर अंतहीन चर्चा हो सकती है, सावरकर के खाते में जो उल्लेखनीय है वह अंग्रेजी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा का औचित्य है। यहाँ एक उदाहरण है। कानपुर के बीबीगढ़ में ऐसा ही हुआ। दृश्य वह है जहां जेल प्रहरियों ने अंग्रेजों का नरसंहार करने से इंकार कर दिया। बागियों के कब्जे वाले बीबीगढ़ की मुख्य अधिकारी बेगम साहब कानपुर की कसाई बस्ती को संदेश भेजती हैं: ''थोड़ी ही देर में कसाई नंगी तलवारें और धारदार चाकू लेकर शाम को बीबीगढ़ में दाखिल हो जाएं और वहां से देर रात बाहर निकलें। उनके अंदर आने और बाहर आने के बीच सफेद खून का एक समुद्र चारों ओर फैल गया। जैसे ही वे अपनी तलवारें और चाकू लेकर घुसे, उन्होंने 150 महिलाओं और बच्चों को मार डाला। अंदर जाते समय कसाई चलते रहे और बाहर आने के दौरान उन्हें खून से लथपथ जमीन की यात्रा करनी पड़ी।"
यहां सावरकर की भावहीन टिप्पणी यह है कि दोनों नस्लों के बीच जमा हुए खाते को चुकता कर दिया गया था। इसलिए बदला, सावरकर के लिए प्राकृतिक कानून और न्याय की स्थापना थी। इस स्वयंसिद्ध से, वह राष्ट्रवाद के एक सिद्धांत को प्राप्त करते हैं। उनके अनुसार हिन्दू और मुसलमान 'दो' राष्ट्र थे। उनका तर्क है कि जहां भी अन्याय बढ़ता है और राष्ट्र आग की लपटों में घिर जाते हैं, जहां भी राष्ट्रवादी युद्ध लड़े जाते हैं, अन्याय का बदला जो राष्ट्र भुगतता है, दूसरे राष्ट्र के कथित अपराधियों को मार कर लिया जाता है।
कम से कम औपचारिक रूप से, सावरकर ने जिन्ना के सामने द्विराष्ट्र सिद्धांत रखा। हालाँकि, हिंदुओं को अधिक 'मर्दाना' बनाए बिना बदला लेना असंभव था। यहां सावरकर की हिंदू धर्म के केंद्रीय सिद्धांतों की समझ की कमी है। उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदुत्व के बीच अंतर किया और हिंदुत्व को अभूतपूर्व प्रधानता प्रदान की। हालाँकि, हिंदुत्व की उनकी अवधारणा का एक अप्रत्याशित स्रोत था। सावरकर ने इस्लाम के राजनीतिक और धार्मिक उत्साह की बहुत प्रशंसा की। वह मुसलमानों के सामाजिक एकता और वीरता के उत्साह से ईर्ष्या करता था, एक ऐसा कारक जिसने उन्हें एक शरीर के रूप में इतना अप्रतिरोध्य बना दिया था।
सावरकर के अनुसार, मुसलमानों में ऐसे गुण थे जो उन्हें अभेद्य बनाते थे जबकि हिंदू तत्वमीमांसा और परंपरा से घिरे हुए थे। छत्रपति शिवाजी द्वारा एक मराठा साम्राज्य की स्थापना के बाद, हिंदुओं ने "मुहम्मदों की सफलता में योगदान देने वाले बहुत कुछ अवशोषित कर लिया था।" सावरकर की थीसिस को फिर से दोहराना उपयोगी होगा कि किस चीज ने मुसलमानों को इतना अप्रतिरोध्य बना दिया। उनके पास एक एकीकृत चर्च था, जिसका हिंदू धर्म में अभाव था। इसने उन्हें अपने विरोधियों से निपटने के लिए बेहतर तरीके से सुसज्जित किया। इसके ठीक विपरीत, हिंदू निराशाजनक रूप से दर्शन के विद्यालयों, दुर्बल करने वाली तत्वमीमांसा प्रस्तावों, जातियों और परम्पराओं के रूप में बंटे हुए थे।
हिंदुओं को कर्म सिद्धांत और बल के उपयोग के सैद्धांतिक विरोध जैसे सिद्धांतों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए छोड़ दिया गया था, जो सभी सिद्धांत और व्यवहार के बीच एक अलगाव की ओर ले जाते हैं। संक्षेप में, 'स्व' ने स्वयं को फिर से परिभाषित करने के लिए 'अन-स्व' का एक बड़ा हिस्सा अवशोषित कर लिया था। यही राजनीतिक हिंदुत्व की बुनियाद है। यह हिंदू धर्म की एक सनकी गलतफहमी पर आधारित है, जबकि कोई वैकल्पिक तत्वमीमांसा या नैतिक ब्रह्मांड की पेशकश नहीं करता है। राजनीतिक हिंदुत्व के केंद्रीय सिद्धांत प्रतिशोध, प्रतिशोध और 'ताकत ही सही है' का खेदजनक सिद्धांत है।
संसद में सावरकर का चित्र सज्जनता, शिष्टता और अहिंसा जैसी धारणाओं के सार्वजनिक जीवन से लुप्त होने का दुखद प्रमाण है। इससे ज्यादा अहिंदू कुछ नहीं हो सकता।
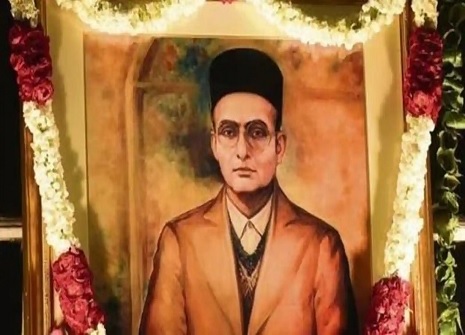
पोर्ट्रेट एज़ मिरर (अप्रैल 2003 वर्ष 9, संख्या 86, कम्युनलिज्म कॉम्बैट)
फरवरी 2003 में यह भारतीय संसद थी; अब,अप्रैल 2003 में, यह महाराष्ट्र राज्य विधानसभा है। इन दोनों पवित्र परिसरों में अब विनायक दामोदर सावरकर का चित्र लटका हुआ है। एक व्यक्ति जिसका महात्मा गांधी की हत्या में हाथ था, वह भारत के पूर्व उप प्रधान मंत्री और गृह मंत्री सरदार पटेल से की बराबरी पर था; एक ऐसा व्यक्ति जिसका भारत के लिए सपना एक ऐसे सैन्यीकृत हिंदू राष्ट्र का था जो प्रतिशोध और बहिष्कार की राजनीति से गढ़ा गया था। हम यहां मेनलाइन मीडिया के दो लेखों को पुन: प्रस्तुत कर रहे हैं जो इस अत्यधिक परेशान करने वाले घटनाक्रम पर गंभीर सवाल उठाते हैं। इस मुद्दे पर अधिक विस्तृत प्रलेखन के लिए, पाठकों से अनुरोध है कि हमारी वेबसाइट www.sabrang.com पर विजिट करें)।
26 फरवरी को राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा वीडी सावरकर के एक चित्र का संसद में अनावरण किया गया। दरअसल सत्ता पक्ष, केंद्र सरकार और इस प्रकरण में शामिल संवैधानिक पदाधिकारियों की मुश्किलें अभी शुरू ही हुई होंगी। निहितार्थ भारत में सरकार के भविष्य के पाठ्यक्रम को छूते हैं। इस मुद्दे का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ वर्गों की भूमिका पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चित्र प्रकरण ने उनके लिए भी एक दर्पण के रूप में काम किया है।
महात्मा गांधी की हत्या में सावरकर की संलिप्तता और कुछ अन्य मुद्दों पर तथ्यों को सार्वजनिक डोमेन में लाने के बाद, अधिकारियों के पास तीन विकल्प थे। पहला था माफ़ी माँगना और उस रास्ते से लौट जाना जिस पर वे चल पड़े थे। दूसरा समारोह को स्थगित करना और तथ्यों को सत्यापित करना था। तीसरा खुद को शर्मिंदा करना था। उन्होंने तीसरा चुना। इसे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के वर्गों के अस्तित्व से सुगम बनाया गया था, जो श्रमसाध्य और स्वतंत्र जांच के बजाय पार्टी के हैंडआउट्स पर पल-पल जीते हैं और फलते-फूलते हैं। सत्तारूढ़ दलों द्वारा किए गए दावों की बारीकी से जांच करने की परंपरा, जो भी हो, ऐसा लगता है कि भुला दिया गया है।
एनडीए के सहयोगियों की राजनीतिक अप्रभावीता को देखते हुए, यह भाजपा-आरएसएस और शिवसेना हैं, जो एक साथ मिलकर प्रभावी सत्तारूढ़ गठबंधन बनाते हैं। भाजपा और आरएसएस के प्रवक्ताओं ने जोर देकर कहा कि उन्हें कांग्रेस, प्रमुख विपक्षी दल, या किसी अन्य से प्रशंसापत्र की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, उन्होंने इंदिरा गांधी, सी राजगोपालाचारी और महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध कम्युनिस्ट द्वारा 1966 में सावरकर की मृत्यु पर दिए गए बयानों का हवाला दिया।
तथ्य यह है कि 27 फरवरी, 1948 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखा गया सरदार पटेल का पत्र मई 1973 में सार्वजनिक हुआ, जब पटेल के पत्राचार का खंड 6 प्रकाशित हुआ। पत्र में, पटेल, जो उप प्रधान मंत्री और गृह मंत्री थे, ने गांधी को मारने की साजिश के बारे में लिखा: "यह सीधे सावरकर के अधीन हिंदू महासभा का एक कट्टर विंग था जिसने साजिश रची और इसे पूरा किया।" (पृष्ठ 56)।
अब डॉ. कलाम ने सत्ताधारी गठजोड़ के इशारे पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद के सेंट्रल हॉल में इसी व्यक्ति की तस्वीर का अनावरण किया है। और यह सत्तारूढ़ गठबंधन की वाहवाही के लिए किया गया है। यह आश्चर्य की बात है कि मीडिया के बड़े हिस्से ने अभी तक इस घटना के अर्थ को स्वीकार नहीं किया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ वर्गों ने महाराष्ट्र में सावरकर की दावा की गई स्थिति को पर्याप्त औचित्य के रूप में पेश किया।
पटेल को खुफिया रिपोर्ट की जानकारी थी। कपूर जांच आयोग द्वारा "महात्मा गांधी की हत्या की साजिश" में कई खुफिया रिपोर्टों का भी उल्लेख किया गया है। इस आयोग ने 1969 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के भाग II के पृष्ठ 318 में हत्यारों के साथ सावरकर की संलिप्तता स्पष्ट रूप से दर्ज है। हालांकि हत्या के मुकदमे में सावरकर को दोषी नहीं ठहराया गया था, लेकिन इसका हत्या के लिए उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी से बहुत कम लेना-देना था। साजिश के लिए सावरकर की कानूनी जिम्मेदारी के संबंध में भी, यह "कोई सबूत नहीं" का मामला नहीं था। सरकारी गवाह दिगंबर बैज ने सावरकर का नाम लिया था। ट्रायल कोर्ट ने विशिष्ट बैरिस्टर, केएल गौबा के रूप में, अपनी पुस्तक महात्मा गांधी की हत्या के पृष्ठ 220-221 में रिकॉर्ड किया, कि अनुमोदक के साक्ष्य की पुष्टि की आवश्यकता है।
इस प्रकार सावरकर का गांधी हत्याकांड में स्पष्ट रूप से नाम आया था। हालांकि साक्ष्य प्रक्रिया के अनुसार कानूनी जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से साबित नहीं हुई थी, उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी पेटेंट है। यही कारण है कि हत्या की जांच के दौरान भी सावरकर ने बीमारी की दलील दी और जैसा कि उनकी आदत थी, एक वचन दिया। उन्होंने 22 फरवरी, 1948 को पुलिस आयुक्त को दिए एक बयान में कहा: "नतीजतन सभी संदेहों को दूर करने और प्रतिनिधित्व का समर्थन करने के लिए मैं सरकार को एक वचन देने की इच्छा व्यक्त करना चाहता हूं कि मैं इसमें भाग लेने से बचूंगा।अगर मुझे उस शर्त पर रिहा किया जाता है तो सरकार को किसी भी अवधि के लिए किसी भी सांप्रदायिक या राजनीतिक गतिविधि की आवश्यकता हो सकती है।" (केएल गौबा, पृष्ठ 209)। जाहिर है, वचन देने वाला अपने खिलाफ सबूतों को लेकर आशंकित था।
सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रवक्ताओं ने यह सुझाव देने की कोशिश की है कि तस्वीर के संबंध में अपने विरोध में कांग्रेस को उन लोगों द्वारा गुमराह किया गया है, जिन्हें कुछ "वामपंथी" और "जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के इतिहासकार" के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि, आरसी मजूमदार किसी भी श्रेणी में नहीं आते थे। उनकी कृति, पेनल सेटलमेंट इन द अंडमान से पता चलता है कि सावरकर का पहले का रिकॉर्ड जिसके कारण उन्हें अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में सेल्युलर जेल में रखा गया था, दूषित हो गया है।
जेल से उन्होंने ब्रिटिश राज के लिए दया याचिकाओं को संबोधित किया। 14 नवंबर, 1913 की उनकी दया याचिका आरसी मजूमदार की किताब के पेज 211-214 में प्रकाशित है। याचिका में सावरकर ने लिखा है: "अब कोई भी व्यक्ति भारत और मानवता की भलाई के लिए आँख बंद करके उन कंटीले रास्तों पर नहीं चलेगा, जिन्होंने 1906-1907 में भारत की उत्तेजित और निराशाजनक स्थिति में हमें शांति और प्रगति के मार्ग से भटका दिया था। इसलिए, यदि सरकार अपने अनेक उपकारों और दया के साथ मुझे रिहा करती है तो मैं संवैधानिक प्रगति और अंग्रेजी सरकार के प्रति निष्ठा का कट्टर हिमायती होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, जो उस प्रगति की सबसे पहली शर्त है।"
इस वचन के अनुसार सावरकर ने इसके बाद कभी भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया। गौरतलब है कि यह दया याचिका भी 1975 में सार्वजनिक डोमेन में आई, जब आरसी मजूमदार की किताब भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई थी। 1911 में सावरकर ने जो पहले की याचिका दायर की थी, वह अभी तक प्रकाश में नहीं आई है, लेकिन 1913 की याचिका में इसका उल्लेख किया गया है।
जैसा कि पहले ही विपक्षी दलों द्वारा बार-बार जोर दिया जा चुका है, सावरकर राष्ट्रीयता के विचार के साथ तालमेल से बाहर थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र में है और जो भारत के संविधान को रेखांकित करता है। उदाहरण के लिए, 15 अगस्त, 1943 को, सावरकर ने घोषणा की: "मुझे मिस्टर जिन्ना के द्वि-राष्ट्र सिद्धांत से कोई झगड़ा नहीं है। हम हिंदू अपने आप में एक राष्ट्र हैं और यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं।" (इंडियन एनुअल रजिस्टर, 1943, खंड 2, पृ.10)। उन्होंने 1939 में इसी तरह का बयान दिया था, जिसमें हिंदुओं को एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित करने की मांग की गई थी। यह भारतीय राष्ट्र का काम नहीं है कि वह उन लोगों को विशेष सम्मान प्रदान करे जो इसके मूलभूत मूल्यों को भी नहीं मानते।
हम यहाँ से कहाँ जायेंगे? जहां तक सत्ताधारी गठजोड़ का सवाल है, उसने अपनी एक सटीक तस्वीर खींची है. केंद्र में वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद पहली बार, और शायद पहली बार जनसंघ और फिर भाजपा की स्थापना के बाद, सावरकरवाद को हिंदू सांप्रदायिकता की परिभाषित विशेषता के रूप में स्थापित किया गया है। भाजपा गठबंधन ने देश और दुनिया को जो आत्म-चित्रण दिया है, उसे देखते हुए उसके एनडीए सहयोगियों को यह विचार करने की जरूरत है कि वे इसके साथ अपनी खिलवाड़ को कहां तक ले जाने को तैयार हैं। यह एक महंगा डालियान रहा है। सावरकरवाद, जैसा कि पटेल ने उल्लेख किया था, केवल हिंदू महासभा के "कट्टरपंथी विंग" की विचारधारा थी। गुजरात 2002 के एक साल बाद, यह आधिकारिक हो गया है।
जिन संवैधानिक अधिकारियों ने इसे सुगम बनाया और इस उद्देश्य के लिए अपना कार्यालय दिया, वे दुनिया के सामने जवाबदेह हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं थी। हालांकि, निष्पक्ष होने के लिए उन्हें चेतावनी दी गई थी, चेतावनी पर्याप्त जल्दी नहीं आई थी। हमें शायद इस आक्रोश के लिए तैयार रहना चाहिए था जब शिवसेना के एक उम्मीदवार को लोकसभा अध्यक्ष चुना गया था। कुछ समय के लिए यह भी स्पष्ट हो गया है कि भारतीय राष्ट्रीयता की सभी चुनौतियों के प्रति सतर्क रहने के लिए अकेले राजनीतिक दलों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। संबंधित सभी व्यक्तियों से क्षमा याचना की अपेक्षा करना बहुत अधिक हो सकता है। सोमनाथ चटर्जी एक सम्माननीय अपवाद हैं।
लेकिन सरदार पटेल द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियों और अन्य सामग्री के आलोक में, इसमें शामिल सभी संवैधानिक अधिकारी, चाहे वे कोई भी हों और चाहे वे कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हों, उन्हें अपनी अंतरात्मा का सामना करने और अपनी फिटनेस के बारे में कठिन सवाल पूछने की जरूरत है। उनके कब्जे वाले कार्यालयों को पकड़ो। वे न केवल अपनी प्रतिष्ठा के बल्कि गणतंत्र की प्रतिष्ठा के संरक्षक हैं। हम सभी को उन भूमिकाओं के बारे में समान प्रश्न पूछने की आवश्यकता है जिन्हें हम करने का दावा करते हैं। यह देश, उसके मीडिया और उसके लोगों के लिए रुकने और विचार करने का समय है। समर्पण, संप्रदायवाद और हत्या की राजनीति का महिमामंडन भारतीय स्व-परिभाषा का हिस्सा नहीं हो सकता।
hinduonnet.com में ज्योतिर्मय शर्मा का यह लेख भी पढ़ने योग्य है। इसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है: मूल लेख यहां पढ़ा जा सकता है।
सावरकर की बदले की राजनीति
BY JYOTIRMAYA SHARMA
14 नवंबर, 1913 को भारत सरकार के गृह सदस्य को दोषी संख्या 32778 की याचिका को केवल आत्म-संरक्षण के कार्य के रूप में देखा जाना चाहिए। इस मामले में दोषी संख्या 32778, विनायक दामोदर सावरकर था। 'शक्तिशाली' अंग्रेजी सरकार से 'दयालु' होने की उनकी अपील संसद के सेंट्रल हॉल में उनके चित्र को लटकाए जाने के विरोध के योग्य नहीं है। और भी कारण हैं।
धनंजय कीर की सावरकर की जीवनी एक घटना की बात करती है जब 12 वर्षीय सावरकर ने गांव की मस्जिद पर पथराव करने के लिए अपने स्कूल के साथियों का नेतृत्व किया। इस घटना के बारे में सावरकर का अपना वृतांत उनके और उनके दोस्तों के खुशी से नाचने की बात करता है। वे जब भी उन्होंने हिंदुओं को प्रतिशोध के रूप में मुसलमानों को मारने के बारे में सुनते हैं तो आनंदित होते हैं।
एक मस्जिद को तोड़ना हिंदू धर्म के संरक्षण और राष्ट्रीय सम्मान की स्थापना में उनका योगदान था। इस घटना के बारे में सावरकर का वर्णन महत्वपूर्ण है। सावरकर कहते हैं, "हमने जी-जान से मस्जिद को तहस-नहस कर दिया और उस पर अपनी वीरता का परचम लहराया। हमने शिवाजी की युद्ध-नीति का पूरी तरह पालन किया और अपना काम पूरा करके वहां से भाग खड़े हुए।"
गांव के मुस्लिम लड़कों ने जवाबी हमला किया। सावरकर के धर्मवीर योद्धाओं के बैंड ने चाकू, पिन और फुट रूलर्स के साथ चुनौती का सामना किया। सावरकर इस धर्मयुद्ध में हिंदुओं की जीत को याद करते हैं। इसलिए, हर दृष्टि से सावरकर प्रतिशोध और प्रतिकार की भाषा के जनक हैं, ये सभी प्रतिशोध के पर्यायवाची हैं। भाजपा, शिवसेना, विहिप, बजरंग दल, नरेंद्र मोदी और प्रवीण तोगड़िया सावरकर के उत्तराधिकारी हैं।
सावरकर और उनकी आध्यात्मिक संतति को बेहतर ढंग से समझने के लिए, 1857 पर उनके लंबे निबंध को फिर से पढ़ना उपयोगी होगा। सावरकर की राष्ट्रवाद की धारणा कभी भी मैजिनी की नकल करने से आगे नहीं बढ़ी। 1857 के उनके वृतांत के बारे में जो चिढ़ाने वाला है, वह है अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों द्वारा एक साथ छेड़े जा रहे राजनीतिक जिहाद शब्द का प्रयोग। इस राजनीतिक जिहाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी हिंसा पर निर्भरता थी।
जबकि राष्ट्रवादी उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में हिंसा की प्रभावकारिता पर अंतहीन चर्चा हो सकती है, सावरकर के खाते में जो उल्लेखनीय है वह अंग्रेजी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा का औचित्य है। यहाँ एक उदाहरण है। कानपुर के बीबीगढ़ में ऐसा ही हुआ। दृश्य वह है जहां जेल प्रहरियों ने अंग्रेजों का नरसंहार करने से इंकार कर दिया। बागियों के कब्जे वाले बीबीगढ़ की मुख्य अधिकारी बेगम साहब कानपुर की कसाई बस्ती को संदेश भेजती हैं: ''थोड़ी ही देर में कसाई नंगी तलवारें और धारदार चाकू लेकर शाम को बीबीगढ़ में दाखिल हो जाएं और वहां से देर रात बाहर निकलें। उनके अंदर आने और बाहर आने के बीच सफेद खून का एक समुद्र चारों ओर फैल गया। जैसे ही वे अपनी तलवारें और चाकू लेकर घुसे, उन्होंने 150 महिलाओं और बच्चों को मार डाला। अंदर जाते समय कसाई चलते रहे और बाहर आने के दौरान उन्हें खून से लथपथ जमीन की यात्रा करनी पड़ी।"
यहां सावरकर की भावहीन टिप्पणी यह है कि दोनों नस्लों के बीच जमा हुए खाते को चुकता कर दिया गया था। इसलिए बदला, सावरकर के लिए प्राकृतिक कानून और न्याय की स्थापना थी। इस स्वयंसिद्ध से, वह राष्ट्रवाद के एक सिद्धांत को प्राप्त करते हैं। उनके अनुसार हिन्दू और मुसलमान 'दो' राष्ट्र थे। उनका तर्क है कि जहां भी अन्याय बढ़ता है और राष्ट्र आग की लपटों में घिर जाते हैं, जहां भी राष्ट्रवादी युद्ध लड़े जाते हैं, अन्याय का बदला जो राष्ट्र भुगतता है, दूसरे राष्ट्र के कथित अपराधियों को मार कर लिया जाता है।
कम से कम औपचारिक रूप से, सावरकर ने जिन्ना के सामने द्विराष्ट्र सिद्धांत रखा। हालाँकि, हिंदुओं को अधिक 'मर्दाना' बनाए बिना बदला लेना असंभव था। यहां सावरकर की हिंदू धर्म के केंद्रीय सिद्धांतों की समझ की कमी है। उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदुत्व के बीच अंतर किया और हिंदुत्व को अभूतपूर्व प्रधानता प्रदान की। हालाँकि, हिंदुत्व की उनकी अवधारणा का एक अप्रत्याशित स्रोत था। सावरकर ने इस्लाम के राजनीतिक और धार्मिक उत्साह की बहुत प्रशंसा की। वह मुसलमानों के सामाजिक एकता और वीरता के उत्साह से ईर्ष्या करता था, एक ऐसा कारक जिसने उन्हें एक शरीर के रूप में इतना अप्रतिरोध्य बना दिया था।
सावरकर के अनुसार, मुसलमानों में ऐसे गुण थे जो उन्हें अभेद्य बनाते थे जबकि हिंदू तत्वमीमांसा और परंपरा से घिरे हुए थे। छत्रपति शिवाजी द्वारा एक मराठा साम्राज्य की स्थापना के बाद, हिंदुओं ने "मुहम्मदों की सफलता में योगदान देने वाले बहुत कुछ अवशोषित कर लिया था।" सावरकर की थीसिस को फिर से दोहराना उपयोगी होगा कि किस चीज ने मुसलमानों को इतना अप्रतिरोध्य बना दिया। उनके पास एक एकीकृत चर्च था, जिसका हिंदू धर्म में अभाव था। इसने उन्हें अपने विरोधियों से निपटने के लिए बेहतर तरीके से सुसज्जित किया। इसके ठीक विपरीत, हिंदू निराशाजनक रूप से दर्शन के विद्यालयों, दुर्बल करने वाली तत्वमीमांसा प्रस्तावों, जातियों और परम्पराओं के रूप में बंटे हुए थे।
हिंदुओं को कर्म सिद्धांत और बल के उपयोग के सैद्धांतिक विरोध जैसे सिद्धांतों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए छोड़ दिया गया था, जो सभी सिद्धांत और व्यवहार के बीच एक अलगाव की ओर ले जाते हैं। संक्षेप में, 'स्व' ने स्वयं को फिर से परिभाषित करने के लिए 'अन-स्व' का एक बड़ा हिस्सा अवशोषित कर लिया था। यही राजनीतिक हिंदुत्व की बुनियाद है। यह हिंदू धर्म की एक सनकी गलतफहमी पर आधारित है, जबकि कोई वैकल्पिक तत्वमीमांसा या नैतिक ब्रह्मांड की पेशकश नहीं करता है। राजनीतिक हिंदुत्व के केंद्रीय सिद्धांत प्रतिशोध, प्रतिशोध और 'ताकत ही सही है' का खेदजनक सिद्धांत है।
संसद में सावरकर का चित्र सज्जनता, शिष्टता और अहिंसा जैसी धारणाओं के सार्वजनिक जीवन से लुप्त होने का दुखद प्रमाण है। इससे ज्यादा अहिंदू कुछ नहीं हो सकता।



