दुनिया के बाकी समाजों की तुलना में भारतीय समाज की एक विशेषता यह है कि उसमें हमेशा से तरह-तरह के साधु-संन्यासी बड़ी संख्या में विद्यमान रहे हैं। आज भी देश में एक बड़ा साधु समाज मौजूद है। कहना न होगा कि हिंदू समाज में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। इसका एक स्पष्ट कारण हिंदू समाज की बाकी समाजों के मुकाबले ज्यादा आबादी तो है ही, इस परिघटना के ठोस समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं, जिनका गंभीर अध्ययन होना अभी बाकी है। दुनिया के सभी समाजों में धार्मिक गतिविधियों से जुड़े साधु-संत प्रायः सभी नागरिकों के सम्मान का पात्र होते हैं। भारत में प्राचीन काल के ऋषि-मुनियों और मध्यकाल के साधु-संतों के प्रति राजा से लेकर रंक तक सभी में अत्यंत आदर का भाव देखने को मिलता है। नास्तिक भी साधुओं को स्वीकार भले ही न करें, उनका असम्मान नहीं करते। आमतौर पर अपना लोक-परलोक सुधारने की चिंता में लोग साधु-संन्यासियों का सम्मान करते हैं, लेकिन विशेषतौर पर साधु-संन्यासियों का भवबंधन से मुक्त अनासक्त, आध्यात्मिक और पवित्र जीवन उनके सम्मान का कारण बनता है।
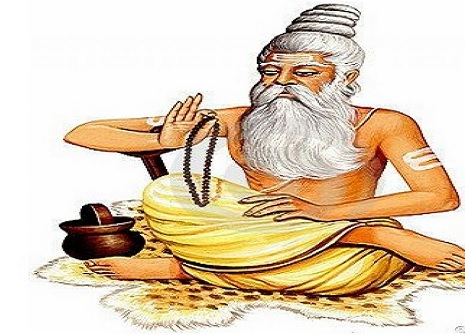
प्रतीकात्मक चित्र
ध्यान दिया जा सकता है कि साधुओं की बहुतायत के साथ, अथवा इस बहुतायत के कारण ही संस्कृत साहित्य से लेकर भक्तिकाल तक और लोक अनुभव में आज तक सच्चे साधु की पहचान का विमर्श भी बराबर मिलता है। इस विमर्श का निचोड़ यही है कि सच्चा साधु कोई एकाध ही होता है। बाकी सब लोक-परलोक का व्यवसाय करके, लोक विमर्श में कहा जाए तो ठगी करके, अपना पेट पालने से लेकर पूरा घर भरने वाले होते हैं। भारतीय समाज में आज भी ऐसे ही साधुओं की बहुतायत है। लोक विश्वास में इन्हें ढोंगी साधु कह कर पुकारने की परंपरा है। रंगे हुए सियार की तर्ज पर इन्हें रंगे हुए साधु भी कहा जाता है। ऐसे साधुओं से समाज को आक्रांत पाकर ही एक भक्त कवि ने कहा था:
‘सिंघन के लहँड़े नहीं, हंसन की नहीं पाँत।
लालन की नहीं बोरियाँ, साधु न चलें जमात।।’
साधु के स्वभाव में निहित गुणों में प्रेम और सार-निस्सार के बीच विवेक की योग्यता को केंद्रीय माना गया है। सांसारिकता में जीते हुए इन गुणों के चलते कोई व्यक्ति साधु होता है और इन गुणों के अभाव में सांसारिकता से विरक्त व्यक्ति भी साधु कहलाने का पात्र नहीं बनता। साधु भक्त भी हो सकता है, लेकिन भक्त जरूरी नहीं कि साधु भी हो। प्रेम-रहित भक्ति करने वाला व्यक्ति कोरा (कठोर पढ़ा जाए) भक्त ही होगा, जो आत्म-मुक्ति के फेर में ही पड़ा रह सकता है, जिसकी कोई वृहत्तर मानवीय सार्थकता नहीं होती। भक्त तत्त्वज्ञानी भी हो सकता है, लेकिन महान तत्वज्ञानी होने के बावजूद वह कई बार क्रूर और अविवेकी हो सकता है। इसे शंकराचार्य के उदाहरण से समझा जा सकता है। भारतीय दर्शन की चरम उपलब्धि माने जाने वाले अद्वैत दर्शन के प्रणेता शंकराचार्य वेद का उच्चारण करने वाले शूद्र की जीभ काट लेने और भूल से भी वेदमंत्र सुन लेने वाले शूद्र के कान में पिघला हुआ शीशा डालने का समर्थन करते हैं। शंकराचार्य महान ज्ञानमार्गी भक्त माने जाते हैं। भक्तिकाल के संतों को भी ज्ञानमार्गी भक्त कहा जाता है। कबीर ने ज्ञान की आँधी आने की बात कही है। सूक्ष्म तत्व-चिंतन भी उनके यहाँ कम नहीं हैः ‘पुहुप बास ते पातरा ऐसा तत्त अनूप’। लेकिन उनका ज्ञान कोरा तत्वज्ञान नहीं है। उसे प्रेम की अंतःसलिला सींचती है। मध्यकालीन संतों-भक्तों का यह प्रेम कोई अमूर्त चीज नहीं है, उसके ठोस मानवीय और सामाजिक संदर्भ हैं। आधुनिक युग में रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य विवेकानन्द ने वेदांत के मूल में प्रेम की प्रतिष्ठा कर उसे नव्यवेदांत के रूप में प्रस्तुत किया, तो उसका भी ठोस मानवीय और सामाजिक संदर्भ बनता है। विवेकानन्द ने तो शंकराचार्य के वेदांत दर्शन में शूद्रों के प्रति बरती गई प्रतिमानवीयता का प्रतिकार यह कह कर किया कि ‘भारत शूद्रों का होगा’।
प्रेम भक्ति में मानवीय अंतर्वस्तु का सृजन करता है, इसीलिए प्रेम को भक्ति के मूल में स्थापित किया गया है। यह अकारण नहीं है कि भक्ति के कई प्रकारों में प्रेममयी रागानुराग भक्ति को ही सर्वोच्च अर्थात् वास्तविक भक्ति माना गया है। प्रेम केवल ईश्वर या परम सत्ता के प्रति ही नहीं, चराचर जीवन-जगत के प्रति। ईश्वर के प्रति प्रेम की साधना से उसकी सृष्टि के प्रति प्रेम विकसित होगा या सृष्टि के प्रति प्रेम की साधना से ईश्वरी प्रेम विकसित होगा - यह पद्धति-भेद की बात हो सकती है। दोनों ही पद्धतियों में प्रेम एक कठिन साधना है। प्रेम के घर में पैठने के लिए अपना सिर उतार कर जमीन पर रखना पड़ सकता है। अतः कह सकते हैं कि सच्चा साधु प्रेम और करुणा के मानवीय गुण से उसके प्रतिलोम घृणा और क्रूरता से निरंतर संघर्ष करता है। सच्चा भक्त भी यही करता है। (इसी स्तर पर साधु और भक्त एकरूप हो जाते हैं।)
यह आसान साधना नहीं है, इसीलिए सच्चा साधु विरल माना गया है और सम्मानीय भी। समाज में साधु के सम्मान का एक और उच्चतर आयाम होता है, जहाँ वह पूज्यनीय हो जाता है - वह झूठ, फरेब, लिप्सा और क्षुद्रताओं से भरे संसार में उस पवित्र-लोक (सेकरेड स्पेस) का प्रतीक होता है, संसार से जिसकी मौजूदगी की कामना हर व्यक्ति के मन में कहीं न कहीं होती है और जिससे जुड़ कर वह दैवी पवित्रता से जुड़ने का अनुभव करता है।
अब उन साधुओं पर विचार करें जो साधु और भक्त होने का एक साथ दावा करते हैं। ये जमात में चलते हैं और उन्होंने आजकल भारतीय समाज को आक्रांत किया हुआ है। यहाँ संघ संप्रदाय (संघ परिवार) के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए आंदोलनरत साधुओं से आशय है। साधु के रूप में उनके चरित्र यानी साधुता को परखने के लिए संघ संप्रदाय के नेताओं का चरित्र देख लेना पर्याप्त होगा, जिनके वे अनुगामी बने हुए हैं। संघ संप्रदाय के नेताओं के चरित्र का यहाँ ज्यादा बखान करने की जरूरत नहीं है। वह सर्वविदित है। केवल यही कहा जा सकता है कि अपने विरोधियों के प्रति सदा घृणा से भरे रहने वाले, धार्मिक मामलों में भी झूठ व फरेब का निस्संकोच सहारा लेने वाले और सत्ता की लिप्सा व भोगवाद से परिचालित इन नेताओं के चरित्र में एक साधु के लिए कुछ भी अनुकरणीय नहीं हो सकता। साधु की भूमिका तो घृणा, झूठ, क्रूरता और भोगवादी प्रवृत्तियों से लड़ने की होती है। इसे उल्टी गंगा बहना ही कहेंगे कि साधु नेताओं का अनुकरण कर रहे हैं। वह भी, समग्रतः हिंदू धर्म और मुख्यतः राम का उद्धार करने के लिए! उद्धार की यह मुहिम आगे भी जारी रहनी है। काशी के शिव और मथुरा के कृष्ण का भी उद्धार होना है। यानी अभी आगे भी साधुओं को संघ संप्रदाय के नेताओं के पीछे चलना है।
संघ संप्रदाय का अपना घोषित एजेंडा और विचारधारा है, जिसे ब्राह्मणवाद की अभी तक की सर्वाधिक निकृष्ट अभिव्यक्ति (मेनीफेस्टेशन) कहा जा सकता है। ब्राह्मणवादी विचारधारा ने झूठ, फरेब और बदले की भावना का ऐसा प्रदर्शन इससे पहले कभी नहीं किया। अपने अच्छे-बुरे सभी दौरों में ब्राह्मणवाद ने जीवन का एक समग्र दर्शन प्रस्तुत करने की कोशिश की है। नए सामाजिक-ऐतिहासिक दबावों में जब आत्यंतिक मान्यताओं को स्थिर रखना असंभव हो गया, तो उसने समन्वयवाद का रास्ता भी अपनाया है। हालाँकि ब्राह्मणवादी समन्वयवाद भारतीय जीवन के सामाजिक-सांस्कृतिक बहुलतावाद का मुकम्मल उत्तर कभी नहीं बन पाया। विविध सामाजिक समूहों और अस्मिताओं पर अपना वर्चस्व बनाए रखने की उसकी मूल प्रवृत्ति बराबर बनी रही। लेकिन कहा जा सकता है कि ब्राह्मणवाद ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए हमेशा ही कड़ी बौद्धिक मशक्कत का परिचय दिया है।
संघ संप्रदाय का मामला अलग है। उसकी ‘विचारधारा’ में अगर कुछ अनुपस्थित है तो वह विचार है। इसकी भरपाई वह एक तरफ रणनीतियों से, जिनमें झूठ-फरेब सब कुछ जायज है, करता है और दूसरी ओर अन्य धर्मावलम्बियों के खिलाफ घृणा और बदले की भावना फैला कर। कहना न होगा कि इस मामले में उसने पश्चिम की फासीवादी-साम्राज्यवादी शक्तियों से गहरी सीख ली है। हेडगेवार, गोलवलकर, रज्जू भैया और और सुदर्शन सभी में यह परंपरा अक्षुण्ण देखने को मिलती है। ‘उदार’ वाजपेयी, ‘कट्टर’ आडवाणी, ‘हिंदू हित शिरोमणि’ बाल ठाकरे, ‘आचार्य’ गिरिराज किशोर, ‘परमहंस’ रामचंद्र दास, ‘साध्वी’ ऋतंभरा, ‘साध्वी’ उमा भारती, ‘साक्षी महाराज’, ‘धर्म शिरोमणि’ अशोक सिंघल और ‘धर्मवीर’ प्रवीन तोगड़िया आदि इसी परंपरा के ‘योग्य’ बच्चे रहे हैं। वैचारिक शून्यता की भरपाई का संघ संप्रदाय का एक और रास्ता है। उसने अपने को पूँजीवादी-उपभोक्तावादी विचारधारा की सेवा में समर्पित कर दिया है।
संघ संप्रदाय का आत्यंतिक लक्ष्य देश में अपना राजनैतिक-सांस्कृतिक वर्चस्व कायम करना है। यह उतनी चिंता का विषय नहीं है, जितना साधुओं का उलट आचरण। संघ संप्रदाय के अभियान को राजनीति और समाज में सक्रिय अन्य धाराएँ चुनौती दे सकती हैं, बल्कि यह चुनौती उसे मिल रही है। लेकिन साधुओं का आचरण मानव जीवन के उस पवित्र-लोक को नष्ट कर रहा है, जिसका जिक्र ऊपर किया गया है। जाहिर है, इसकी चिंता सबसे ज्यादा साधुओं को ही करनी है। उन्हें गंभीरता से यह सोचना है कि जिस आदर्श के साथ उनकी छवि या पहचान जुड़ी हुई है, क्या उसे वे संघ संप्रदाय के साथ जुड़ नष्ट कर देने को तैयार हैं? साथ ही उन साहित्यकारों और विचारकों को - इनमें सीधे निर्मल वर्मा, धर्मपाल, रामेश्वर मिश्र, ‘पंकज’, लक्ष्मीमल्ल सिंघवी और विद्यानिवास मिश्र जैसी हस्तियों का नाम लिया जा सकता है - भी अपने संघ संप्रदाय के प्रति नजरिए पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, जो जीवन से आध्यात्मिक पवित्र ‘स्पेस’ के नष्ट होने की अतिशय चर्चा और चिंता करते हैं। कुछ साहित्यकार और विचारक परोक्ष रूप से भी संघ संप्रदाय के बचाव में लगे रहते हैं। संघ संप्रदाय का सीधे या परोक्ष बचाव करके जहाँ इस ‘स्पेस’ को नहीं बचाया जा सकता, वहीं यह बचाव कुछ निजी उपलब्यिों के बदले में किया जाता है तो बौद्धिकों के लिए इससे ज्यादा पतन की बात नहीं हो सकती। साधुओं के लिए तो ऐसा सोचना ही पाप कहलाएगा।
(यह लेख 2001-2002 के आस-पास 'जनसत्ता' में छपा था और 'कट्टरता जीतेगी या उदारता' (राजकमल प्रकाशन, 2004) पुस्तक में संकलित है. तथाकथित धर्म संसदों में जो घृणा का प्रचार हो रहा है, उसके मद्देनजर यह लेख फिर से जारी किया गया है.)
Author introduction
Dr. Prem Singh
Dept. of Hindi
University of Delhi
Related:
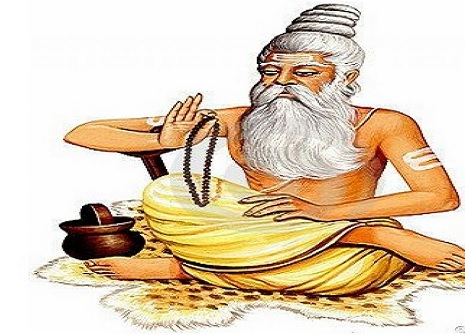
प्रतीकात्मक चित्र
ध्यान दिया जा सकता है कि साधुओं की बहुतायत के साथ, अथवा इस बहुतायत के कारण ही संस्कृत साहित्य से लेकर भक्तिकाल तक और लोक अनुभव में आज तक सच्चे साधु की पहचान का विमर्श भी बराबर मिलता है। इस विमर्श का निचोड़ यही है कि सच्चा साधु कोई एकाध ही होता है। बाकी सब लोक-परलोक का व्यवसाय करके, लोक विमर्श में कहा जाए तो ठगी करके, अपना पेट पालने से लेकर पूरा घर भरने वाले होते हैं। भारतीय समाज में आज भी ऐसे ही साधुओं की बहुतायत है। लोक विश्वास में इन्हें ढोंगी साधु कह कर पुकारने की परंपरा है। रंगे हुए सियार की तर्ज पर इन्हें रंगे हुए साधु भी कहा जाता है। ऐसे साधुओं से समाज को आक्रांत पाकर ही एक भक्त कवि ने कहा था:
‘सिंघन के लहँड़े नहीं, हंसन की नहीं पाँत।
लालन की नहीं बोरियाँ, साधु न चलें जमात।।’
साधु के स्वभाव में निहित गुणों में प्रेम और सार-निस्सार के बीच विवेक की योग्यता को केंद्रीय माना गया है। सांसारिकता में जीते हुए इन गुणों के चलते कोई व्यक्ति साधु होता है और इन गुणों के अभाव में सांसारिकता से विरक्त व्यक्ति भी साधु कहलाने का पात्र नहीं बनता। साधु भक्त भी हो सकता है, लेकिन भक्त जरूरी नहीं कि साधु भी हो। प्रेम-रहित भक्ति करने वाला व्यक्ति कोरा (कठोर पढ़ा जाए) भक्त ही होगा, जो आत्म-मुक्ति के फेर में ही पड़ा रह सकता है, जिसकी कोई वृहत्तर मानवीय सार्थकता नहीं होती। भक्त तत्त्वज्ञानी भी हो सकता है, लेकिन महान तत्वज्ञानी होने के बावजूद वह कई बार क्रूर और अविवेकी हो सकता है। इसे शंकराचार्य के उदाहरण से समझा जा सकता है। भारतीय दर्शन की चरम उपलब्धि माने जाने वाले अद्वैत दर्शन के प्रणेता शंकराचार्य वेद का उच्चारण करने वाले शूद्र की जीभ काट लेने और भूल से भी वेदमंत्र सुन लेने वाले शूद्र के कान में पिघला हुआ शीशा डालने का समर्थन करते हैं। शंकराचार्य महान ज्ञानमार्गी भक्त माने जाते हैं। भक्तिकाल के संतों को भी ज्ञानमार्गी भक्त कहा जाता है। कबीर ने ज्ञान की आँधी आने की बात कही है। सूक्ष्म तत्व-चिंतन भी उनके यहाँ कम नहीं हैः ‘पुहुप बास ते पातरा ऐसा तत्त अनूप’। लेकिन उनका ज्ञान कोरा तत्वज्ञान नहीं है। उसे प्रेम की अंतःसलिला सींचती है। मध्यकालीन संतों-भक्तों का यह प्रेम कोई अमूर्त चीज नहीं है, उसके ठोस मानवीय और सामाजिक संदर्भ हैं। आधुनिक युग में रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य विवेकानन्द ने वेदांत के मूल में प्रेम की प्रतिष्ठा कर उसे नव्यवेदांत के रूप में प्रस्तुत किया, तो उसका भी ठोस मानवीय और सामाजिक संदर्भ बनता है। विवेकानन्द ने तो शंकराचार्य के वेदांत दर्शन में शूद्रों के प्रति बरती गई प्रतिमानवीयता का प्रतिकार यह कह कर किया कि ‘भारत शूद्रों का होगा’।
प्रेम भक्ति में मानवीय अंतर्वस्तु का सृजन करता है, इसीलिए प्रेम को भक्ति के मूल में स्थापित किया गया है। यह अकारण नहीं है कि भक्ति के कई प्रकारों में प्रेममयी रागानुराग भक्ति को ही सर्वोच्च अर्थात् वास्तविक भक्ति माना गया है। प्रेम केवल ईश्वर या परम सत्ता के प्रति ही नहीं, चराचर जीवन-जगत के प्रति। ईश्वर के प्रति प्रेम की साधना से उसकी सृष्टि के प्रति प्रेम विकसित होगा या सृष्टि के प्रति प्रेम की साधना से ईश्वरी प्रेम विकसित होगा - यह पद्धति-भेद की बात हो सकती है। दोनों ही पद्धतियों में प्रेम एक कठिन साधना है। प्रेम के घर में पैठने के लिए अपना सिर उतार कर जमीन पर रखना पड़ सकता है। अतः कह सकते हैं कि सच्चा साधु प्रेम और करुणा के मानवीय गुण से उसके प्रतिलोम घृणा और क्रूरता से निरंतर संघर्ष करता है। सच्चा भक्त भी यही करता है। (इसी स्तर पर साधु और भक्त एकरूप हो जाते हैं।)
यह आसान साधना नहीं है, इसीलिए सच्चा साधु विरल माना गया है और सम्मानीय भी। समाज में साधु के सम्मान का एक और उच्चतर आयाम होता है, जहाँ वह पूज्यनीय हो जाता है - वह झूठ, फरेब, लिप्सा और क्षुद्रताओं से भरे संसार में उस पवित्र-लोक (सेकरेड स्पेस) का प्रतीक होता है, संसार से जिसकी मौजूदगी की कामना हर व्यक्ति के मन में कहीं न कहीं होती है और जिससे जुड़ कर वह दैवी पवित्रता से जुड़ने का अनुभव करता है।
अब उन साधुओं पर विचार करें जो साधु और भक्त होने का एक साथ दावा करते हैं। ये जमात में चलते हैं और उन्होंने आजकल भारतीय समाज को आक्रांत किया हुआ है। यहाँ संघ संप्रदाय (संघ परिवार) के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए आंदोलनरत साधुओं से आशय है। साधु के रूप में उनके चरित्र यानी साधुता को परखने के लिए संघ संप्रदाय के नेताओं का चरित्र देख लेना पर्याप्त होगा, जिनके वे अनुगामी बने हुए हैं। संघ संप्रदाय के नेताओं के चरित्र का यहाँ ज्यादा बखान करने की जरूरत नहीं है। वह सर्वविदित है। केवल यही कहा जा सकता है कि अपने विरोधियों के प्रति सदा घृणा से भरे रहने वाले, धार्मिक मामलों में भी झूठ व फरेब का निस्संकोच सहारा लेने वाले और सत्ता की लिप्सा व भोगवाद से परिचालित इन नेताओं के चरित्र में एक साधु के लिए कुछ भी अनुकरणीय नहीं हो सकता। साधु की भूमिका तो घृणा, झूठ, क्रूरता और भोगवादी प्रवृत्तियों से लड़ने की होती है। इसे उल्टी गंगा बहना ही कहेंगे कि साधु नेताओं का अनुकरण कर रहे हैं। वह भी, समग्रतः हिंदू धर्म और मुख्यतः राम का उद्धार करने के लिए! उद्धार की यह मुहिम आगे भी जारी रहनी है। काशी के शिव और मथुरा के कृष्ण का भी उद्धार होना है। यानी अभी आगे भी साधुओं को संघ संप्रदाय के नेताओं के पीछे चलना है।
संघ संप्रदाय का अपना घोषित एजेंडा और विचारधारा है, जिसे ब्राह्मणवाद की अभी तक की सर्वाधिक निकृष्ट अभिव्यक्ति (मेनीफेस्टेशन) कहा जा सकता है। ब्राह्मणवादी विचारधारा ने झूठ, फरेब और बदले की भावना का ऐसा प्रदर्शन इससे पहले कभी नहीं किया। अपने अच्छे-बुरे सभी दौरों में ब्राह्मणवाद ने जीवन का एक समग्र दर्शन प्रस्तुत करने की कोशिश की है। नए सामाजिक-ऐतिहासिक दबावों में जब आत्यंतिक मान्यताओं को स्थिर रखना असंभव हो गया, तो उसने समन्वयवाद का रास्ता भी अपनाया है। हालाँकि ब्राह्मणवादी समन्वयवाद भारतीय जीवन के सामाजिक-सांस्कृतिक बहुलतावाद का मुकम्मल उत्तर कभी नहीं बन पाया। विविध सामाजिक समूहों और अस्मिताओं पर अपना वर्चस्व बनाए रखने की उसकी मूल प्रवृत्ति बराबर बनी रही। लेकिन कहा जा सकता है कि ब्राह्मणवाद ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए हमेशा ही कड़ी बौद्धिक मशक्कत का परिचय दिया है।
संघ संप्रदाय का मामला अलग है। उसकी ‘विचारधारा’ में अगर कुछ अनुपस्थित है तो वह विचार है। इसकी भरपाई वह एक तरफ रणनीतियों से, जिनमें झूठ-फरेब सब कुछ जायज है, करता है और दूसरी ओर अन्य धर्मावलम्बियों के खिलाफ घृणा और बदले की भावना फैला कर। कहना न होगा कि इस मामले में उसने पश्चिम की फासीवादी-साम्राज्यवादी शक्तियों से गहरी सीख ली है। हेडगेवार, गोलवलकर, रज्जू भैया और और सुदर्शन सभी में यह परंपरा अक्षुण्ण देखने को मिलती है। ‘उदार’ वाजपेयी, ‘कट्टर’ आडवाणी, ‘हिंदू हित शिरोमणि’ बाल ठाकरे, ‘आचार्य’ गिरिराज किशोर, ‘परमहंस’ रामचंद्र दास, ‘साध्वी’ ऋतंभरा, ‘साध्वी’ उमा भारती, ‘साक्षी महाराज’, ‘धर्म शिरोमणि’ अशोक सिंघल और ‘धर्मवीर’ प्रवीन तोगड़िया आदि इसी परंपरा के ‘योग्य’ बच्चे रहे हैं। वैचारिक शून्यता की भरपाई का संघ संप्रदाय का एक और रास्ता है। उसने अपने को पूँजीवादी-उपभोक्तावादी विचारधारा की सेवा में समर्पित कर दिया है।
संघ संप्रदाय का आत्यंतिक लक्ष्य देश में अपना राजनैतिक-सांस्कृतिक वर्चस्व कायम करना है। यह उतनी चिंता का विषय नहीं है, जितना साधुओं का उलट आचरण। संघ संप्रदाय के अभियान को राजनीति और समाज में सक्रिय अन्य धाराएँ चुनौती दे सकती हैं, बल्कि यह चुनौती उसे मिल रही है। लेकिन साधुओं का आचरण मानव जीवन के उस पवित्र-लोक को नष्ट कर रहा है, जिसका जिक्र ऊपर किया गया है। जाहिर है, इसकी चिंता सबसे ज्यादा साधुओं को ही करनी है। उन्हें गंभीरता से यह सोचना है कि जिस आदर्श के साथ उनकी छवि या पहचान जुड़ी हुई है, क्या उसे वे संघ संप्रदाय के साथ जुड़ नष्ट कर देने को तैयार हैं? साथ ही उन साहित्यकारों और विचारकों को - इनमें सीधे निर्मल वर्मा, धर्मपाल, रामेश्वर मिश्र, ‘पंकज’, लक्ष्मीमल्ल सिंघवी और विद्यानिवास मिश्र जैसी हस्तियों का नाम लिया जा सकता है - भी अपने संघ संप्रदाय के प्रति नजरिए पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, जो जीवन से आध्यात्मिक पवित्र ‘स्पेस’ के नष्ट होने की अतिशय चर्चा और चिंता करते हैं। कुछ साहित्यकार और विचारक परोक्ष रूप से भी संघ संप्रदाय के बचाव में लगे रहते हैं। संघ संप्रदाय का सीधे या परोक्ष बचाव करके जहाँ इस ‘स्पेस’ को नहीं बचाया जा सकता, वहीं यह बचाव कुछ निजी उपलब्यिों के बदले में किया जाता है तो बौद्धिकों के लिए इससे ज्यादा पतन की बात नहीं हो सकती। साधुओं के लिए तो ऐसा सोचना ही पाप कहलाएगा।
(यह लेख 2001-2002 के आस-पास 'जनसत्ता' में छपा था और 'कट्टरता जीतेगी या उदारता' (राजकमल प्रकाशन, 2004) पुस्तक में संकलित है. तथाकथित धर्म संसदों में जो घृणा का प्रचार हो रहा है, उसके मद्देनजर यह लेख फिर से जारी किया गया है.)
Author introduction
Dr. Prem Singh
Dept. of Hindi
University of Delhi
Related:



