ज्योतिभाई देसाई, जो दो महीने में 98 वर्ष के होने वाले थे, का मंगलवार, 27 फरवरी, 2024 की शाम बड़ौदा में निधन हो गया। वह एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद्, जन आंदोलनों के सिपाही, उचित लेकिन अलोकप्रिय कारणों के समर्थन के स्तंभ थे।
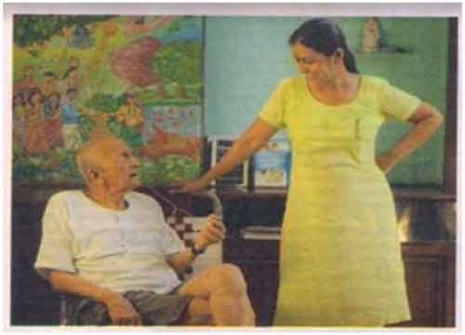
ज्योतिभाई एक प्रख्यात गांधीवादी थे, और स्वाति देसाई के पिता थे जो एआईडी की पहली साथी थीं। माइकल मझगांवकर और स्वाति देसाई एआईडी परिवार के बहुत करीबी सदस्य हैं, और उन्होंने गुजरात के नर्मदा जिले के आदिवासी गांव जूना मोजदा में रहकर बहुत प्रेरणादायक काम किया है। उनका काम उनके गांधीवादी माता-पिता, ज्योतिभाई और मालिनी बेन, डैनियल मजगांवकर और हंसा बहन की विरासत को जारी रखता है।
1950 के दशक में, ज्योतिभाई ने गुजरात के भावनगर जिले के सनोसरा गाँव में ग्रामीण विकास और शिक्षा के लिए स्थापित 'लोक भारती' नामक गांधीवादी संस्थान में एक शिक्षक के रूप में काम किया।
1960 के दशक में उन्हें जुगतराम दवे ने वेदच्छी में गांधी विद्यापीठ में शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। जुगतराम गांधी विद्यापीठ में शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के संस्थापक निदेशक थे।
ज्योतिभाई गांधी की दार्शनिक शिक्षाओं को व्यवहार में लाने के लिए कृतसंकल्प थे और पूरी लगन से इस काम में लगे हुए थे। 1957 में, उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से शिक्षा में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की, और 1975 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए आगे बढ़े।
उन्होंने 1975-1982 तक गुजरात राज्य माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड के साथ काम किया और 1990 से 1994 तक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) में सदस्य रहे। उन्होंने नई तालीम समिति, सेवाग्राम आश्रम की प्रशासनिक परिषद के सदस्य, इंदौर स्थित कस्तूरबा शिक्षा समिति के सदस्य, गांधी विद्यापीठ के प्रशासनिक निकाय के सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया और सेवाग्राम के अध्यक्ष जैसे विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य किया।'
वह वर्तमान शिक्षा प्रणाली के कट्टर आलोचक थे जो पूरी तरह से पूंजीगत लाभ पर आधारित है।
ज्योतिभाई के साथ यह साक्षात्कार 2023 में काउंटरकरेंट्स में प्रकाशित हुआ था।
------------------------------------------------
ज्योतिभाई देसाई महात्मा गांधी के समकालीन हैं जिनका जीवन गांधीवादी दर्शन के सिद्धांतों के प्रति सच्चा रहा है। ज्योतिभाई का जीवन-कार्य एक ऐसे स्थान पर विकसित हुआ है, जिसने समकालीन भारत के इतिहास में सांप्रदायिक हिंसा का सबसे खराब उदाहरण देखा है। फिर भी वह इस हिंसा के बीच भी दृढ़ता के साथ अहिंसा के दर्शन का पालन करते हैं। यहां गांधीजी, स्वतंत्रता संग्राम और शिक्षा दर्शन पर ज्योतिभाई के साथ बातचीत का पूरा विवरण दे रहे हैं।
ज्योतिभाई देसाई गांधी के उन चंद समकालीनों में से एक हैं जो आज भी जीवित हैं और हमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रत्यक्ष विवरण देते हैं। बंबई में जन्मे ज्योतिभाई भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण 1944 तक बाइकुला जेल में बंद रहे। बंबई में गांधीवादियों की सलाह पर वह ग्रामीणों के साथ काम करने के लिए गुजरात के वेदछी चले गए, जहां अंततः उनकी मुलाकात प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जुगतराम दवे से हुई। युवा जोश और चपलता के साथ, जो उनकी 92 साल की उम्र को भी कम कर देता है, ज्योतिभाई सुबह 4 बजे उठते हैं, खाना बनाते हैं और अपने निजी काम करते हैं, और अपने पुराने चरखे पर सूत कातने में चार घंटे बिताते हैं। वह अपना शेष दिन शांति से पढ़ने, लिखने और अपने राजनीतिक कार्यों में बिताते हैं। जो सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता उनसे मिलने आते हैं, उनके सामने वे बिना किसी समझौते के तीव्र विश्वास के साथ अपने विचार रखते हैं, लेकिन अपने विशिष्ट मधुर और नम्र तरीके से।
अपने दैनिक जीवन में, वह दृढ़ अनुशासन के साथ गांधी की मौलिक शिक्षाओं का पालन करते हैं। वह एक 'अराजकतावादी' है जो गर्व से एक ऐसे व्यक्ति के रूप में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करता है जो किसी भी ढांचे में बंधना नहीं चाहता। उनका मानना है कि हमारी संस्कृति व्यक्तिवादी नहीं है, बल्कि कई लोगों के निस्वार्थ योगदान की एक लंबी श्रृंखला का अंतिम परिणाम है। शायद यही वजह है कि सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र में वर्षों के अनुभव के बाद भी वे संस्मरण लिखना ज़रूरी नहीं समझते। जब कोई ज्योतिभाई से बात करता है, तो हम उनके शब्दों में मुक्ति के मजबूत मूल को समझ सकते हैं।
यह दृढ़ता से विश्वास करते हुए कि एक राष्ट्र और उसके लोग केवल शिक्षा के माध्यम से सच्ची स्वतंत्रता और स्वायत्तता प्राप्त कर सकते हैं, ज्योतिभाई ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा गांधीजी के 'नई तालीम' शैक्षिक दर्शन को साकार करने के लिए गतिविधियों और अभियानों में बिताया। आज भी ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं जिन्होंने गांधीजी के शिक्षा दर्शन को सही मायने में समझा हो और उस ज्ञान को व्यवहार में लाने का प्रयास किया हो।
1950 के दशक में, ज्योतिभाई ने गुजरात के भावनगर जिले के सनोसरा गाँव में ग्रामीण विकास और शिक्षा के लिए स्थापित 'लोक भारती' नामक गांधीवादी संस्थान में एक शिक्षक के रूप में काम किया। 1960 के दशक में उन्हें जुगतराम दवे ने वेदच्छी में गांधी विद्यापीठ में शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। जुगतराम गांधी विद्यापीठ में शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के संस्थापक निदेशक थे। ज्योतिभाई गांधी की दार्शनिक शिक्षाओं को व्यवहार में लाने के लिए कृतसंकल्प थे और पूरी लगन से इस काम में लगे हुए थे। 1957 में, उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से शिक्षा में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की, और 1975 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पूरा किया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और सेवाग्राम 'नई तालीम' समिति के अध्यक्ष, सेवाग्राम आश्रम की प्रशासनिक परिषद के सदस्य, इंदौर स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यापीठ शिक्षा समिति के सदस्य, प्रशासनिक निकाय के सदस्य जैसे विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य किया। वह वर्तमान शिक्षा प्रणाली के कट्टर आलोचक हैं जो पूरी तरह से पूंजीगत लाभ पर आधारित है।
ज्योतिभाई धारवाड़ में तुंगबादरा नदी में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ लोकप्रिय आंदोलन के मुख्य आयोजकों में से एक थे। जल, जमीन और जंगल की सुरक्षा के लिए लड़े गए कई लोकप्रिय विरोध प्रदर्शनों में उनकी मजबूत उपस्थिति रही है। वह नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी सबसे आगे हैं। 1989 में उन्हें मेधा पाटकर के साथ नर्मदा बचाओ आंदोलन के धरना स्थल से गिरफ्तार किया गया था। वह अंतर्राष्ट्रीय शांति ब्रिगेड में एक स्वयंसेवक भी थे। अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध के मैदान, मध्य अमेरिका में संघर्ष स्थलों पर आयोजित सत्याग्रहों ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था। पर्यावरण क्षरण, परमाणु हथियारों, बड़े बांधों और जन-विरोधी विकास उपायों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों में भाग लेने के लिए, उन्हें स्वतंत्रता के बाद भारत में पांच बार जेल भेजा गया था।
ज्योतिभाई ने राज्य-हिंसा और इसके हानिकारक विकास उपायों के खिलाफ लोकप्रिय संघर्षों और आंदोलनों में जीवन भर भागीदारी के रास्ते में कभी भी उम्र को आड़े नहीं आने दिया। सच्ची स्वतंत्रता, न्याय और सत्य की खोज में अटूट विश्वास के साथ, वह अपनी जीवन साथी मालिनी देसाई और बेटी स्वाति देसाई के साथ एक अनुकरणीय जीवन जी रहे हैं, जबकि मेधा पाटकर जैसी दृढ़ सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ एकजुटता से खड़े हैं। वह सूरत के आदिवासी गांव वेदछी से हमसे बातचीत करते हैं।
ए.के. शिबुराज: क्या आप हमें उस संदर्भ और परिस्थितियों का वर्णन कर सकते हैं जिसके कारण आपको स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना पड़ा?
ज्योतिभाई देसाई: मेरे पिता स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदार थे। उन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया और इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मैं तब छह साल का था। इसलिए मुझे किसी का सामना नहीं करना पड़ा।'
स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के दौरान विरोध। वास्तव में, मैंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी स्कूली शिक्षा छोड़ दी थी। उस समय, मैं बहुत उत्तेजित था और खतरनाक विचार रखता था। इसी अवधि के दौरान बॉम्बे प्रेसीडेंसी के तत्कालीन मुख्यमंत्री बी.जी. खेर ने मुझे गांवों में जाकर काम करने के लिए प्रेरित किया। इस तरह मैं वेदछी पहुंचा और असहयोग आंदोलन में सक्रिय हो गया। अन्यथा यह एक ऐसा रास्ता था जिसके साथ मैं कभी समझौता नहीं कर पाता। तब तक मेरा दृढ़ विश्वास था कि जिन्होंने गलतियाँ की हैं उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाद में तत्कालीन बॉम्बे मेयर युसुफअली मेहरअली की सिफारिश से मुझे कॉलेज में प्रवेश मिल गया। यह उनके हस्तक्षेप के कारण ही था कि मेरी राजनीतिक गतिविधियों के बावजूद मुझे प्रवेश से वंचित नहीं किया गया।
ए.के. शिबुराज: क्या आप कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने के तुरंत बाद वेदछी चले गए?
ज्योतिभाई देसाई: खार में गांधीजी के अनुयायियों के सौम्य अनुनय और सहयोग ने ग्रामीणों के बीच काम करने के मेरे निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समय मैंने गांधीवादी विचारों के बारे में पढ़ना शुरू ही किया था। शिक्षा के बारे में गांधीजी के दर्शन और ग्रामीणों के बीच उनके जीवन के तरीके को समझने में मुझे 2-3 साल लग गए। मैंने सौराष्ट्र क्षेत्र में आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में भाग लिया था। सेवक भोजराज द्वारा स्थापित बाल्कनजी बारी प्रशिक्षण संस्थान में मैंने शिक्षा के बारे में आगे सीखा। वेदच्छी पहुंचने के बाद, मैं बंबई से एक शहरवासी होने से पूरी तरह से बदल गया। नाना भाई और जुगतराम के कुशल मार्गदर्शन में शिविरों में प्राप्त प्रशिक्षण ने मुझे अच्छी स्थिति में पहुँचाया। तब तक जुगतराम, जो गांधी के भरोसेमंद शिष्य थे, ने 'स्वराज आश्रम' में नेतृत्व संभाल लिया था। वह गुजरात के दक्षिण में आदिवासी लोगों के निर्विवाद नेता भी थे।
ए.के. शिबुराज: आप एक निडर और साहसी व्यक्ति के रूप में बड़े हुए थे। गांधीजी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक दर्शन की ओर आपकी रुचि किस कारण से बढ़ी?
ज्योतिभाई देसाई: मैंने कभी किसी का आँख बंद करके अनुसरण नहीं किया। मैं किसी भी व्यक्ति को अंतिम शब्द मानने के लिए तैयार नहीं हूं- तब नहीं, अब नहीं। वेदच्छी पहुंचने पर मुझे बच्चों और छात्रों की जरूरतों से अवगत कराया गया। उन दिनों नानाभाई और जुगतराम शिक्षा में चरखे के महत्व के बारे में बात करते थे। हालाँकि यह कोई अंध विश्वास नहीं था। यदि चरखा कभी निरर्थक साबित हुआ तो वे उसे जलाने के लिए भी तैयार थे।
यह सच है कि गांधीजी का मुझ पर गहरा प्रभाव था। हालाँकि, मैं गांधीवादी शिक्षाविद् के रूप में नहीं जाना जाना चाहता। मैं आजादी से जीने की इच्छा रखता हूं। आज़ादी के बारे में सोचने और कार्य करने के लिए ही हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। स्वतंत्र विचार और कार्य में इस दृढ़ विश्वास के कारण मुझे कम से कम सात बार अपने कार्य संस्थान बदलने पड़े। मैं किसी भी कीमत पर सत्य और न्याय प्राप्त करना चाहता हूं।
गांधीजी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि शिक्षा का अर्थ अभ्यास के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान के माध्यम से एक मजबूत नैतिक स्थिति बनाना है। लेकिन आज, उथले सतही स्तर का ज्ञान प्राप्त करके, हम उपनिवेश होने से भी बदतर हो गए हैं।
ए.के. शिबुराज: आपका मानना है कि केवल शिक्षा के माध्यम से ही कोई राष्ट्र सच्ची स्वतंत्रता और स्वायत्तता प्राप्त कर सकता है। आज की शिक्षा प्रणाली, इसकी शिक्षाशास्त्र, इसकी सामग्री और उद्देश्यों के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
ज्योतिभाई देसाई: आज के शिक्षण संस्थान विनाशकारी हैं। बच्चों के लिए ज्ञान प्राप्त करने या स्वतंत्र रूप से सोचने की कोई गुंजाइश नहीं है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवा मस्तिष्क की जन्मजात प्रतिभाओं को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने का प्रयास करती है। माता-पिता को अपने बच्चों को ऐसे संस्थानों में भेजने से पहले दो बार सोचने की जरूरत है। मुख्यधारा की शिक्षा बच्चों के भीतर ज्ञान खोजने और प्राप्त करने के अंतर्निहित जुनून की परवाह किए बिना विकसित हो रही है। हमें एक राष्ट्रीय केंद्रीकृत शैक्षिक प्रणाली की नहीं, बल्कि विभिन्न स्वदेशी, सामुदायिक स्तर की शिक्षा प्रणालियों की आवश्यकता है, जो सत्य, न्याय और स्वतंत्रता के मूल में बनी हों।
एक बच्चे का पालन-पोषण अकेले माता-पिता द्वारा नहीं किया जा सकता। एक बच्चे के पालन-पोषण के लिए एक गाँव की आवश्यकता होती है। आज की शिक्षा प्रणाली बच्चों को असहाय और समर्थनहीन बनाती है। इससे बच्चे के भीतर यह बेहद गलत धारणा घर कर जाती है कि जीवन का मतलब नौकरी पाना और पैसा कमाना है। उसे पाना भी असंभव साबित हुआ है। आज की शिक्षा जिस दुनिया का वादा करती है वह मौजूद नहीं हो सकती। यही कारण है कि हार्दिक पटेल जैसे लोग बनते हैं।
ए.के. शिबूराज: आपने शिक्षण के सभी पुरातन और अप्रचलित तरीकों को त्यागकर छात्रों के बीच गुरु का पद ग्रहण किया। गांधी विद्यापीठ में छात्र यंत्रवत् रटकर नहीं सीख रहे थे। यह बाहरी वास्तविक दुनिया के संपर्क के माध्यम से है कि आपने छात्रों की चेतना के विकास के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार की है। मध्य प्रदेश में बुंदेल गुट के बीच अस्पृश्यता उन्मूलन के प्रयासों और पन्ना में लक्ष्मीपुर ओपन जेल के कैदियों के पुनर्वास के लिए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्रों के प्रयासों ने बहुत ध्यान आकर्षित किया था। मैंने पढ़ा है कि कैसे इन उदाहरणों को यूनिसेफ और ऑक्सफैम में प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में पढ़ाया जाता है। क्या आप हमें इसके बारे में और बता सकते हैं?
ज्योतिभाई देसाई: नवप्रवर्तन के ये प्रयास भारी बाधाओं और आलोचनाओं का सामना करते हुए किए गए। छात्रों की मुख्य चिंता परीक्षा और प्रमाणपत्रों को लेकर थी। हालाँकि जब इन चिंताओं को महत्व नहीं दिया गया तो वे पहले चिंतित थे, लेकिन लंबे समय में उन्होंने इससे होने वाले लाभों को पहचाना। सिकुड़ी हुई और कक्षाओं तथा पाठ्य पुस्तकों तक सीमित शैक्षिक व्यवस्था में, समाज से हमारे नाड़ी-संबंध कटते जा रहे हैं। जो छात्र भविष्य में इस राष्ट्र के राजनीतिक निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, उन्हें अपने चरित्र को ढालना चाहिए और अपने जीवन के आसपास के वास्तविक सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण के साथ सक्रिय जुड़ाव के साथ अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। छात्रों ने बांग्लादेशी शरणार्थी शिविरों में हैजा की रोकथाम के कार्यक्रमों में स्वेच्छा से भाग लिया। जयपुर बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए घर बनाना केवल एक दान नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक कार्य था। यहीं शिक्षा का असली लक्ष्य निहित है।
ए.के. शिबुराज: उस समय भी आलोचनाएँ थीं कि नई तालीम शैक्षिक दर्शन, जिसे गांधीजी ने प्रोत्साहित किया था, को उसके उचित सार में लागू नहीं किया गया था। कई उदाहरणों पर, उत्पादक कार्य अलग से सिखाया जा रहा था।
ज्योतिभाई देसाई: यह विभिन्न विषयों में ज्ञान प्राप्त करने वाले उद्यम के रूप में शिक्षा की संकीर्ण समझ का नकारात्मक परिणाम है। विषयों के कृत्रिम पृथक्करण के माध्यम से शिक्षण पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण है! यह निश्चित रूप से शिक्षा का लक्ष्य नहीं है।
जब मैंने अपने छात्रों को जामुन फल तोड़ने के लिए भेजा, तो वे वास्तव में विभिन्न चीजें सीख रहे थे। इस सीखने को भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान आदि जैसी श्रेणियों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अलग-अलग विषय क्षेत्रों में सीखने के इस विभाजन से कम से कम शिक्षा के शुरुआती चरणों में बचना होगा। अन्यथा यह ज्ञान प्राप्ति की व्यापकता में बाधा उत्पन्न करेगा। वास्तविक शिक्षा पाठ्यक्रम की दीवारों से परे है। गुजरात के कई स्कूलों में नई तालीम को गलत तरीके से लागू किया जा रहा है। यह केवल इसलिए है क्योंकि मुझे जुगतराम जैसे मजबूत नेताओं का समर्थन प्राप्त था कि मैं गांधी विद्यापीठ में नई तालीम को इसके वास्तविक मूल को दूर किए बिना लागू कर सका।
जुगतराम भाई एक अलग और असाधारण प्रजाति के नेताओं से थे। उन्होंने कभी भी गांधी सहित किसी का भी आंख मूंदकर अनुसरण नहीं किया। जब भी वह खुद को गलत पाते तो माफी मांगने और आवश्यक संशोधन करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे।
ए.के. शिबुराज: क्या उस समय के हमारे राजनेताओं और धार्मिक सुधारकों ने हमारी शिक्षा प्रणाली के निर्माण में औपनिवेशिक शक्तियों के प्रभावों को नजरअंदाज किया था?
ज्योतिभाई देसाई: भारत के इतिहास में, स्वेच्छा से शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी लेने वाले एकमात्र नेता बॉम्बे प्रेसीडेंसी के मुख्यमंत्री बी.जे. खेर थे। भारत की पहली केंद्रीय सरकार ने मौलाना आज़ाद को यह जिम्मेदारी केवल इसलिए सौंपी क्योंकि वे शिक्षा को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार के समय से ही हमारे देश में शिक्षा के महत्व को नजरअंदाज किया गया। हर कोई सत्ता में रुचि रखता था।
ए.के. शिबुराज: क्या यह उपेक्षा गांधीजी के जीवनकाल में भी थी?
ज्योतिभाई देसाई: लेकिन गांधीजी इस दावे से पूरी तरह असहमत थे। राजनीतिक सत्ता हासिल करने में रुचि रखने वाली कांग्रेस कार्य समिति ने भी गांधीजी की राय की उपेक्षा की। आजादी के तुरंत बाद कांग्रेस को भंग करने के सुझाव पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए स्वाभाविक रूप से राजनीतिक सत्ता का पीछा करने वालों ने उनकी शिक्षा नीतियों को कूड़ेदान में डालने के बारे में दोबारा नहीं सोचा। एक व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे दूसरे व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं है। मैं सत्ता के सभी कृत्यों के खिलाफ हूं। शिक्षा शासक वर्ग के हितों के अनुरूप भावी पीढ़ियों को विकृत करने का साधन नहीं होनी चाहिए।
ए.के. शिबुराज: 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में पूरे भारत में नई तालीम लागू करने का निर्णय लिया गया था। आज़ादी के बाद भारत में सत्ता में आई कांग्रेस सरकार इस फैसले को टालने में कैसे कामयाब रही?
ज्योतिभाई देसाई: हमें याद रखना चाहिए कि अधिकांश राजनेता चतुर और चालाक हैं। इसलिए, वे सावधानी से अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। उनकी अधिकांश नीतियाँ प्रतिगामी प्रकृति की थीं। खादी आयोग का गठन वर्ष 1950 में किया गया था। अनुदान प्राप्त करने के लिए आयोग की अनुमति आवश्यक थी। गांधीजी के मुद्रक स्वामी आनंद आश्चर्यचकित थे और उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया था कि दिल्ली में बैठा एक आयोग उनके घर के अंदर उत्पादित खादी को कैसे प्रमाणित कर सकता है। आपको अपने घर में काटी गई खादी के लिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता क्यों है? क्या आपको अपने घर में उत्पादित घी और दूध के लिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? हमें अच्छी गुणवत्ता वाली खादी की जरूरत है, न कि खादी बोर्ड से मिलने वाले वेतन और अन्य परिलब्धियों की। यह बात यूजीसी पर भी लागू होती है. मुझे कॉलेज चलाने के लिए यूजीसी द्वारा अनुमोदन और मान्यता की आवश्यकता क्यों है? जैसे खादी आयोग ने योजनाबद्ध तरीके से खादी को नष्ट कर दिया है, वैसे ही यूजीसी शिक्षा को नष्ट करने की राह पर है। आज़ाद भारत में ऐसी बहुत सी बेतुकी हरकतें हो रही हैं।
जो राज्य शिक्षा और छात्रों की जरूरतों के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ है, वह बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा है और कुछ लोगों को प्रमाणपत्र बांट रहा है। राज्य के दोषपूर्ण दृष्टिकोण के कारण नई तालीम नष्ट हो गई। सत्ता की अपनी अंधी चाहत में, हमारे राजनेता शिक्षा के मूल्य और लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव को समझने में विफल रहे हैं।
ए.के. शिबूराज: क्या आप यह सुझाव दे रहे हैं कि राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए?
ज्योतिभाई देसाई: शिक्षा को सरकार के दायरे से बाहर करना होगा। राज्य की भूमिका शिक्षा के लिए आवश्यक भौतिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने तक सीमित होनी चाहिए। छात्रों को क्या सीखना चाहिए या कैसे सीखना चाहिए, इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। परन्तु मेरा यह दृष्टिकोण कभी स्वीकार नहीं किया जायेगा और न ही लागू किया जायेगा। छात्रों और शिक्षकों की एक पीढ़ी जो राज्य के नियंत्रण से मुक्त हो सकती है, वही सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि शिक्षा को बहुराष्ट्रीय निगमों के हवाले कर दिया जाना चाहिए या इसे अंधाधुंध निजीकरण के लिए खुला रखा जाना चाहिए। अफसोस की बात है कि अभी यही हो रहा है। दरअसल, शिक्षा का अधिकार कानून की आड़ में शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है।
आज की शिक्षा नीतियां केवल पहले से मौजूद विषम संरचनाओं को मजबूत कर रही हैं जो कुछ अमीर लोगों के हाथों में सत्ता हासिल करते हुए कई छात्रों को हाशिए पर धकेल रही हैं। वहां नैतिकता या मूल्यों के लिए कोई जगह नहीं है। यह जीवन के लिए भी हानिकारक है! यह लोगों की भलाई को ख़तरे में डाल देगा। इस खतरनाक व्यवस्था के पीछे पूंजी ही एकमात्र प्रेरक शक्ति है। छात्र स्वतंत्र नहीं हैं; वे निर्विवाद और विनम्र होने के साँचे में ढले हुए हैं। अदृश्य जेलें उनका इंतजार कर रही हैं।
ए.के. शिबुराज: शिक्षा में निजी पूंजी के हस्तक्षेप से छात्रों को मिलने वाली भौतिक सुविधाओं में उल्लेखनीय अंतर आया है। आम धारणा यह है कि प्रौद्योगिकी ने शिक्षा के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन ला दिया है। शिक्षकों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर पुनर्विचार किया जा रहा है। आप इन परिवर्तनों को कैसे समझते हैं?
ज्योतिभाई देसाई: इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन में सकारात्मक अभिव्यक्तियाँ लायी हैं। हालाँकि, इसकी शक्तियों पर आँख मूँदकर विश्वास करना बेहद खतरनाक साबित होगा। तकनीकी प्रतिभा का दावा करने वाले अधिकांश उपाय वास्तव में हमारे जीवन की गति को तेज करके और हमें एक-दूसरे के साथ अधिक प्रतिस्पर्धी बनाकर मुनाफा बढ़ाने के शॉर्टकट हैं। यह मानना गलत और खतरनाक है कि तकनीकी प्रगति ही हमारी सभी सामाजिक समस्याओं का समाधान होगी। ऐसी स्थितियों में जो हमारी नैतिक चेतना के आधार पर निर्णय लेने की मांग करती हैं, तकनीक बेकार होगी। मुझे नहीं लगता कि प्रौद्योगिकी न्याय और समानता का मार्ग प्रशस्त करेगी। नैतिक दिशा-निर्देश से रहित लक्ष्यहीन जीवन अंततः विनाश की ओर ले जाएगा। यह हमारी जीवन-शक्ति का विनाश है! तकनीकी उन्नति के नाम पर शिक्षण संस्थानों में अपनाए गए कुछ उपाय पूरी तरह से फर्जी हैं!
ए.के. शिबूराज: शिक्षा में आपका हस्तक्षेप ऐसे समय में हुआ जब भारत में जाति व्यवस्था बेहद मजबूत थी, जाति-आधारित हिंसा के निरंतर कृत्यों के माध्यम से हमारे समाज के एक वर्ग को हाशिए पर रखा गया था और गंभीर घाव दिए गए थे। इस काल में प्रचलित सवर्ण वर्चस्व से आपने कैसे निपटा?
ज्योतिभाई देसाई: भारतीय ब्राह्मण भारत के संदर्भ में अस्पृश्यता और पूर्वाग्रही पक्षपात की प्रथा के माध्यम से दासता के पश्चिमी तरीकों का उपयोग कर रहे थे। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत दास प्रथा को संस्थागत बना दिया गया है। गांधीजी आश्रम के भीतर इस प्रणाली के चलन के सख्त खिलाफ थे। आश्रम के प्रबंधक मगनलाल, जिन्होंने आश्रम में शामिल होने आए हरिजन परिवार के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया था, को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालाँकि, वह छह महीने बाद एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में वापस लौटे। गांधीजी का स्पष्ट दृष्टिकोण था कि जाति व्यवस्था के खतरे से कैसे निपटा जाए।
मैं एक और उदाहरण बताता हूँ। मेरे स्कूल में ग्राम प्रधान के बेटे ने घोषणा की कि मेरी कक्षा का हरिजन छात्र भरे हुए बर्तनों से पानी नहीं पी सकता। उसने यह भी घोषणा की कि उसके अलावा कोई भी इसे नहीं पी सकता। मैंने उससे कहा कि उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। आख़िर निराश होकर वह बर्तन तोड़ने लगा। उसने करीब सात मटके तोड़े। अंततः उसने यह पूर्वाग्रह बंद कर दिया। कक्षा भ्रमण के दौरान, उसने हममें से बाकी लोगों के साथ भी भोजन साझा किया।
मैंने कभी भी जाति व्यवस्था के ख़िलाफ़ अभियान का नेतृत्व नहीं किया। मेरी जीवनशैली, मेरे विश्वास और व्यवहार ही मेरे शस्त्रागार थे। जिन लोगों ने गलत किया है उनके लिए हमेशा धार्मिकता की ओर वापस जाने का रास्ता खोजने की जगह होती है। अन्यायी हमेशा खुद को सुधार सकता है और न्याय के रास्ते पर लौट सकता है।
ए.के. शिबूराज: अम्बेडकर ने गाँवों को अज्ञानता का अड्डा और जातिगत उत्पीड़न के सबसे क्रूर रूपों से घिरा हुआ पाया था। दलितों का शहरों की ओर पलायन वास्तव में उनके मुक्ति आंदोलन का एक हिस्सा था। आज भी, शहर सुरक्षित स्थान हैं जहां निचली जाति के लोग 'इंसान' के रूप में रह सकते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
ज्योतिभाई देसाई: सबसे पहले, शहरों में जाति से रहित कोई नई मूल्य प्रणाली नहीं है। हाँ, गाँवों में पाई जाने वाली जातिगत प्रथाओं का शहरों में पालन करना व्यावहारिक रूप से कठिन है। इसलिए, शहरों में जाति-व्यवस्था अपेक्षाकृत कमज़ोर है। हालाँकि, शहरों में भी जाति के आधार पर निवास और भोजन देने या उपलब्ध कराने से इनकार करने के उदाहरण अभी भी मौजूद हैं।
अंबेडकर की बात करें तो वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें जाति के कारण जीवन में बहुत सारे नकारात्मक अनुभवों से गुजरना पड़ा। इसने उनके जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे व्यक्तिगत उथल-पुथल मच गई। उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएँ उन्हें लगातार हो रही चोट का परिणाम हैं। यह उनके दार्शनिक और बौद्धिक विचारों में परिलक्षित होता है।
ए.के. शिबूराज: जाति-व्यवस्था पर गांधी और अंबेडकर के विचार अलग-अलग थे। क्या हम कह सकते हैं कि गांधी अम्बेडकर को समझने में असफल रहे?
ज्योतिभाई देसाई: गांधीजी ने कभी भी जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। गांधीजी की चिंताओं का केंद्र मनुष्य था। उनका उद्देश्य हमारे बीच मौजूद विभिन्न भेदभावों के बावजूद मानवता को एक साथ लाना था। गांधीजी ने अम्बेडकर की उपेक्षा या अवहेलना नहीं की। हालाँकि अम्बेडकर कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, फिर भी गांधीजी ने मंत्री पद के लिए उनके नाम की सिफारिश की। गांधीजी ने संविधान निर्माण प्रक्रिया में अंबेडकर की भागीदारी और योगदान भी सुनिश्चित किया।
ए.के. शिबूराज: क्या आपको लगता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान और इसके द्वारा प्रस्तुत लोकतांत्रिक आदर्शों को गंभीर खतरा है? क्या हम अधिनायकवाद के चरणों में विविधता और धर्मनिरपेक्षता के अपने मूल्यों को त्याग रहे हैं? खुली बहस और बातचीत का अभाव परेशान करने वाला है, है ना?
ज्योतिभाई देसाई: स्वतंत्रता के बाद भारत में विभिन्न ऐतिहासिक मोड़ों पर लोकतंत्र को कई हमलों का सामना करना पड़ा। एक राष्ट्र और उसके लोग जिन्होंने आज़ादी में आज़ादी का सपना देखा था, उन्हें इसके पीछे विनाश और ध्रुवीकरण और विभाजन मिला। लोग यह देखकर हैरान रह गए कि जिन नेताओं को उन्होंने देश का नेतृत्व करने के लिए चुना था, वे बेशर्मी से सत्ता और धन के पीछे भाग रहे थे। मुझे डर है कि आज हमारे देश पर अधिनायकवाद अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। यह निर्णय लिया जा रहा है कि केवल एक ऊंची आवाज सुनी जाएगी, जिससे हमारे बाकी विरोधात्मक विलाप को शांत कर दिया जाएगा। जो राष्ट्र असहाय है और सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करने से डरता है, वह अंधकार के युग में प्रवेश का प्रतीक है। मैं फिर से दोहराता हूं कि हम एक ऐसी पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं जो कभी भी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करेगी।
केंद्र सरकार के अधीन युवाओं के कौशल विकास की योजना क्यों है? यह हमारे युवाओं को भविष्य में किसकी सेवा में काम करना है, इसके बारे में क्या संदेश देता है? स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए जगह कहां है? अंतिम उद्देश्य व्यक्तियों को विभिन्न उद्योगों में काम करने वाली बिना सोचे-समझे मशीनों में बदलना है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे देश में विविध कार्य कौशल का समृद्ध संसाधन मौजूद है। हमारे पास बीजों के संरक्षण, मृदा संरक्षण, नवाचार और शिल्प के संबंध में ज्ञान का मूल्यवान भंडार है। ये कौशल कोई ऐसी चीज़ नहीं हैं जो हमने राज्य एजेंसियों के किसी संस्थान में दाखिला लेकर सीखी है। हमारे देश में कौशल की कभी कमी नहीं रही। बेरोजगारी का कारण निश्चय ही यह नहीं है।
ए.के. शिबुराज: आपने लगातार शक्तिशाली लोगों के निरंकुश व्यवहार का विरोध किया है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को चुप कराने के किसी भी प्रयास के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। क्या आपके इस स्पष्टवादी व्यवहार के कारण अन्य व्यक्तियों के साथ मनमुटाव हुआ है? मैंने सुना है कि आप आचार्य विनोबा भावे से खुले तौर पर असहमत थे।
ज्योतिभाई देसाई: महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन किसके लिए लड़ रहा है? आप किसके हक के लिए आवाज उठा रहे हैं? जब हमारी प्रतिक्रियाएँ हमारे अहंकार को प्रतिबिंबित करती हैं तो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। विनोबा भावे ने एक बार मुझसे उड़ीसा में सर्वोदय संस्थान की शैक्षिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए कहा। उन्होंने उड़ीसा के सीएम के अनुरोध के आधार पर यह निर्देश दिया था। विनोबा इंदिरा की शक्ति के वायरस से प्रभावित थे और भूल गए थे कि वे उसी शक्ति के साथ मिलीभगत कर रहे हैं जिसके खिलाफ उन्होंने अब तक विरोध किया था। मैंने उन्हें याद दिलाया कि सर्वोदय का मिशन और सत्ता की जिन संरचनाओं के साथ वह मुझसे काम करने के लिए कह रहे थे, वे कभी एक साथ नहीं चल सकते। जब उन्होंने मुझे और समझाया तो मैंने उनसे कहा कि वह पागलपन की बात कर रहे हैं। वह लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे जयप्रकाश नारायण से दूरी बनाते हुए इंदिरा के करीब बढ़ रहे थे। हवाई अड्डे पर इंदिरा से मिलने गए विनोबा ने बार-बार आग्रह करने के बाद भी जेपी की मृत्यु शय्या पर उनसे मिलने से इनकार कर दिया।
सत्ता लोगों को भ्रष्ट करती है। गांधी जो यह जानते थे वे दिल्ली नहीं बल्कि नोआखाली गए। दिल्ली में जो लोग सत्ता में हैं, उन्हें ही लोगों के पास आना चाहिए। मैं यह बात मेधा को हर समय बताता हूं कि दिल्ली में सत्ता में बैठे लोगों को यहां के हालात समझने के लिए नर्मदा आना चाहिए। अन्यथा राज्य की निरंकुश शक्ति अंततः लोगों की स्वतंत्रता के अधिकार को छीन लेगी।
ए.के. शिबुराज: नर्मदा में आपके हस्तक्षेप और सक्रियता के पीछे क्या परिस्थिति थी? क्या आपको यह देखकर निराशा हुई है कि अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलकर विरोध करने वाले लोग अपने उद्देश्यों तक पहुँचने में असफल हो जाते हैं?
ज्योतिभाई देसाई: जब लोग राज्य मशीनरी के अधिकार और अहंकार से उत्पीड़न से लड़ रहे थे तो मैं कैसे खड़ा होकर देख सकता हूँ? लोकप्रिय विरोध आंदोलनों में जीत और हार का आकलन करना आसान नहीं है। नर्मदा विरोध प्रदर्शन के कारण विकास संबंधी वादों के खोखलेपन और असहाय पीड़ितों और आम आदमी पर होने वाले अन्याय पर राष्ट्रीय स्तर पर जोरदार चर्चा हुई। यह विरोध बड़ी विकास परियोजनाओं के परिणामस्वरूप पर्यावरणीय विविधता और आम लोगों के जीवन के बड़े पैमाने पर विनाश के बारे में लोकप्रिय चेतना को समझाने में सहायक था। मुझे लगता है कि यह विरोध यह दिखाने में सफल रहा कि सरकार वास्तव में कैसे चंद शक्तिशाली समूहों के हितों का समर्थन कर रही थी और देश के संसाधनों के विनाश का मार्ग प्रशस्त कर रही थी।
ए.के. शिबुराज: 21वीं सदी पर्यावरणीय स्थिरता की चिंताओं और विभिन्न तात्कालिक चुनौतियों से घिरी हुई है जो मानवता के अस्तित्व पर हमला करती हैं। चूंकि ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण विनाश से संपूर्ण जीवन प्रणालियों के अस्तित्व को खतरा है, आम आदमी अभी भी जीवित रहने की बुनियादी जरूरतों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है। बाहर निकलने का रास्ता क्या है?
ज्योतिभाई देसाई: मानवता भयानक संकट के कगार पर है। लेकिन इस समस्या का समाधान कोई एक देश नहीं ढूंढ सकता। आगे का रास्ता खोजने के लिए पूरे विश्व समुदाय को एक साथ आना होगा, एकजुट होना होगा। यह कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हम निष्क्रिय बने रहें।
गांधी की प्रासंगिकता इस संदर्भ में बढ़ती जा रही है, जहां मानव समुदाय गंभीर पर्यावरणीय संकटों का सामना कर रहे हैं। उनकी दूरदर्शी दृष्टि को हिंद स्वराज में दर्शाया गया है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, सत्ता की दौड़ में गांधी की उपेक्षा की गई। गांधीजी ने हमें पहले ही आगाह कर दिया था कि औद्योगिक क्रांति की अस्थायी प्रगति पर आधारित उपभोक्तावादी लालच हमारे भविष्य के लिए बहुत महंगी साबित होगी। क्या हम अब भी ग्राम स्वराज के महत्व को नजरअंदाज कर सकते हैं? अमेरिका और यूरोप की संस्कृतियों की बिना सोचे-समझे नकल करना बेहद बेवकूफी है, सत्ता में बैठे लोगों के खाली खोखले वादों से एक पूरी पीढ़ी को मूर्ख बनाया जा रहा है। हम अब अमेरिकी मॉडल का अनुसरण करने की स्थिति में नहीं हैं।'
ए.के. शिबूराज: आपके पास स्वतंत्रता संग्राम की अवधि, गांधीजी के साथ आपके संबंध, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान, न्याय और लोकतंत्र की खोज में आपके द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों और आंदोलनों से संबंधित अनुभवों का खजाना है। इतने सारे विविध अनुभव, दृष्टिकोण, विचार... फिर भी आपने एक संस्मरण लिखकर इसे लिखने के बारे में क्यों नहीं सोचा?
ज्योतिभाई देसाई: देखिए, भारतीय संस्कृति किसी व्यक्ति के योगदान पर गर्व नहीं करती है। यह बहुत से लोगों के साझा और संयुक्त प्रयासों का नतीजा है और इसमें बहुत सारा आपसी लेन-देन शामिल है। मैं जो व्यक्ति हूं, उसमें 'मैं' का ज्यादा महत्व नहीं है। यहां तक कि कृष्ण और राम को भी अन्य कारणों की पूर्ति के लिए यहां बुलाया गया था।
मेरा जीवन और मेरा कार्य मेरे अंदर मौजूद किसी विशेष गुण का परिणाम नहीं है। इसके बजाय यह सब प्रयासों के संगम और कई व्यक्तियों के विभिन्न पहलुओं के पूर्ण समर्थन के कारण संभव हुआ, जो एक बड़े उद्देश्य के लिए मजबूती से एक साथ खड़े थे। मैं पूरी आजादी से रहना चाहता हूं। मैं गांधीवादी या शिक्षाशास्त्री नहीं हूं। मुझे ढाँचों में बंधनों में नहीं बंधना है। मैं उस आज़ादी का आनंद लेता हूँ जो सत्ता की भ्रष्ट इच्छा और प्रभाव से अलग खड़े होने से मिलती है। मैं स्वतंत्र नागरिकों वाले एक स्वतंत्र राष्ट्र का सपना देखता हूं।
ए.के. शिबूराज एक स्वतंत्र पत्रकार हैं
(अपर्णा ईश्वरन द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित, सबरंग टीम द्वारा हिंदी में अनुवादित)
सौजन्य: काउंटरकरंट
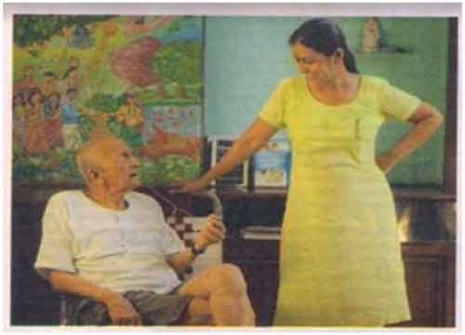
ज्योतिभाई एक प्रख्यात गांधीवादी थे, और स्वाति देसाई के पिता थे जो एआईडी की पहली साथी थीं। माइकल मझगांवकर और स्वाति देसाई एआईडी परिवार के बहुत करीबी सदस्य हैं, और उन्होंने गुजरात के नर्मदा जिले के आदिवासी गांव जूना मोजदा में रहकर बहुत प्रेरणादायक काम किया है। उनका काम उनके गांधीवादी माता-पिता, ज्योतिभाई और मालिनी बेन, डैनियल मजगांवकर और हंसा बहन की विरासत को जारी रखता है।
1950 के दशक में, ज्योतिभाई ने गुजरात के भावनगर जिले के सनोसरा गाँव में ग्रामीण विकास और शिक्षा के लिए स्थापित 'लोक भारती' नामक गांधीवादी संस्थान में एक शिक्षक के रूप में काम किया।
1960 के दशक में उन्हें जुगतराम दवे ने वेदच्छी में गांधी विद्यापीठ में शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। जुगतराम गांधी विद्यापीठ में शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के संस्थापक निदेशक थे।
ज्योतिभाई गांधी की दार्शनिक शिक्षाओं को व्यवहार में लाने के लिए कृतसंकल्प थे और पूरी लगन से इस काम में लगे हुए थे। 1957 में, उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से शिक्षा में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की, और 1975 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए आगे बढ़े।
उन्होंने 1975-1982 तक गुजरात राज्य माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड के साथ काम किया और 1990 से 1994 तक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) में सदस्य रहे। उन्होंने नई तालीम समिति, सेवाग्राम आश्रम की प्रशासनिक परिषद के सदस्य, इंदौर स्थित कस्तूरबा शिक्षा समिति के सदस्य, गांधी विद्यापीठ के प्रशासनिक निकाय के सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया और सेवाग्राम के अध्यक्ष जैसे विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य किया।'
वह वर्तमान शिक्षा प्रणाली के कट्टर आलोचक थे जो पूरी तरह से पूंजीगत लाभ पर आधारित है।
ज्योतिभाई के साथ यह साक्षात्कार 2023 में काउंटरकरेंट्स में प्रकाशित हुआ था।
------------------------------------------------
ज्योतिभाई देसाई महात्मा गांधी के समकालीन हैं जिनका जीवन गांधीवादी दर्शन के सिद्धांतों के प्रति सच्चा रहा है। ज्योतिभाई का जीवन-कार्य एक ऐसे स्थान पर विकसित हुआ है, जिसने समकालीन भारत के इतिहास में सांप्रदायिक हिंसा का सबसे खराब उदाहरण देखा है। फिर भी वह इस हिंसा के बीच भी दृढ़ता के साथ अहिंसा के दर्शन का पालन करते हैं। यहां गांधीजी, स्वतंत्रता संग्राम और शिक्षा दर्शन पर ज्योतिभाई के साथ बातचीत का पूरा विवरण दे रहे हैं।
ज्योतिभाई देसाई गांधी के उन चंद समकालीनों में से एक हैं जो आज भी जीवित हैं और हमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रत्यक्ष विवरण देते हैं। बंबई में जन्मे ज्योतिभाई भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण 1944 तक बाइकुला जेल में बंद रहे। बंबई में गांधीवादियों की सलाह पर वह ग्रामीणों के साथ काम करने के लिए गुजरात के वेदछी चले गए, जहां अंततः उनकी मुलाकात प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जुगतराम दवे से हुई। युवा जोश और चपलता के साथ, जो उनकी 92 साल की उम्र को भी कम कर देता है, ज्योतिभाई सुबह 4 बजे उठते हैं, खाना बनाते हैं और अपने निजी काम करते हैं, और अपने पुराने चरखे पर सूत कातने में चार घंटे बिताते हैं। वह अपना शेष दिन शांति से पढ़ने, लिखने और अपने राजनीतिक कार्यों में बिताते हैं। जो सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता उनसे मिलने आते हैं, उनके सामने वे बिना किसी समझौते के तीव्र विश्वास के साथ अपने विचार रखते हैं, लेकिन अपने विशिष्ट मधुर और नम्र तरीके से।
अपने दैनिक जीवन में, वह दृढ़ अनुशासन के साथ गांधी की मौलिक शिक्षाओं का पालन करते हैं। वह एक 'अराजकतावादी' है जो गर्व से एक ऐसे व्यक्ति के रूप में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करता है जो किसी भी ढांचे में बंधना नहीं चाहता। उनका मानना है कि हमारी संस्कृति व्यक्तिवादी नहीं है, बल्कि कई लोगों के निस्वार्थ योगदान की एक लंबी श्रृंखला का अंतिम परिणाम है। शायद यही वजह है कि सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र में वर्षों के अनुभव के बाद भी वे संस्मरण लिखना ज़रूरी नहीं समझते। जब कोई ज्योतिभाई से बात करता है, तो हम उनके शब्दों में मुक्ति के मजबूत मूल को समझ सकते हैं।
यह दृढ़ता से विश्वास करते हुए कि एक राष्ट्र और उसके लोग केवल शिक्षा के माध्यम से सच्ची स्वतंत्रता और स्वायत्तता प्राप्त कर सकते हैं, ज्योतिभाई ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा गांधीजी के 'नई तालीम' शैक्षिक दर्शन को साकार करने के लिए गतिविधियों और अभियानों में बिताया। आज भी ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं जिन्होंने गांधीजी के शिक्षा दर्शन को सही मायने में समझा हो और उस ज्ञान को व्यवहार में लाने का प्रयास किया हो।
1950 के दशक में, ज्योतिभाई ने गुजरात के भावनगर जिले के सनोसरा गाँव में ग्रामीण विकास और शिक्षा के लिए स्थापित 'लोक भारती' नामक गांधीवादी संस्थान में एक शिक्षक के रूप में काम किया। 1960 के दशक में उन्हें जुगतराम दवे ने वेदच्छी में गांधी विद्यापीठ में शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। जुगतराम गांधी विद्यापीठ में शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के संस्थापक निदेशक थे। ज्योतिभाई गांधी की दार्शनिक शिक्षाओं को व्यवहार में लाने के लिए कृतसंकल्प थे और पूरी लगन से इस काम में लगे हुए थे। 1957 में, उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से शिक्षा में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की, और 1975 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पूरा किया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और सेवाग्राम 'नई तालीम' समिति के अध्यक्ष, सेवाग्राम आश्रम की प्रशासनिक परिषद के सदस्य, इंदौर स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यापीठ शिक्षा समिति के सदस्य, प्रशासनिक निकाय के सदस्य जैसे विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य किया। वह वर्तमान शिक्षा प्रणाली के कट्टर आलोचक हैं जो पूरी तरह से पूंजीगत लाभ पर आधारित है।
ज्योतिभाई धारवाड़ में तुंगबादरा नदी में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ लोकप्रिय आंदोलन के मुख्य आयोजकों में से एक थे। जल, जमीन और जंगल की सुरक्षा के लिए लड़े गए कई लोकप्रिय विरोध प्रदर्शनों में उनकी मजबूत उपस्थिति रही है। वह नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी सबसे आगे हैं। 1989 में उन्हें मेधा पाटकर के साथ नर्मदा बचाओ आंदोलन के धरना स्थल से गिरफ्तार किया गया था। वह अंतर्राष्ट्रीय शांति ब्रिगेड में एक स्वयंसेवक भी थे। अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध के मैदान, मध्य अमेरिका में संघर्ष स्थलों पर आयोजित सत्याग्रहों ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था। पर्यावरण क्षरण, परमाणु हथियारों, बड़े बांधों और जन-विरोधी विकास उपायों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों में भाग लेने के लिए, उन्हें स्वतंत्रता के बाद भारत में पांच बार जेल भेजा गया था।
ज्योतिभाई ने राज्य-हिंसा और इसके हानिकारक विकास उपायों के खिलाफ लोकप्रिय संघर्षों और आंदोलनों में जीवन भर भागीदारी के रास्ते में कभी भी उम्र को आड़े नहीं आने दिया। सच्ची स्वतंत्रता, न्याय और सत्य की खोज में अटूट विश्वास के साथ, वह अपनी जीवन साथी मालिनी देसाई और बेटी स्वाति देसाई के साथ एक अनुकरणीय जीवन जी रहे हैं, जबकि मेधा पाटकर जैसी दृढ़ सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ एकजुटता से खड़े हैं। वह सूरत के आदिवासी गांव वेदछी से हमसे बातचीत करते हैं।
ए.के. शिबुराज: क्या आप हमें उस संदर्भ और परिस्थितियों का वर्णन कर सकते हैं जिसके कारण आपको स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना पड़ा?
ज्योतिभाई देसाई: मेरे पिता स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदार थे। उन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया और इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मैं तब छह साल का था। इसलिए मुझे किसी का सामना नहीं करना पड़ा।'
स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के दौरान विरोध। वास्तव में, मैंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी स्कूली शिक्षा छोड़ दी थी। उस समय, मैं बहुत उत्तेजित था और खतरनाक विचार रखता था। इसी अवधि के दौरान बॉम्बे प्रेसीडेंसी के तत्कालीन मुख्यमंत्री बी.जी. खेर ने मुझे गांवों में जाकर काम करने के लिए प्रेरित किया। इस तरह मैं वेदछी पहुंचा और असहयोग आंदोलन में सक्रिय हो गया। अन्यथा यह एक ऐसा रास्ता था जिसके साथ मैं कभी समझौता नहीं कर पाता। तब तक मेरा दृढ़ विश्वास था कि जिन्होंने गलतियाँ की हैं उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाद में तत्कालीन बॉम्बे मेयर युसुफअली मेहरअली की सिफारिश से मुझे कॉलेज में प्रवेश मिल गया। यह उनके हस्तक्षेप के कारण ही था कि मेरी राजनीतिक गतिविधियों के बावजूद मुझे प्रवेश से वंचित नहीं किया गया।
ए.के. शिबुराज: क्या आप कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने के तुरंत बाद वेदछी चले गए?
ज्योतिभाई देसाई: खार में गांधीजी के अनुयायियों के सौम्य अनुनय और सहयोग ने ग्रामीणों के बीच काम करने के मेरे निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समय मैंने गांधीवादी विचारों के बारे में पढ़ना शुरू ही किया था। शिक्षा के बारे में गांधीजी के दर्शन और ग्रामीणों के बीच उनके जीवन के तरीके को समझने में मुझे 2-3 साल लग गए। मैंने सौराष्ट्र क्षेत्र में आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में भाग लिया था। सेवक भोजराज द्वारा स्थापित बाल्कनजी बारी प्रशिक्षण संस्थान में मैंने शिक्षा के बारे में आगे सीखा। वेदच्छी पहुंचने के बाद, मैं बंबई से एक शहरवासी होने से पूरी तरह से बदल गया। नाना भाई और जुगतराम के कुशल मार्गदर्शन में शिविरों में प्राप्त प्रशिक्षण ने मुझे अच्छी स्थिति में पहुँचाया। तब तक जुगतराम, जो गांधी के भरोसेमंद शिष्य थे, ने 'स्वराज आश्रम' में नेतृत्व संभाल लिया था। वह गुजरात के दक्षिण में आदिवासी लोगों के निर्विवाद नेता भी थे।
ए.के. शिबुराज: आप एक निडर और साहसी व्यक्ति के रूप में बड़े हुए थे। गांधीजी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक दर्शन की ओर आपकी रुचि किस कारण से बढ़ी?
ज्योतिभाई देसाई: मैंने कभी किसी का आँख बंद करके अनुसरण नहीं किया। मैं किसी भी व्यक्ति को अंतिम शब्द मानने के लिए तैयार नहीं हूं- तब नहीं, अब नहीं। वेदच्छी पहुंचने पर मुझे बच्चों और छात्रों की जरूरतों से अवगत कराया गया। उन दिनों नानाभाई और जुगतराम शिक्षा में चरखे के महत्व के बारे में बात करते थे। हालाँकि यह कोई अंध विश्वास नहीं था। यदि चरखा कभी निरर्थक साबित हुआ तो वे उसे जलाने के लिए भी तैयार थे।
यह सच है कि गांधीजी का मुझ पर गहरा प्रभाव था। हालाँकि, मैं गांधीवादी शिक्षाविद् के रूप में नहीं जाना जाना चाहता। मैं आजादी से जीने की इच्छा रखता हूं। आज़ादी के बारे में सोचने और कार्य करने के लिए ही हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। स्वतंत्र विचार और कार्य में इस दृढ़ विश्वास के कारण मुझे कम से कम सात बार अपने कार्य संस्थान बदलने पड़े। मैं किसी भी कीमत पर सत्य और न्याय प्राप्त करना चाहता हूं।
गांधीजी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि शिक्षा का अर्थ अभ्यास के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान के माध्यम से एक मजबूत नैतिक स्थिति बनाना है। लेकिन आज, उथले सतही स्तर का ज्ञान प्राप्त करके, हम उपनिवेश होने से भी बदतर हो गए हैं।
ए.के. शिबुराज: आपका मानना है कि केवल शिक्षा के माध्यम से ही कोई राष्ट्र सच्ची स्वतंत्रता और स्वायत्तता प्राप्त कर सकता है। आज की शिक्षा प्रणाली, इसकी शिक्षाशास्त्र, इसकी सामग्री और उद्देश्यों के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
ज्योतिभाई देसाई: आज के शिक्षण संस्थान विनाशकारी हैं। बच्चों के लिए ज्ञान प्राप्त करने या स्वतंत्र रूप से सोचने की कोई गुंजाइश नहीं है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवा मस्तिष्क की जन्मजात प्रतिभाओं को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने का प्रयास करती है। माता-पिता को अपने बच्चों को ऐसे संस्थानों में भेजने से पहले दो बार सोचने की जरूरत है। मुख्यधारा की शिक्षा बच्चों के भीतर ज्ञान खोजने और प्राप्त करने के अंतर्निहित जुनून की परवाह किए बिना विकसित हो रही है। हमें एक राष्ट्रीय केंद्रीकृत शैक्षिक प्रणाली की नहीं, बल्कि विभिन्न स्वदेशी, सामुदायिक स्तर की शिक्षा प्रणालियों की आवश्यकता है, जो सत्य, न्याय और स्वतंत्रता के मूल में बनी हों।
एक बच्चे का पालन-पोषण अकेले माता-पिता द्वारा नहीं किया जा सकता। एक बच्चे के पालन-पोषण के लिए एक गाँव की आवश्यकता होती है। आज की शिक्षा प्रणाली बच्चों को असहाय और समर्थनहीन बनाती है। इससे बच्चे के भीतर यह बेहद गलत धारणा घर कर जाती है कि जीवन का मतलब नौकरी पाना और पैसा कमाना है। उसे पाना भी असंभव साबित हुआ है। आज की शिक्षा जिस दुनिया का वादा करती है वह मौजूद नहीं हो सकती। यही कारण है कि हार्दिक पटेल जैसे लोग बनते हैं।
ए.के. शिबूराज: आपने शिक्षण के सभी पुरातन और अप्रचलित तरीकों को त्यागकर छात्रों के बीच गुरु का पद ग्रहण किया। गांधी विद्यापीठ में छात्र यंत्रवत् रटकर नहीं सीख रहे थे। यह बाहरी वास्तविक दुनिया के संपर्क के माध्यम से है कि आपने छात्रों की चेतना के विकास के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार की है। मध्य प्रदेश में बुंदेल गुट के बीच अस्पृश्यता उन्मूलन के प्रयासों और पन्ना में लक्ष्मीपुर ओपन जेल के कैदियों के पुनर्वास के लिए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्रों के प्रयासों ने बहुत ध्यान आकर्षित किया था। मैंने पढ़ा है कि कैसे इन उदाहरणों को यूनिसेफ और ऑक्सफैम में प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में पढ़ाया जाता है। क्या आप हमें इसके बारे में और बता सकते हैं?
ज्योतिभाई देसाई: नवप्रवर्तन के ये प्रयास भारी बाधाओं और आलोचनाओं का सामना करते हुए किए गए। छात्रों की मुख्य चिंता परीक्षा और प्रमाणपत्रों को लेकर थी। हालाँकि जब इन चिंताओं को महत्व नहीं दिया गया तो वे पहले चिंतित थे, लेकिन लंबे समय में उन्होंने इससे होने वाले लाभों को पहचाना। सिकुड़ी हुई और कक्षाओं तथा पाठ्य पुस्तकों तक सीमित शैक्षिक व्यवस्था में, समाज से हमारे नाड़ी-संबंध कटते जा रहे हैं। जो छात्र भविष्य में इस राष्ट्र के राजनीतिक निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, उन्हें अपने चरित्र को ढालना चाहिए और अपने जीवन के आसपास के वास्तविक सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण के साथ सक्रिय जुड़ाव के साथ अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। छात्रों ने बांग्लादेशी शरणार्थी शिविरों में हैजा की रोकथाम के कार्यक्रमों में स्वेच्छा से भाग लिया। जयपुर बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए घर बनाना केवल एक दान नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक कार्य था। यहीं शिक्षा का असली लक्ष्य निहित है।
ए.के. शिबुराज: उस समय भी आलोचनाएँ थीं कि नई तालीम शैक्षिक दर्शन, जिसे गांधीजी ने प्रोत्साहित किया था, को उसके उचित सार में लागू नहीं किया गया था। कई उदाहरणों पर, उत्पादक कार्य अलग से सिखाया जा रहा था।
ज्योतिभाई देसाई: यह विभिन्न विषयों में ज्ञान प्राप्त करने वाले उद्यम के रूप में शिक्षा की संकीर्ण समझ का नकारात्मक परिणाम है। विषयों के कृत्रिम पृथक्करण के माध्यम से शिक्षण पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण है! यह निश्चित रूप से शिक्षा का लक्ष्य नहीं है।
जब मैंने अपने छात्रों को जामुन फल तोड़ने के लिए भेजा, तो वे वास्तव में विभिन्न चीजें सीख रहे थे। इस सीखने को भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान आदि जैसी श्रेणियों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अलग-अलग विषय क्षेत्रों में सीखने के इस विभाजन से कम से कम शिक्षा के शुरुआती चरणों में बचना होगा। अन्यथा यह ज्ञान प्राप्ति की व्यापकता में बाधा उत्पन्न करेगा। वास्तविक शिक्षा पाठ्यक्रम की दीवारों से परे है। गुजरात के कई स्कूलों में नई तालीम को गलत तरीके से लागू किया जा रहा है। यह केवल इसलिए है क्योंकि मुझे जुगतराम जैसे मजबूत नेताओं का समर्थन प्राप्त था कि मैं गांधी विद्यापीठ में नई तालीम को इसके वास्तविक मूल को दूर किए बिना लागू कर सका।
जुगतराम भाई एक अलग और असाधारण प्रजाति के नेताओं से थे। उन्होंने कभी भी गांधी सहित किसी का भी आंख मूंदकर अनुसरण नहीं किया। जब भी वह खुद को गलत पाते तो माफी मांगने और आवश्यक संशोधन करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे।
ए.के. शिबुराज: क्या उस समय के हमारे राजनेताओं और धार्मिक सुधारकों ने हमारी शिक्षा प्रणाली के निर्माण में औपनिवेशिक शक्तियों के प्रभावों को नजरअंदाज किया था?
ज्योतिभाई देसाई: भारत के इतिहास में, स्वेच्छा से शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी लेने वाले एकमात्र नेता बॉम्बे प्रेसीडेंसी के मुख्यमंत्री बी.जे. खेर थे। भारत की पहली केंद्रीय सरकार ने मौलाना आज़ाद को यह जिम्मेदारी केवल इसलिए सौंपी क्योंकि वे शिक्षा को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार के समय से ही हमारे देश में शिक्षा के महत्व को नजरअंदाज किया गया। हर कोई सत्ता में रुचि रखता था।
ए.के. शिबुराज: क्या यह उपेक्षा गांधीजी के जीवनकाल में भी थी?
ज्योतिभाई देसाई: लेकिन गांधीजी इस दावे से पूरी तरह असहमत थे। राजनीतिक सत्ता हासिल करने में रुचि रखने वाली कांग्रेस कार्य समिति ने भी गांधीजी की राय की उपेक्षा की। आजादी के तुरंत बाद कांग्रेस को भंग करने के सुझाव पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए स्वाभाविक रूप से राजनीतिक सत्ता का पीछा करने वालों ने उनकी शिक्षा नीतियों को कूड़ेदान में डालने के बारे में दोबारा नहीं सोचा। एक व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे दूसरे व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं है। मैं सत्ता के सभी कृत्यों के खिलाफ हूं। शिक्षा शासक वर्ग के हितों के अनुरूप भावी पीढ़ियों को विकृत करने का साधन नहीं होनी चाहिए।
ए.के. शिबुराज: 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में पूरे भारत में नई तालीम लागू करने का निर्णय लिया गया था। आज़ादी के बाद भारत में सत्ता में आई कांग्रेस सरकार इस फैसले को टालने में कैसे कामयाब रही?
ज्योतिभाई देसाई: हमें याद रखना चाहिए कि अधिकांश राजनेता चतुर और चालाक हैं। इसलिए, वे सावधानी से अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। उनकी अधिकांश नीतियाँ प्रतिगामी प्रकृति की थीं। खादी आयोग का गठन वर्ष 1950 में किया गया था। अनुदान प्राप्त करने के लिए आयोग की अनुमति आवश्यक थी। गांधीजी के मुद्रक स्वामी आनंद आश्चर्यचकित थे और उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया था कि दिल्ली में बैठा एक आयोग उनके घर के अंदर उत्पादित खादी को कैसे प्रमाणित कर सकता है। आपको अपने घर में काटी गई खादी के लिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता क्यों है? क्या आपको अपने घर में उत्पादित घी और दूध के लिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? हमें अच्छी गुणवत्ता वाली खादी की जरूरत है, न कि खादी बोर्ड से मिलने वाले वेतन और अन्य परिलब्धियों की। यह बात यूजीसी पर भी लागू होती है. मुझे कॉलेज चलाने के लिए यूजीसी द्वारा अनुमोदन और मान्यता की आवश्यकता क्यों है? जैसे खादी आयोग ने योजनाबद्ध तरीके से खादी को नष्ट कर दिया है, वैसे ही यूजीसी शिक्षा को नष्ट करने की राह पर है। आज़ाद भारत में ऐसी बहुत सी बेतुकी हरकतें हो रही हैं।
जो राज्य शिक्षा और छात्रों की जरूरतों के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ है, वह बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा है और कुछ लोगों को प्रमाणपत्र बांट रहा है। राज्य के दोषपूर्ण दृष्टिकोण के कारण नई तालीम नष्ट हो गई। सत्ता की अपनी अंधी चाहत में, हमारे राजनेता शिक्षा के मूल्य और लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव को समझने में विफल रहे हैं।
ए.के. शिबूराज: क्या आप यह सुझाव दे रहे हैं कि राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए?
ज्योतिभाई देसाई: शिक्षा को सरकार के दायरे से बाहर करना होगा। राज्य की भूमिका शिक्षा के लिए आवश्यक भौतिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने तक सीमित होनी चाहिए। छात्रों को क्या सीखना चाहिए या कैसे सीखना चाहिए, इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। परन्तु मेरा यह दृष्टिकोण कभी स्वीकार नहीं किया जायेगा और न ही लागू किया जायेगा। छात्रों और शिक्षकों की एक पीढ़ी जो राज्य के नियंत्रण से मुक्त हो सकती है, वही सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि शिक्षा को बहुराष्ट्रीय निगमों के हवाले कर दिया जाना चाहिए या इसे अंधाधुंध निजीकरण के लिए खुला रखा जाना चाहिए। अफसोस की बात है कि अभी यही हो रहा है। दरअसल, शिक्षा का अधिकार कानून की आड़ में शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है।
आज की शिक्षा नीतियां केवल पहले से मौजूद विषम संरचनाओं को मजबूत कर रही हैं जो कुछ अमीर लोगों के हाथों में सत्ता हासिल करते हुए कई छात्रों को हाशिए पर धकेल रही हैं। वहां नैतिकता या मूल्यों के लिए कोई जगह नहीं है। यह जीवन के लिए भी हानिकारक है! यह लोगों की भलाई को ख़तरे में डाल देगा। इस खतरनाक व्यवस्था के पीछे पूंजी ही एकमात्र प्रेरक शक्ति है। छात्र स्वतंत्र नहीं हैं; वे निर्विवाद और विनम्र होने के साँचे में ढले हुए हैं। अदृश्य जेलें उनका इंतजार कर रही हैं।
ए.के. शिबुराज: शिक्षा में निजी पूंजी के हस्तक्षेप से छात्रों को मिलने वाली भौतिक सुविधाओं में उल्लेखनीय अंतर आया है। आम धारणा यह है कि प्रौद्योगिकी ने शिक्षा के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन ला दिया है। शिक्षकों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर पुनर्विचार किया जा रहा है। आप इन परिवर्तनों को कैसे समझते हैं?
ज्योतिभाई देसाई: इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन में सकारात्मक अभिव्यक्तियाँ लायी हैं। हालाँकि, इसकी शक्तियों पर आँख मूँदकर विश्वास करना बेहद खतरनाक साबित होगा। तकनीकी प्रतिभा का दावा करने वाले अधिकांश उपाय वास्तव में हमारे जीवन की गति को तेज करके और हमें एक-दूसरे के साथ अधिक प्रतिस्पर्धी बनाकर मुनाफा बढ़ाने के शॉर्टकट हैं। यह मानना गलत और खतरनाक है कि तकनीकी प्रगति ही हमारी सभी सामाजिक समस्याओं का समाधान होगी। ऐसी स्थितियों में जो हमारी नैतिक चेतना के आधार पर निर्णय लेने की मांग करती हैं, तकनीक बेकार होगी। मुझे नहीं लगता कि प्रौद्योगिकी न्याय और समानता का मार्ग प्रशस्त करेगी। नैतिक दिशा-निर्देश से रहित लक्ष्यहीन जीवन अंततः विनाश की ओर ले जाएगा। यह हमारी जीवन-शक्ति का विनाश है! तकनीकी उन्नति के नाम पर शिक्षण संस्थानों में अपनाए गए कुछ उपाय पूरी तरह से फर्जी हैं!
ए.के. शिबूराज: शिक्षा में आपका हस्तक्षेप ऐसे समय में हुआ जब भारत में जाति व्यवस्था बेहद मजबूत थी, जाति-आधारित हिंसा के निरंतर कृत्यों के माध्यम से हमारे समाज के एक वर्ग को हाशिए पर रखा गया था और गंभीर घाव दिए गए थे। इस काल में प्रचलित सवर्ण वर्चस्व से आपने कैसे निपटा?
ज्योतिभाई देसाई: भारतीय ब्राह्मण भारत के संदर्भ में अस्पृश्यता और पूर्वाग्रही पक्षपात की प्रथा के माध्यम से दासता के पश्चिमी तरीकों का उपयोग कर रहे थे। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत दास प्रथा को संस्थागत बना दिया गया है। गांधीजी आश्रम के भीतर इस प्रणाली के चलन के सख्त खिलाफ थे। आश्रम के प्रबंधक मगनलाल, जिन्होंने आश्रम में शामिल होने आए हरिजन परिवार के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया था, को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालाँकि, वह छह महीने बाद एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में वापस लौटे। गांधीजी का स्पष्ट दृष्टिकोण था कि जाति व्यवस्था के खतरे से कैसे निपटा जाए।
मैं एक और उदाहरण बताता हूँ। मेरे स्कूल में ग्राम प्रधान के बेटे ने घोषणा की कि मेरी कक्षा का हरिजन छात्र भरे हुए बर्तनों से पानी नहीं पी सकता। उसने यह भी घोषणा की कि उसके अलावा कोई भी इसे नहीं पी सकता। मैंने उससे कहा कि उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। आख़िर निराश होकर वह बर्तन तोड़ने लगा। उसने करीब सात मटके तोड़े। अंततः उसने यह पूर्वाग्रह बंद कर दिया। कक्षा भ्रमण के दौरान, उसने हममें से बाकी लोगों के साथ भी भोजन साझा किया।
मैंने कभी भी जाति व्यवस्था के ख़िलाफ़ अभियान का नेतृत्व नहीं किया। मेरी जीवनशैली, मेरे विश्वास और व्यवहार ही मेरे शस्त्रागार थे। जिन लोगों ने गलत किया है उनके लिए हमेशा धार्मिकता की ओर वापस जाने का रास्ता खोजने की जगह होती है। अन्यायी हमेशा खुद को सुधार सकता है और न्याय के रास्ते पर लौट सकता है।
ए.के. शिबूराज: अम्बेडकर ने गाँवों को अज्ञानता का अड्डा और जातिगत उत्पीड़न के सबसे क्रूर रूपों से घिरा हुआ पाया था। दलितों का शहरों की ओर पलायन वास्तव में उनके मुक्ति आंदोलन का एक हिस्सा था। आज भी, शहर सुरक्षित स्थान हैं जहां निचली जाति के लोग 'इंसान' के रूप में रह सकते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
ज्योतिभाई देसाई: सबसे पहले, शहरों में जाति से रहित कोई नई मूल्य प्रणाली नहीं है। हाँ, गाँवों में पाई जाने वाली जातिगत प्रथाओं का शहरों में पालन करना व्यावहारिक रूप से कठिन है। इसलिए, शहरों में जाति-व्यवस्था अपेक्षाकृत कमज़ोर है। हालाँकि, शहरों में भी जाति के आधार पर निवास और भोजन देने या उपलब्ध कराने से इनकार करने के उदाहरण अभी भी मौजूद हैं।
अंबेडकर की बात करें तो वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें जाति के कारण जीवन में बहुत सारे नकारात्मक अनुभवों से गुजरना पड़ा। इसने उनके जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे व्यक्तिगत उथल-पुथल मच गई। उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएँ उन्हें लगातार हो रही चोट का परिणाम हैं। यह उनके दार्शनिक और बौद्धिक विचारों में परिलक्षित होता है।
ए.के. शिबूराज: जाति-व्यवस्था पर गांधी और अंबेडकर के विचार अलग-अलग थे। क्या हम कह सकते हैं कि गांधी अम्बेडकर को समझने में असफल रहे?
ज्योतिभाई देसाई: गांधीजी ने कभी भी जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। गांधीजी की चिंताओं का केंद्र मनुष्य था। उनका उद्देश्य हमारे बीच मौजूद विभिन्न भेदभावों के बावजूद मानवता को एक साथ लाना था। गांधीजी ने अम्बेडकर की उपेक्षा या अवहेलना नहीं की। हालाँकि अम्बेडकर कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, फिर भी गांधीजी ने मंत्री पद के लिए उनके नाम की सिफारिश की। गांधीजी ने संविधान निर्माण प्रक्रिया में अंबेडकर की भागीदारी और योगदान भी सुनिश्चित किया।
ए.के. शिबूराज: क्या आपको लगता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान और इसके द्वारा प्रस्तुत लोकतांत्रिक आदर्शों को गंभीर खतरा है? क्या हम अधिनायकवाद के चरणों में विविधता और धर्मनिरपेक्षता के अपने मूल्यों को त्याग रहे हैं? खुली बहस और बातचीत का अभाव परेशान करने वाला है, है ना?
ज्योतिभाई देसाई: स्वतंत्रता के बाद भारत में विभिन्न ऐतिहासिक मोड़ों पर लोकतंत्र को कई हमलों का सामना करना पड़ा। एक राष्ट्र और उसके लोग जिन्होंने आज़ादी में आज़ादी का सपना देखा था, उन्हें इसके पीछे विनाश और ध्रुवीकरण और विभाजन मिला। लोग यह देखकर हैरान रह गए कि जिन नेताओं को उन्होंने देश का नेतृत्व करने के लिए चुना था, वे बेशर्मी से सत्ता और धन के पीछे भाग रहे थे। मुझे डर है कि आज हमारे देश पर अधिनायकवाद अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। यह निर्णय लिया जा रहा है कि केवल एक ऊंची आवाज सुनी जाएगी, जिससे हमारे बाकी विरोधात्मक विलाप को शांत कर दिया जाएगा। जो राष्ट्र असहाय है और सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करने से डरता है, वह अंधकार के युग में प्रवेश का प्रतीक है। मैं फिर से दोहराता हूं कि हम एक ऐसी पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं जो कभी भी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करेगी।
केंद्र सरकार के अधीन युवाओं के कौशल विकास की योजना क्यों है? यह हमारे युवाओं को भविष्य में किसकी सेवा में काम करना है, इसके बारे में क्या संदेश देता है? स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए जगह कहां है? अंतिम उद्देश्य व्यक्तियों को विभिन्न उद्योगों में काम करने वाली बिना सोचे-समझे मशीनों में बदलना है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे देश में विविध कार्य कौशल का समृद्ध संसाधन मौजूद है। हमारे पास बीजों के संरक्षण, मृदा संरक्षण, नवाचार और शिल्प के संबंध में ज्ञान का मूल्यवान भंडार है। ये कौशल कोई ऐसी चीज़ नहीं हैं जो हमने राज्य एजेंसियों के किसी संस्थान में दाखिला लेकर सीखी है। हमारे देश में कौशल की कभी कमी नहीं रही। बेरोजगारी का कारण निश्चय ही यह नहीं है।
ए.के. शिबुराज: आपने लगातार शक्तिशाली लोगों के निरंकुश व्यवहार का विरोध किया है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को चुप कराने के किसी भी प्रयास के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। क्या आपके इस स्पष्टवादी व्यवहार के कारण अन्य व्यक्तियों के साथ मनमुटाव हुआ है? मैंने सुना है कि आप आचार्य विनोबा भावे से खुले तौर पर असहमत थे।
ज्योतिभाई देसाई: महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन किसके लिए लड़ रहा है? आप किसके हक के लिए आवाज उठा रहे हैं? जब हमारी प्रतिक्रियाएँ हमारे अहंकार को प्रतिबिंबित करती हैं तो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। विनोबा भावे ने एक बार मुझसे उड़ीसा में सर्वोदय संस्थान की शैक्षिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए कहा। उन्होंने उड़ीसा के सीएम के अनुरोध के आधार पर यह निर्देश दिया था। विनोबा इंदिरा की शक्ति के वायरस से प्रभावित थे और भूल गए थे कि वे उसी शक्ति के साथ मिलीभगत कर रहे हैं जिसके खिलाफ उन्होंने अब तक विरोध किया था। मैंने उन्हें याद दिलाया कि सर्वोदय का मिशन और सत्ता की जिन संरचनाओं के साथ वह मुझसे काम करने के लिए कह रहे थे, वे कभी एक साथ नहीं चल सकते। जब उन्होंने मुझे और समझाया तो मैंने उनसे कहा कि वह पागलपन की बात कर रहे हैं। वह लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे जयप्रकाश नारायण से दूरी बनाते हुए इंदिरा के करीब बढ़ रहे थे। हवाई अड्डे पर इंदिरा से मिलने गए विनोबा ने बार-बार आग्रह करने के बाद भी जेपी की मृत्यु शय्या पर उनसे मिलने से इनकार कर दिया।
सत्ता लोगों को भ्रष्ट करती है। गांधी जो यह जानते थे वे दिल्ली नहीं बल्कि नोआखाली गए। दिल्ली में जो लोग सत्ता में हैं, उन्हें ही लोगों के पास आना चाहिए। मैं यह बात मेधा को हर समय बताता हूं कि दिल्ली में सत्ता में बैठे लोगों को यहां के हालात समझने के लिए नर्मदा आना चाहिए। अन्यथा राज्य की निरंकुश शक्ति अंततः लोगों की स्वतंत्रता के अधिकार को छीन लेगी।
ए.के. शिबुराज: नर्मदा में आपके हस्तक्षेप और सक्रियता के पीछे क्या परिस्थिति थी? क्या आपको यह देखकर निराशा हुई है कि अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलकर विरोध करने वाले लोग अपने उद्देश्यों तक पहुँचने में असफल हो जाते हैं?
ज्योतिभाई देसाई: जब लोग राज्य मशीनरी के अधिकार और अहंकार से उत्पीड़न से लड़ रहे थे तो मैं कैसे खड़ा होकर देख सकता हूँ? लोकप्रिय विरोध आंदोलनों में जीत और हार का आकलन करना आसान नहीं है। नर्मदा विरोध प्रदर्शन के कारण विकास संबंधी वादों के खोखलेपन और असहाय पीड़ितों और आम आदमी पर होने वाले अन्याय पर राष्ट्रीय स्तर पर जोरदार चर्चा हुई। यह विरोध बड़ी विकास परियोजनाओं के परिणामस्वरूप पर्यावरणीय विविधता और आम लोगों के जीवन के बड़े पैमाने पर विनाश के बारे में लोकप्रिय चेतना को समझाने में सहायक था। मुझे लगता है कि यह विरोध यह दिखाने में सफल रहा कि सरकार वास्तव में कैसे चंद शक्तिशाली समूहों के हितों का समर्थन कर रही थी और देश के संसाधनों के विनाश का मार्ग प्रशस्त कर रही थी।
ए.के. शिबुराज: 21वीं सदी पर्यावरणीय स्थिरता की चिंताओं और विभिन्न तात्कालिक चुनौतियों से घिरी हुई है जो मानवता के अस्तित्व पर हमला करती हैं। चूंकि ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण विनाश से संपूर्ण जीवन प्रणालियों के अस्तित्व को खतरा है, आम आदमी अभी भी जीवित रहने की बुनियादी जरूरतों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है। बाहर निकलने का रास्ता क्या है?
ज्योतिभाई देसाई: मानवता भयानक संकट के कगार पर है। लेकिन इस समस्या का समाधान कोई एक देश नहीं ढूंढ सकता। आगे का रास्ता खोजने के लिए पूरे विश्व समुदाय को एक साथ आना होगा, एकजुट होना होगा। यह कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हम निष्क्रिय बने रहें।
गांधी की प्रासंगिकता इस संदर्भ में बढ़ती जा रही है, जहां मानव समुदाय गंभीर पर्यावरणीय संकटों का सामना कर रहे हैं। उनकी दूरदर्शी दृष्टि को हिंद स्वराज में दर्शाया गया है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, सत्ता की दौड़ में गांधी की उपेक्षा की गई। गांधीजी ने हमें पहले ही आगाह कर दिया था कि औद्योगिक क्रांति की अस्थायी प्रगति पर आधारित उपभोक्तावादी लालच हमारे भविष्य के लिए बहुत महंगी साबित होगी। क्या हम अब भी ग्राम स्वराज के महत्व को नजरअंदाज कर सकते हैं? अमेरिका और यूरोप की संस्कृतियों की बिना सोचे-समझे नकल करना बेहद बेवकूफी है, सत्ता में बैठे लोगों के खाली खोखले वादों से एक पूरी पीढ़ी को मूर्ख बनाया जा रहा है। हम अब अमेरिकी मॉडल का अनुसरण करने की स्थिति में नहीं हैं।'
ए.के. शिबूराज: आपके पास स्वतंत्रता संग्राम की अवधि, गांधीजी के साथ आपके संबंध, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान, न्याय और लोकतंत्र की खोज में आपके द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों और आंदोलनों से संबंधित अनुभवों का खजाना है। इतने सारे विविध अनुभव, दृष्टिकोण, विचार... फिर भी आपने एक संस्मरण लिखकर इसे लिखने के बारे में क्यों नहीं सोचा?
ज्योतिभाई देसाई: देखिए, भारतीय संस्कृति किसी व्यक्ति के योगदान पर गर्व नहीं करती है। यह बहुत से लोगों के साझा और संयुक्त प्रयासों का नतीजा है और इसमें बहुत सारा आपसी लेन-देन शामिल है। मैं जो व्यक्ति हूं, उसमें 'मैं' का ज्यादा महत्व नहीं है। यहां तक कि कृष्ण और राम को भी अन्य कारणों की पूर्ति के लिए यहां बुलाया गया था।
मेरा जीवन और मेरा कार्य मेरे अंदर मौजूद किसी विशेष गुण का परिणाम नहीं है। इसके बजाय यह सब प्रयासों के संगम और कई व्यक्तियों के विभिन्न पहलुओं के पूर्ण समर्थन के कारण संभव हुआ, जो एक बड़े उद्देश्य के लिए मजबूती से एक साथ खड़े थे। मैं पूरी आजादी से रहना चाहता हूं। मैं गांधीवादी या शिक्षाशास्त्री नहीं हूं। मुझे ढाँचों में बंधनों में नहीं बंधना है। मैं उस आज़ादी का आनंद लेता हूँ जो सत्ता की भ्रष्ट इच्छा और प्रभाव से अलग खड़े होने से मिलती है। मैं स्वतंत्र नागरिकों वाले एक स्वतंत्र राष्ट्र का सपना देखता हूं।
ए.के. शिबूराज एक स्वतंत्र पत्रकार हैं
(अपर्णा ईश्वरन द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित, सबरंग टीम द्वारा हिंदी में अनुवादित)
सौजन्य: काउंटरकरंट



