कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि कोई असंबंधित तीसरा पक्ष शिकायत दर्ज नहीं कर सकता, राज्य के कानून की धारा 4 की व्याख्या को सीमित कर दिया है।
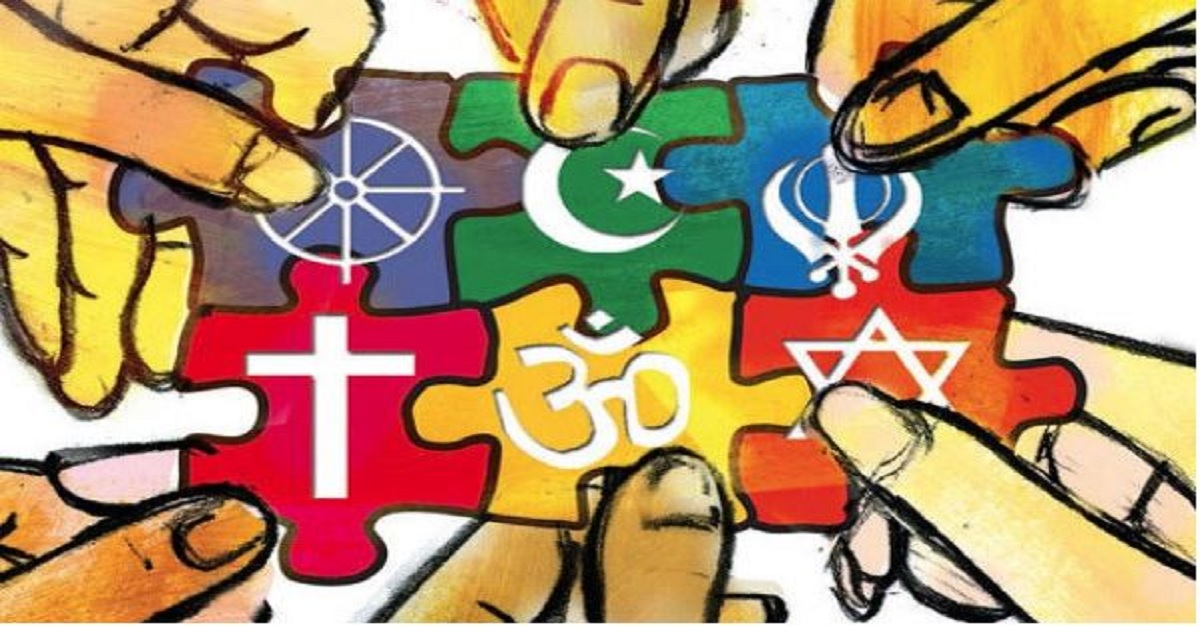
धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य शक्ति के इस्तेमाल पर सीधा प्रभाव डालने वाले एक फैसले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य के विवादास्पद धर्मांतरण-विरोधी कानून पर एक प्रारंभिक और महत्वपूर्ण न्यायिक अंकुश लगाया है। यह फैसला 17 जुलाई 2025 को मुस्तफा एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य मामले में सुनाया गया, जिसमें तीन मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया था। उन पर हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश का आरोप लगाया गया था। 2022 में पारित कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार संरक्षण अधिनियम (KPRFR अधिनियम) के तहत यह न्यायिक व्याख्या अभी प्रारंभिक अवस्था में है। यह निर्णय भले ही अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर नहीं गया, लेकिन इसने कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय स्थापित किए हैं, जो इस कानून की प्रारंभिक व्याख्या की दिशा तय करेंगे। गौरतलब है कि जब यह कानून पारित किया गया था, तब राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता में थी। मई 2023 में भारी बहुमत से सत्ता में आई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) ने इस कानून को निरस्त करने का वादा किया था, लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बावजूद यह कानून आज भी विधि पुस्तिकाओं में बरकरार है।
यह निर्णय एक महत्वपूर्ण न्यायिक फैसला है। इसकी विशेषता इस बात में नहीं है कि इसने किसी कानून को रद्द किया - क्योंकि यह अधिनियम अब भी विधि पुस्तिकाओं (statute books) में बरकरार है- बल्कि इसमें दी गई राहत के विशिष्ट कानूनी आधारों में निहित है। उच्च न्यायालय ने लोकस स्टैंडी (यानी शिकायत दर्ज कराने का अधिकार) और प्रथम दृष्टया आपराधिक मामला स्थापित करने में हुई विफलता पर जोर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि तीसरे पक्ष के स्वयंभू निगरानीकर्ताओं द्वारा इस कानून के संभावित दुरुपयोग के खिलाफ एक मिसाल स्थापित हुई। धर्मांतरण विरोधी इस अधिनियम की प्रारंभिक व्याख्या के रूप में, मुस्तफा मामले का निर्णय एक स्पष्ट मिसाल पेश करता है, जिसके आधार पर इस प्रकार की अभियोजन कार्रवाइयों को चुनौती दी जा सकती है भले ही सरकार ने कर्नाटक में इस कानून को निरस्त करने की योजना बना रखी हो।
मामले के तथ्य
मुस्तफा मामले में प्रस्तुत तथ्य ठीक उसी प्रकार की स्थिति दर्शाते हैं, जिसके लिए कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार संरक्षण अधिनियम (KPRFR Act) को कथित रूप से बनाया गया था। 4 मई 2025 को रामतीर्थ मंदिर, जमखंडी के एक भक्त रमेश मल्लप्पा नावि ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता इस्लामिक पुस्तिकाएं बांट रहे थे और जब उन्हें रोका गया, तो उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। साथ ही उन्होंने कथित रूप से यह भी कहा कि उनका उद्देश्य “पूरी दुनिया को इस्लाम की ओर मोड़ना” है और जो रास्ते में आएगा उसे देख लेंगे। आज के भारत में, यह जानकारी शायद किसी गुस्से भरे व्हाट्सऐप फॉरवर्ड की विषयवस्तु बन सकती है, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत - सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य जैसी सीमाओं के अधीन- प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का समान अधिकार प्राप्त है।
इस मामले में दर्ज एफआईआर में KPRFR अधिनियम की विशिष्ट भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ताओं ने धर्मांतरण के लिए लोगों को “लुभावने प्रलोभन” -जैसे वाहन और दुबई में नौकरी के मौके-दिए। इस तरह का “लालच” इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित अपराध का एक केंद्रीय आधार है। चूंकि प्रस्तुत तथ्य लगभग उसी प्रकार के थे जिन्हें यह कानून लक्षित करता है, इसलिए यह मामला कानून के इस्तेमाल की सीधी न्यायिक परीक्षा के लिए उपयुक्त प्रतीत हो रहा था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस पर फैसला देते समय संविधानिक वैधता की व्यापक पड़ताल में जाए बिना ही अभियोजन पक्ष के मामले में मौलिक प्रक्रियात्मक और तथ्यात्मक त्रुटियों को आधार बनाया।
पहला आधार: शिकायत दर्ज करने का अधिकार किसे है?
अदालत द्वारा एफआईआर रद्द करने का प्रमुख कारण यह था कि शिकायतकर्ता के पास कानूनी हैसियत (legal standing) नहीं थी। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि यह शिकायत एक "तृतीय पक्ष" द्वारा दर्ज की गई थी जो अधिनियम की धारा 4 में निर्दिष्ट व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं आता।
इसी आधार पर एफआईआर का पंजीकरण “कानूनी रूप से अमान्य” करार दिया गया।
KPRFR अधिनियम की धारा 4 यह स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि शिकायत केवल वही व्यक्ति दर्ज कर सकता है जिसका कथित रूप से धर्मांतरण किया गया हो या फिर उसके माता-पिता, भाई-बहन, या बेहद करीबी रिश्तेदार, विवाह या गोद लेने के संबंध से जुड़े कोई अन्य रिश्तेदार। इस मामले में शिकायतकर्ता मंदिर में मौजूद एक दर्शक (bystander) था, जो इन मानकों में से किसी में भी फिट नहीं बैठता।
इस प्रावधान का सख़्ती से पालन एक स्पष्ट संदेश देता है कि: इस आपराधिक कानून की प्रक्रिया किसी भी सामान्य नागरिक या वैचारिक रूप से प्रेरित कार्यकर्ता द्वारा शुरू नहीं की जा सकती। इस व्याख्या के जरिए न्यायपालिका ने इस अधिनियम और अन्य राज्यों में इसके समकक्ष कानूनों में प्रयुक्त व्यापक और अस्पष्ट भाषा के खिलाफ एक महत्वपूर्ण न्यायिक संतुलन स्थापित किया है। उदाहरण के लिए, कर्नाटक अधिनियम में शिकायत की अनुमति “किसी भी रूप में जुड़े व्यक्ति या सहकर्मी” को दी गई है -जो बेहद अस्पष्ट है। वहीं उत्तर प्रदेश कानून में हालिया संशोधन के तहत “कोई भी व्यक्ति” एफआईआर दर्ज करा सकता है। इस तरह के नियम जनता को न्यायिक प्रक्रिया में तृतीय पक्ष के रूप में शामिल कर देते हैं, जो स्वयंभू निगरानी समूहों (vigilante groups) के कारण पैदा होने वाले झूठे और परेशान करने वाले मुकदमों के लिए रास्ता खोलते हैं।
मुस्तफा मामला में फैसले की तर्कसंगत व्याख्या कानूनी प्रक्रिया को उस व्यक्ति पर केंद्रित करती है, जिसके अधिकार वास्तव में खतरे में हैं, यानी कथित अवैध धर्मांतरण का शिकार।यह ध्यान किसी बाहरी व्यक्ति की चोटिल भावनाओं से हटाकर उस व्यक्ति पर ले जाता है, जिसे अपनी मान्यता और विश्वास की आज़ादी का असली नुकसान हुआ हो। यह एक प्रकार की “प्रक्रियात्मक सुरक्षा” (procedural firewall) बनाता है, जो एक प्रारंभिक कानूनी तर्क के रूप में काम करता है। अब वकील इस तर्क का इस्तेमाल उन मामलों को चुनौती देने के लिए कर सकते हैं जो सामान्य आरोपों या सांप्रदायिक नफरत से प्रेरित होते हैं।
दूसरा आधार: क्या कोई “धर्मांतरण का प्रयास” हुआ?
प्रक्रियात्मक खामी के अलावा उच्च न्यायालय ने शिकायत की सामग्री में एक बड़ा दोष पाया। एफआईआर में दर्ज सभी आरोपों को सच मानते हुए भी, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वे “अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध के आवश्यक तत्वों को पूरा करने में असफल हैं।”
न्यायालय की बात बिल्कुल स्पष्ट थी: “यह कहीं भी आरोप नहीं लगाया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने किसी व्यक्ति का धर्मांतरण किया या करने की कोशिश की।” यह निष्कर्ष अभियोजन के लिए एक बड़ी कसौटी तय करता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल सामान्य स्तर पर किए गए धर्म प्रचार के कार्य-जैसे साहित्य बांटना, धार्मिक बहस करना आदि-अपने आप में इस अधिनियम के तहत अपराध नहीं माने जा सकते। इस कानून को लागू करने के लिए राज्य को यह साबित करना होगा कि कोई विशेष, लक्षित कार्य किसी पहचाने जा सकने वाले व्यक्ति को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से किया गया था।
यह भेद स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 25 के तहत धर्म “प्रचार” करने के संवैधानिक अधिकार और KPRFR अधिनियम के तहत “धर्मांतरण का प्रयास” जैसी दंडनीय कार्रवाई के बीच एक महत्वपूर्ण रेखा खींचता है। न्यायालय का संकेत है कि किसी धार्मिक अभिव्यक्ति को जब तक वह किसी विशेष व्यक्ति के प्रति लक्षित ठोस धर्मांतरण प्रयास में न बदले, तब तक उसे संविधानिक संरक्षण प्राप्त रहेगा और वह आपराधिक कृत्य नहीं मानी जाएगी। मुस्तफा एफआईआर में याचिकाकर्ताओं की गतिविधियों का विस्तृत विवरण होने के बावजूद, ऐसा कोई आरोप नहीं था कि उन्होंने किसी व्यक्ति को धर्मांतरण के लिए निशाना बनाया। इसी कारण शिकायत कानूनी रूप से उपयुक्त नहीं मानी गई। यह निर्णय एक और महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है जिससे बचाव पक्ष (defence counsel) के पास यह ठोस दलील उपलब्ध हो जाती है कि इस अधिनियम का इस्तेमाल केवल धर्म प्रचार या संवाद जैसी गतिविधियों को अपराध ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता।
राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य: कानून को लगातार कठोर बनाते जाने की प्रवृत्ति
कर्नाटक का यह अधिनियम कोई अलग-थलग कानून नहीं है, बल्कि एक समन्वित राष्ट्रीय प्रवृत्ति का हिस्सा है। 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों ने या तो नए धर्मांतरण-रोधी कानून बनाए हैं या मौजूदा कानूनों में संशोधन किए हैं और हर नया कानून अपने पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक कठोर साबित हुआ है। इन नए कानूनों की बनावट और वैचारिक आधार लगभग एक जैसे हैं और अक्सर इन्हें तथाकथित “लव जिहाद” के निराधार नैरेटिव और जनसंख्या संतुलन को लेकर फैलाई जा रही आशंकाओं के तर्क पर न्यायोचित ठहराया जाता है।
इन कानूनों की विशेषताएं इस प्रकार हैं:
● अत्यधिक व्यापक परिभाषाएं: “प्रलोभन” जैसे शब्दों को इतनी व्यापकता से परिभाषित किया गया है कि यदि कोई धार्मिक संस्था नि:शुल्क शिक्षा या रोजगार का अवसर देती है, तो उसे भी अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है। इससे वैध और परोपकारी कार्यों के आपराधिक दायरे में आने का खतरा बनता है।
● अंतरधार्मिक विवाह को निशाना बनाना: “शादी का वादा” धर्मांतरण के लिए प्रतिबंधित माध्यमों में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है, जो वयस्कों को अपने जीवनसाथी चुनने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सीधा दखल देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा माना है।
●पक्षपातपूर्ण अपवाद: इन कानूनों में से कुछ “पूर्व धर्म में पुनः धर्मांतरण” (reconversion) को विशेष छूट देते हैं, यानी व्यक्ति के “तत्काल पूर्व धर्म” में वापसी को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है। यह प्रावधान व्यापक रूप से एक एकतरफा रास्ते के रूप में देखा जा रहा है, जो हिंदू धर्म में वापसी को वैध मानते हुए, अन्य धर्मों में धर्मांतरण को दंडनीय बनाता है।
● दखल देने वाली प्रक्रियाएं: ये कानून धर्मांतरण से पहले और बाद में ज़िलाधिकारी के समक्ष विस्तृत घोषणा प्रक्रिया को अनिवार्य बनाते हैं जिसमें सार्वजनिक सूचना जारी करना और पुलिस जांच तक शामिल है। इस प्रक्रिया के चलते, व्यक्तिगत आस्था का विषय एक लोक परीक्षण और नौकरशाही मंज़ूरी के दायरे में आ जाता है।
● कठोर दंड: उदाहरण के लिए राजस्थान के धर्मांतरण विरोधी कानून में अपराध गंभीर (cognizable) और गैर जमानती (non-bailable) घोषित किए गए हैं। इतना ही नहीं, सबूत का भार (burden of proof) भी उलट दिया गया है यानी आरोपी को यह साबित करना होगा कि धर्मांतरण वैध था। यह न्याय के उस मूल सिद्धांत के विपरीत है, जिसमें माना जाता है कि "जब तक दोष सिद्ध न हो, व्यक्ति निर्दोष है।"
यह बेहद दखल देने वाली और मौलिक अधिकारों की खुली अवहेलना पूरे देश में कानूनी चुनौती का विषय बन चुकी है। देश भर की विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में इन कानूनों के खिलाफ कई याचिकाएं लंबित हैं।
इन कानूनों को दी जा रही कानूनी चुनौती सुप्रीम कोर्ट की दो परस्पर-विरोधी व्याख्याओं के बीच संभावित टकराव की जमीन तैयार कर रही है। एक ओर है साल 1977 का फैसला रेव. स्टेनिसलौस बनाम मध्य प्रदेश राज्य (Rev. Stainislaus v. State of Madhya Pradesh) जिसमें संविधान पीठ (Constitution Bench) ने शुरुआती धर्मांतरण विरोधी कानूनों को वैध ठहराया था। इस निर्णय में अनुच्छेद 25 के तहत धर्म “प्रचार” करने के अधिकार की व्याख्या सीमित रूप में की गई, यह कहते हुए कि इसमें किसी दूसरे व्यक्ति को धर्मांतरित करने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। इस फैसले ने इन कानूनों को वैध ठहराने के लिए राज्य को “लोक व्यवस्था बनाए रखने” की शक्ति का आधार माना था।
दूसरी ओर है आधुनिक और व्यापक व्याख्या, जो व्यक्तिगत स्वायत्तता (individual autonomy) को केंद्र में रखती है जिसे साल 2017 के ऐतिहासिक निर्णय जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (Right to Privacy) में जिक्र किया गया था। इस मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने यह घोषणा की कि गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है जो व्यक्ति की गरिमा, निजी स्वायत्तता, और जीवन से जुड़े बुनियादी निर्णयों जैसे परिवार, विवाह और आस्था को स्वतंत्र रूप से लेने की स्वतंत्रता को शामिल करता है।
नए धर्मांतरण विरोधी कानून जो व्यक्तिगत धार्मिक आस्थाओं पर राज्य की दखलअंदाजी और निगरानी को बढ़ावा देते हैं, इस न्यायिक मतभेद के बिल्कुल बीचों-बीच स्थित हैं। जहां स्टैनिसलौस (Stainislaus) फैसले ने जबरदस्ती या धोखे जैसे अवैध तरीकों से धर्मांतरण रोकने पर ध्यान केंद्रित किया था, वहीं ये नए कानून स्वेच्छा से धर्म बदलने के काम को ही नियंत्रित करते हैं। राज्य को अपनी धर्मांतरण की मंशा बताने और इसके लिए सार्वजनिक जांच का सामना करने की आवश्यकता, सीधे तौर पर उस “चयन और आत्म-निर्धारण के क्षेत्र” (zone of choice and self-determination) को चुनौती देती है, जिसकी रक्षा पुट्टास्वामी फैसले ने की थी।
मूलभूत संवैधानिक प्रश्न अब केवल धर्म प्रचार के अधिकार (स्टैनिसलौस वाला मुद्दा) तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह है कि क्या राज्य इतनी बोझिल और हस्तक्षेपकारी प्रक्रिया को एक बेहद व्यक्तिगत निर्णय पर थोप सकता है, बिना व्यक्ति के निजता और स्वतंत्रता के अधिकार (पुट्टास्वामी वाला मुद्दा) का उल्लंघन किए।
आगे का रास्ता
मुस्तफा मामले का निर्णय न्यायपालिका की एक सतर्क और सीमित दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण परिणाम है, जो केवल कानून की भाषा पर आधारित रहा। यह फैसला तत्काल और ठोस राहत प्रदान करता है, साथ ही बिना किसी सीधे संवैधानिक टकराव को जन्म दिए कुछ अहम प्रक्रियात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस निर्णय की विरासत यह होगी कि यह अभियुक्तों और उनके वकीलों को ऐसे सटीक और प्रभावी कानूनी तर्क देता है, जिनके जरिए वे मुकदमे की शुरुआत में ही अभियोजन को चुनौती दे सकें और इस तरह कानून के दुरुपयोग की संभावनाओं पर समय रहते रोक लगाई जा सके।
हालांकि असली लड़ा अभी बाकी है। KPRFR अधिनियम और उसके जैसे अन्य धर्मांतरण विरोधी कानूनों की मूल धाराओं - जैसे उनकी विस्तृत परिभाषाएं, पक्षपातपूर्ण प्रावधान और हस्तक्षेपकारी प्रक्रियाएं — को अब भी संविधान की कसौटी पर पूरी तरह परखा जाना बाकी है। आखिरकार, सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना होगा कि जबरन धर्मांतरण रोकने में राज्य का हित कहां तक जायज है -और वह कहां पर व्यक्ति की निजता, स्वतंत्रता, समानता और अंतरात्मा की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों से टकराता है। मुस्तफा मामले में फैसला इस व्यापक संवैधानिक बहस का पहला महत्वपूर्ण अध्याय है- एक स्थिर और विवेकपूर्ण निर्णय, जिसने प्रक्रिया संबंधी जरूरी स्पष्टता प्रदान की है, जबकि अहम संवैधानिक पड़ताल अब भी बाकी है।
(लेखक इस संगठन की कानूनी शोध टीम का हिस्सा हैं।)
Related
विरोध में इस्तीफा: मध्य प्रदेश की महिला न्यायाधीश ने भेदभाव और उत्पीड़न के आरोपी वरिष्ठ की पदोन्नति पर दिया इस्तीफा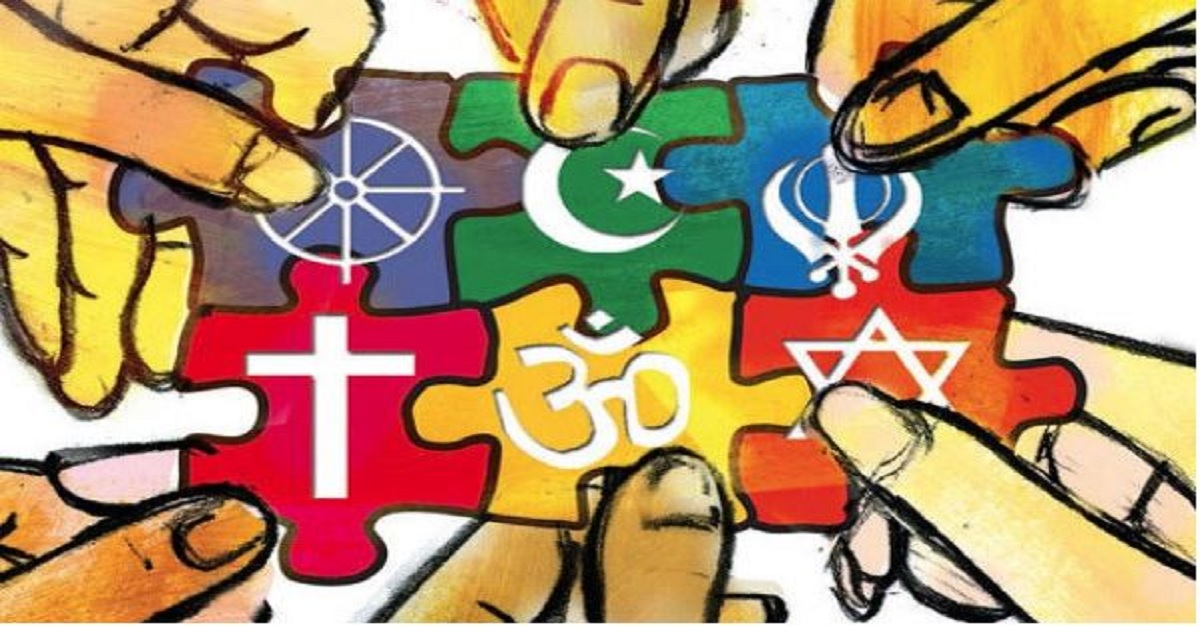
धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य शक्ति के इस्तेमाल पर सीधा प्रभाव डालने वाले एक फैसले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य के विवादास्पद धर्मांतरण-विरोधी कानून पर एक प्रारंभिक और महत्वपूर्ण न्यायिक अंकुश लगाया है। यह फैसला 17 जुलाई 2025 को मुस्तफा एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य मामले में सुनाया गया, जिसमें तीन मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया था। उन पर हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश का आरोप लगाया गया था। 2022 में पारित कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार संरक्षण अधिनियम (KPRFR अधिनियम) के तहत यह न्यायिक व्याख्या अभी प्रारंभिक अवस्था में है। यह निर्णय भले ही अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर नहीं गया, लेकिन इसने कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय स्थापित किए हैं, जो इस कानून की प्रारंभिक व्याख्या की दिशा तय करेंगे। गौरतलब है कि जब यह कानून पारित किया गया था, तब राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता में थी। मई 2023 में भारी बहुमत से सत्ता में आई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) ने इस कानून को निरस्त करने का वादा किया था, लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बावजूद यह कानून आज भी विधि पुस्तिकाओं में बरकरार है।
यह निर्णय एक महत्वपूर्ण न्यायिक फैसला है। इसकी विशेषता इस बात में नहीं है कि इसने किसी कानून को रद्द किया - क्योंकि यह अधिनियम अब भी विधि पुस्तिकाओं (statute books) में बरकरार है- बल्कि इसमें दी गई राहत के विशिष्ट कानूनी आधारों में निहित है। उच्च न्यायालय ने लोकस स्टैंडी (यानी शिकायत दर्ज कराने का अधिकार) और प्रथम दृष्टया आपराधिक मामला स्थापित करने में हुई विफलता पर जोर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि तीसरे पक्ष के स्वयंभू निगरानीकर्ताओं द्वारा इस कानून के संभावित दुरुपयोग के खिलाफ एक मिसाल स्थापित हुई। धर्मांतरण विरोधी इस अधिनियम की प्रारंभिक व्याख्या के रूप में, मुस्तफा मामले का निर्णय एक स्पष्ट मिसाल पेश करता है, जिसके आधार पर इस प्रकार की अभियोजन कार्रवाइयों को चुनौती दी जा सकती है भले ही सरकार ने कर्नाटक में इस कानून को निरस्त करने की योजना बना रखी हो।
मामले के तथ्य
मुस्तफा मामले में प्रस्तुत तथ्य ठीक उसी प्रकार की स्थिति दर्शाते हैं, जिसके लिए कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार संरक्षण अधिनियम (KPRFR Act) को कथित रूप से बनाया गया था। 4 मई 2025 को रामतीर्थ मंदिर, जमखंडी के एक भक्त रमेश मल्लप्पा नावि ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता इस्लामिक पुस्तिकाएं बांट रहे थे और जब उन्हें रोका गया, तो उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। साथ ही उन्होंने कथित रूप से यह भी कहा कि उनका उद्देश्य “पूरी दुनिया को इस्लाम की ओर मोड़ना” है और जो रास्ते में आएगा उसे देख लेंगे। आज के भारत में, यह जानकारी शायद किसी गुस्से भरे व्हाट्सऐप फॉरवर्ड की विषयवस्तु बन सकती है, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत - सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य जैसी सीमाओं के अधीन- प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का समान अधिकार प्राप्त है।
इस मामले में दर्ज एफआईआर में KPRFR अधिनियम की विशिष्ट भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ताओं ने धर्मांतरण के लिए लोगों को “लुभावने प्रलोभन” -जैसे वाहन और दुबई में नौकरी के मौके-दिए। इस तरह का “लालच” इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित अपराध का एक केंद्रीय आधार है। चूंकि प्रस्तुत तथ्य लगभग उसी प्रकार के थे जिन्हें यह कानून लक्षित करता है, इसलिए यह मामला कानून के इस्तेमाल की सीधी न्यायिक परीक्षा के लिए उपयुक्त प्रतीत हो रहा था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस पर फैसला देते समय संविधानिक वैधता की व्यापक पड़ताल में जाए बिना ही अभियोजन पक्ष के मामले में मौलिक प्रक्रियात्मक और तथ्यात्मक त्रुटियों को आधार बनाया।
पहला आधार: शिकायत दर्ज करने का अधिकार किसे है?
अदालत द्वारा एफआईआर रद्द करने का प्रमुख कारण यह था कि शिकायतकर्ता के पास कानूनी हैसियत (legal standing) नहीं थी। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि यह शिकायत एक "तृतीय पक्ष" द्वारा दर्ज की गई थी जो अधिनियम की धारा 4 में निर्दिष्ट व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं आता।
इसी आधार पर एफआईआर का पंजीकरण “कानूनी रूप से अमान्य” करार दिया गया।
KPRFR अधिनियम की धारा 4 यह स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि शिकायत केवल वही व्यक्ति दर्ज कर सकता है जिसका कथित रूप से धर्मांतरण किया गया हो या फिर उसके माता-पिता, भाई-बहन, या बेहद करीबी रिश्तेदार, विवाह या गोद लेने के संबंध से जुड़े कोई अन्य रिश्तेदार। इस मामले में शिकायतकर्ता मंदिर में मौजूद एक दर्शक (bystander) था, जो इन मानकों में से किसी में भी फिट नहीं बैठता।
इस प्रावधान का सख़्ती से पालन एक स्पष्ट संदेश देता है कि: इस आपराधिक कानून की प्रक्रिया किसी भी सामान्य नागरिक या वैचारिक रूप से प्रेरित कार्यकर्ता द्वारा शुरू नहीं की जा सकती। इस व्याख्या के जरिए न्यायपालिका ने इस अधिनियम और अन्य राज्यों में इसके समकक्ष कानूनों में प्रयुक्त व्यापक और अस्पष्ट भाषा के खिलाफ एक महत्वपूर्ण न्यायिक संतुलन स्थापित किया है। उदाहरण के लिए, कर्नाटक अधिनियम में शिकायत की अनुमति “किसी भी रूप में जुड़े व्यक्ति या सहकर्मी” को दी गई है -जो बेहद अस्पष्ट है। वहीं उत्तर प्रदेश कानून में हालिया संशोधन के तहत “कोई भी व्यक्ति” एफआईआर दर्ज करा सकता है। इस तरह के नियम जनता को न्यायिक प्रक्रिया में तृतीय पक्ष के रूप में शामिल कर देते हैं, जो स्वयंभू निगरानी समूहों (vigilante groups) के कारण पैदा होने वाले झूठे और परेशान करने वाले मुकदमों के लिए रास्ता खोलते हैं।
मुस्तफा मामला में फैसले की तर्कसंगत व्याख्या कानूनी प्रक्रिया को उस व्यक्ति पर केंद्रित करती है, जिसके अधिकार वास्तव में खतरे में हैं, यानी कथित अवैध धर्मांतरण का शिकार।यह ध्यान किसी बाहरी व्यक्ति की चोटिल भावनाओं से हटाकर उस व्यक्ति पर ले जाता है, जिसे अपनी मान्यता और विश्वास की आज़ादी का असली नुकसान हुआ हो। यह एक प्रकार की “प्रक्रियात्मक सुरक्षा” (procedural firewall) बनाता है, जो एक प्रारंभिक कानूनी तर्क के रूप में काम करता है। अब वकील इस तर्क का इस्तेमाल उन मामलों को चुनौती देने के लिए कर सकते हैं जो सामान्य आरोपों या सांप्रदायिक नफरत से प्रेरित होते हैं।
दूसरा आधार: क्या कोई “धर्मांतरण का प्रयास” हुआ?
प्रक्रियात्मक खामी के अलावा उच्च न्यायालय ने शिकायत की सामग्री में एक बड़ा दोष पाया। एफआईआर में दर्ज सभी आरोपों को सच मानते हुए भी, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वे “अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध के आवश्यक तत्वों को पूरा करने में असफल हैं।”
न्यायालय की बात बिल्कुल स्पष्ट थी: “यह कहीं भी आरोप नहीं लगाया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने किसी व्यक्ति का धर्मांतरण किया या करने की कोशिश की।” यह निष्कर्ष अभियोजन के लिए एक बड़ी कसौटी तय करता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल सामान्य स्तर पर किए गए धर्म प्रचार के कार्य-जैसे साहित्य बांटना, धार्मिक बहस करना आदि-अपने आप में इस अधिनियम के तहत अपराध नहीं माने जा सकते। इस कानून को लागू करने के लिए राज्य को यह साबित करना होगा कि कोई विशेष, लक्षित कार्य किसी पहचाने जा सकने वाले व्यक्ति को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से किया गया था।
यह भेद स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 25 के तहत धर्म “प्रचार” करने के संवैधानिक अधिकार और KPRFR अधिनियम के तहत “धर्मांतरण का प्रयास” जैसी दंडनीय कार्रवाई के बीच एक महत्वपूर्ण रेखा खींचता है। न्यायालय का संकेत है कि किसी धार्मिक अभिव्यक्ति को जब तक वह किसी विशेष व्यक्ति के प्रति लक्षित ठोस धर्मांतरण प्रयास में न बदले, तब तक उसे संविधानिक संरक्षण प्राप्त रहेगा और वह आपराधिक कृत्य नहीं मानी जाएगी। मुस्तफा एफआईआर में याचिकाकर्ताओं की गतिविधियों का विस्तृत विवरण होने के बावजूद, ऐसा कोई आरोप नहीं था कि उन्होंने किसी व्यक्ति को धर्मांतरण के लिए निशाना बनाया। इसी कारण शिकायत कानूनी रूप से उपयुक्त नहीं मानी गई। यह निर्णय एक और महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है जिससे बचाव पक्ष (defence counsel) के पास यह ठोस दलील उपलब्ध हो जाती है कि इस अधिनियम का इस्तेमाल केवल धर्म प्रचार या संवाद जैसी गतिविधियों को अपराध ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता।
राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य: कानून को लगातार कठोर बनाते जाने की प्रवृत्ति
कर्नाटक का यह अधिनियम कोई अलग-थलग कानून नहीं है, बल्कि एक समन्वित राष्ट्रीय प्रवृत्ति का हिस्सा है। 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों ने या तो नए धर्मांतरण-रोधी कानून बनाए हैं या मौजूदा कानूनों में संशोधन किए हैं और हर नया कानून अपने पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक कठोर साबित हुआ है। इन नए कानूनों की बनावट और वैचारिक आधार लगभग एक जैसे हैं और अक्सर इन्हें तथाकथित “लव जिहाद” के निराधार नैरेटिव और जनसंख्या संतुलन को लेकर फैलाई जा रही आशंकाओं के तर्क पर न्यायोचित ठहराया जाता है।
इन कानूनों की विशेषताएं इस प्रकार हैं:
● अत्यधिक व्यापक परिभाषाएं: “प्रलोभन” जैसे शब्दों को इतनी व्यापकता से परिभाषित किया गया है कि यदि कोई धार्मिक संस्था नि:शुल्क शिक्षा या रोजगार का अवसर देती है, तो उसे भी अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है। इससे वैध और परोपकारी कार्यों के आपराधिक दायरे में आने का खतरा बनता है।
● अंतरधार्मिक विवाह को निशाना बनाना: “शादी का वादा” धर्मांतरण के लिए प्रतिबंधित माध्यमों में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है, जो वयस्कों को अपने जीवनसाथी चुनने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सीधा दखल देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा माना है।
●पक्षपातपूर्ण अपवाद: इन कानूनों में से कुछ “पूर्व धर्म में पुनः धर्मांतरण” (reconversion) को विशेष छूट देते हैं, यानी व्यक्ति के “तत्काल पूर्व धर्म” में वापसी को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है। यह प्रावधान व्यापक रूप से एक एकतरफा रास्ते के रूप में देखा जा रहा है, जो हिंदू धर्म में वापसी को वैध मानते हुए, अन्य धर्मों में धर्मांतरण को दंडनीय बनाता है।
● दखल देने वाली प्रक्रियाएं: ये कानून धर्मांतरण से पहले और बाद में ज़िलाधिकारी के समक्ष विस्तृत घोषणा प्रक्रिया को अनिवार्य बनाते हैं जिसमें सार्वजनिक सूचना जारी करना और पुलिस जांच तक शामिल है। इस प्रक्रिया के चलते, व्यक्तिगत आस्था का विषय एक लोक परीक्षण और नौकरशाही मंज़ूरी के दायरे में आ जाता है।
● कठोर दंड: उदाहरण के लिए राजस्थान के धर्मांतरण विरोधी कानून में अपराध गंभीर (cognizable) और गैर जमानती (non-bailable) घोषित किए गए हैं। इतना ही नहीं, सबूत का भार (burden of proof) भी उलट दिया गया है यानी आरोपी को यह साबित करना होगा कि धर्मांतरण वैध था। यह न्याय के उस मूल सिद्धांत के विपरीत है, जिसमें माना जाता है कि "जब तक दोष सिद्ध न हो, व्यक्ति निर्दोष है।"
यह बेहद दखल देने वाली और मौलिक अधिकारों की खुली अवहेलना पूरे देश में कानूनी चुनौती का विषय बन चुकी है। देश भर की विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में इन कानूनों के खिलाफ कई याचिकाएं लंबित हैं।
इन कानूनों को दी जा रही कानूनी चुनौती सुप्रीम कोर्ट की दो परस्पर-विरोधी व्याख्याओं के बीच संभावित टकराव की जमीन तैयार कर रही है। एक ओर है साल 1977 का फैसला रेव. स्टेनिसलौस बनाम मध्य प्रदेश राज्य (Rev. Stainislaus v. State of Madhya Pradesh) जिसमें संविधान पीठ (Constitution Bench) ने शुरुआती धर्मांतरण विरोधी कानूनों को वैध ठहराया था। इस निर्णय में अनुच्छेद 25 के तहत धर्म “प्रचार” करने के अधिकार की व्याख्या सीमित रूप में की गई, यह कहते हुए कि इसमें किसी दूसरे व्यक्ति को धर्मांतरित करने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। इस फैसले ने इन कानूनों को वैध ठहराने के लिए राज्य को “लोक व्यवस्था बनाए रखने” की शक्ति का आधार माना था।
दूसरी ओर है आधुनिक और व्यापक व्याख्या, जो व्यक्तिगत स्वायत्तता (individual autonomy) को केंद्र में रखती है जिसे साल 2017 के ऐतिहासिक निर्णय जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (Right to Privacy) में जिक्र किया गया था। इस मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने यह घोषणा की कि गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है जो व्यक्ति की गरिमा, निजी स्वायत्तता, और जीवन से जुड़े बुनियादी निर्णयों जैसे परिवार, विवाह और आस्था को स्वतंत्र रूप से लेने की स्वतंत्रता को शामिल करता है।
नए धर्मांतरण विरोधी कानून जो व्यक्तिगत धार्मिक आस्थाओं पर राज्य की दखलअंदाजी और निगरानी को बढ़ावा देते हैं, इस न्यायिक मतभेद के बिल्कुल बीचों-बीच स्थित हैं। जहां स्टैनिसलौस (Stainislaus) फैसले ने जबरदस्ती या धोखे जैसे अवैध तरीकों से धर्मांतरण रोकने पर ध्यान केंद्रित किया था, वहीं ये नए कानून स्वेच्छा से धर्म बदलने के काम को ही नियंत्रित करते हैं। राज्य को अपनी धर्मांतरण की मंशा बताने और इसके लिए सार्वजनिक जांच का सामना करने की आवश्यकता, सीधे तौर पर उस “चयन और आत्म-निर्धारण के क्षेत्र” (zone of choice and self-determination) को चुनौती देती है, जिसकी रक्षा पुट्टास्वामी फैसले ने की थी।
मूलभूत संवैधानिक प्रश्न अब केवल धर्म प्रचार के अधिकार (स्टैनिसलौस वाला मुद्दा) तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह है कि क्या राज्य इतनी बोझिल और हस्तक्षेपकारी प्रक्रिया को एक बेहद व्यक्तिगत निर्णय पर थोप सकता है, बिना व्यक्ति के निजता और स्वतंत्रता के अधिकार (पुट्टास्वामी वाला मुद्दा) का उल्लंघन किए।
आगे का रास्ता
मुस्तफा मामले का निर्णय न्यायपालिका की एक सतर्क और सीमित दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण परिणाम है, जो केवल कानून की भाषा पर आधारित रहा। यह फैसला तत्काल और ठोस राहत प्रदान करता है, साथ ही बिना किसी सीधे संवैधानिक टकराव को जन्म दिए कुछ अहम प्रक्रियात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस निर्णय की विरासत यह होगी कि यह अभियुक्तों और उनके वकीलों को ऐसे सटीक और प्रभावी कानूनी तर्क देता है, जिनके जरिए वे मुकदमे की शुरुआत में ही अभियोजन को चुनौती दे सकें और इस तरह कानून के दुरुपयोग की संभावनाओं पर समय रहते रोक लगाई जा सके।
हालांकि असली लड़ा अभी बाकी है। KPRFR अधिनियम और उसके जैसे अन्य धर्मांतरण विरोधी कानूनों की मूल धाराओं - जैसे उनकी विस्तृत परिभाषाएं, पक्षपातपूर्ण प्रावधान और हस्तक्षेपकारी प्रक्रियाएं — को अब भी संविधान की कसौटी पर पूरी तरह परखा जाना बाकी है। आखिरकार, सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना होगा कि जबरन धर्मांतरण रोकने में राज्य का हित कहां तक जायज है -और वह कहां पर व्यक्ति की निजता, स्वतंत्रता, समानता और अंतरात्मा की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों से टकराता है। मुस्तफा मामले में फैसला इस व्यापक संवैधानिक बहस का पहला महत्वपूर्ण अध्याय है- एक स्थिर और विवेकपूर्ण निर्णय, जिसने प्रक्रिया संबंधी जरूरी स्पष्टता प्रदान की है, जबकि अहम संवैधानिक पड़ताल अब भी बाकी है।
(लेखक इस संगठन की कानूनी शोध टीम का हिस्सा हैं।)
Related



