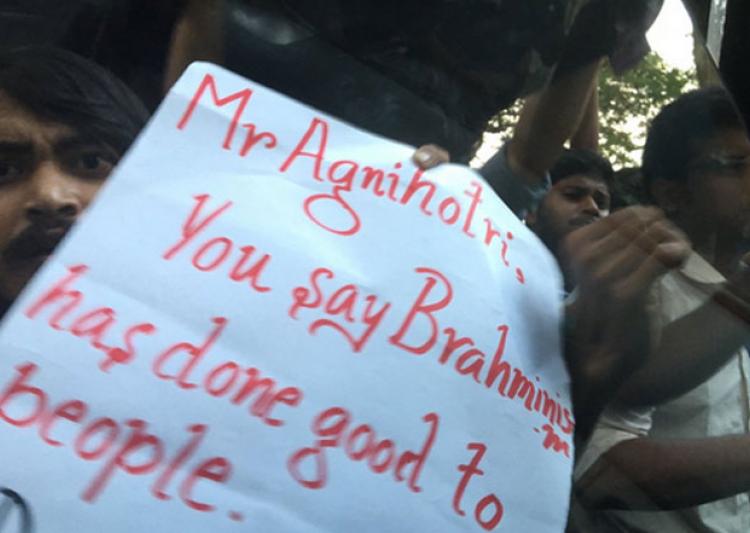
Image Courtesy:IANS
देश के 'सबसे बड़े दुश्मनों' और 'सबसे बड़ी समस्याओं' से लड़ने के तरीके और उनसे पार पाने के 'रास्ते' अब वॉलीवुड के फिल्मकारों ने बताना शुरू कर दिया है! हालांकि सिनेमा के परदे पर 'उपदेश' तो पहले भी होते थे, लेकिन उन्हें 'फिल्मी' कह और मान कर माफ कर दिया जाता था! लेकिन अब फिल्में बाकायदा राजनीतिक एजेंडे के तहत दर्शकों को संबोधित करती हैं।
इस लिहाज से देखें तो 'बुद्धा इन ए ट्राफिक जाम' के निर्माता-निर्देशकों ने नक्सलवाद और सरकारी तंत्र के फंसे आदिवासियों की सभी तकलीफों या समस्याओं का हल निकाल लिया है, आदिवासियों के उद्धारकों की खोज कर ली है! यह उद्धारक है 'बिजनेस' और जाहिर है 'बिजनेसमैन' यह उद्धार करने के लिए अपने और आदिवासियों के बीच के सारे 'मिडिलमैन' यानी बिचौलिये को खत्म करना चाहता है!
परदे पर शुरुआती दो दृश्यों में पिछले डेढ़ दशक से एक हालत में अभाव की जिंदगी जीते एक निरीह, लाचार आदिवासी को सत्ता और नक्सलियों के बीच पिसने के 'मार्मिक' दृश्यों के जरिए हॉल में बैठे दर्शकों को सहानुभूति के सागर में गोते लगाने पर मजबूर किया जाता है, फिर 'लोक-स्पर्श' के गीत के जरिए बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कराने वाले आधुनिक लड़के-लड़कियों को अपना 'सरोकार' जताते दिखाया जाता है। इस 'सरोकार' प्रदर्शन में पश्चिमी अंगरेजी मादकता है, शराब है, नशा है, एक बिंदास उन्माद है, 'नैतिक पुलिस' का हमला है... और सब पर 'सरोकार' का संगीत है..!
नक्सली क्यों और कैसे उगे, एनजीओ कैसे और क्यों उगे, सरकार की क्या जवाबदेही है, व्यवस्था की नाकामी के लिए कौन जिम्मेदार है, इससे सबसे फिल्मकार को कोई मतलब नहीं।
खैर, फिल्म आगे बढ़ती है और बताती है कि कैसे एक प्रोफेसर (अनुपम खेर) इतने बड़े बिजनेस स्कूल में घुसपैठ करके वहां के विद्यार्थियों को नक्सली बनाने की फिराक में है, एक 'भोले' स्टूडेंट (अरुणोदय) सिंह को वह इसके लिए फंसाना चाहता है, नक्सलियों के कमांडर तक कैसे प्रोफेसर की सीधी पहुंच है, घर में उसका दोहरा चेहरा है और उसकी पत्नी तक को नहीं मालूम कि वह नक्सली है! एक एनजीओ चलाने वाली या कार्यकर्ता कैसे सरकार से फंड लेकर वह पैसा नक्सलियों तक पहुंचाती हैं, वह प्रोफेसर कैसे सीधे आदिवासियों की मदद के प्रस्ताव को खारिज कर देता है। नक्सली राष्ट्रद्रोही हैं, उन्होंने जितने जवानों को मारा, उतने तो कारगिल जैसी लड़ाइयों में भी नहीं मारे गए! ये नक्सली एनजीओ वाले और बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर की तरह चेहरा बदल कर सिस्टम के हर कोने में पैठ चुके हैं और अमेरिका की चकाचौंध को ठुकरा कर भारत में बिजनेस के जरिए उद्धार करने की आकांक्षा पाले एक 'लाचार' नौजवान को कैसे इन सबसे डरना चाहिए। परदे पर परदा, विरोधाभासों के बीच..!
बहरहाल, इसमें बदलाव का सपना लिए 'पिंक चड्ढी कैंपेन' चलाने वाले इस बिजनेस के दीवाने नौजवान के अलावा एक और 'लाचार' पक्ष है- सत्ता! सत्ता पूरी तरह निर्दोष है, मासूम है, वह आदिवासियों का कल्याण करने के लिए एनजीओ वालों को पैसा देती है और वे लोग वह पैसा नक्सलियों तक पहुंचा देते हैं! इसका हल सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है, जो हर तरह के बिचौलियों को खत्म करके सीधे आदिवासियों का 'कल्याण' करेगा! वह बिचौलिया चाहे एनजीओ वाले हों या सरकार हो!
नक्सली क्यों और कैसे उगे, एनजीओ कैसे और क्यों उगे, सरकार की क्या जवाबदेही है, व्यवस्था की नाकामी के लिए कौन जिम्मेदार है, इससे सबसे फिल्मकार को कोई मतलब नहीं। उसकी निगाह में आदिवासियों का भला सिर्फ और सिर्फ इंडियन बिजनेस स्कूल, बिजनेस और बिजनेसमैन ही कर सकते हैं! आदिवासियों के लिए संवेदना का समंदर हाथ में लिए बिजनेस-सॉल्यूशन-मॉडल में समूचे देश में जमीन कब्जाने के खेल पर सोचने की कोई जरूरत नहीं, इस मॉडल में मजदूरों के सवालों के लिए कोई जगह नहीं, इससे सरकार या तंत्र की जरूरत और उसकी जिम्मेदारियों का क्या होगा, इसकी फिक्र नहीं, सरकार की जिम्मेदारियों पर सवाल खड़े करने के बजाय उसे नाकारा बना कर पेश करना मकसद, लेकिन इस समूचे मसले पर एक खास राजनीतिक धारा के नजरिए का विस्तार...! इसी लोकेशन से मां शब्द से जुड़ी वीभत्स गाली का इतनी बार इस्तेमाल है कि जुगुप्सा हो जाती है...! लगता है कि फिल्मकार का मन इसी गाली में डूबा हुआ है..!
एक ऐसा विषय क्यों, उसके साथ खिलवाड़ क्यों, उसमें सरकार से लेकर राजनीतिक दलों तक भूमिका की अनदेखी क्यों, जिसमें एक बड़ी आबादी कीड़ों-मकोड़ों की तरह समझी जा रही है, जमीन कब्जाने का व्यापक खेल चल रहा है!
दिखने के लिए 'भारत माता की जय' के साथ मां की सबसे 'मशहूर' और वीभत्स गाली परोसने के सिरे से लगता है कि इसमें किसी के पक्ष से नहीं खेला गया है, लेकिन इस 'औपचारिकता' के अलावा जिन-जिन राजनीतिक धाराओं और संस्थानों को कठघरे में किया गया है, सरकार और तंत्र को बख्श दिया गया है, उससे इस फिल्म की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं! नक्सली संगठनों के बारे में अलग से कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया गया, जो प्रचारित है। लेकिन सरकार क्या करती है, आदिवासी किन वजहों से उस हालत में पहुंचे, उसमें सरकार की क्या भूमिका या जिम्मेदारियां हैं, दो पाटों के बीच से वे कैसे निकलेंगे, इस पर जानबूझ कर परदा..! जवाब होगा कि एक फिल्म क्या-क्या करेगी! ठीक है! तो फिर यही क्यों किया..!
फिल्में अगर राजनीति नहीं हैं, एक एजेंडे के तहत नहीं बनाई गई, मनोरंजन हैं तो सलमान खान या कपिल शर्मा टाइप क्यों नहीं! एक ऐसा विषय क्यों, उसके साथ खिलवाड़ क्यों, उसमें सरकार से लेकर राजनीतिक दलों तक भूमिका की अनदेखी क्यों, जिसमें एक बड़ी आबादी कीड़ों-मकोड़ों की तरह समझी जा रही है, जमीन कब्जाने का व्यापक खेल चल रहा है! मारी जा रही आबादी की तकलीफों के साथ खिलवाड़ का अधिकार-पत्र कहां से जारी हुआ है..!
...और! एक जिक्र कि 'बुद्ध के समय का एक गांव इसलिए आज भी मौलिक कलाकृतियों के जरिए अपनी संस्कृति और इतिहास बता रहा है कि आज तक वहां कोई 'बाहरी' नहीं पहुंचा', शायद इस फिल्म के नाम 'बुद्धा इन ए ट्राफिक जाम' का आधार है। लेकिन क्या यह नाम इतना भोला और मासूम है..!
Source: 'चार्वाक' ब्लॉग से



