सितंबर 2025 में "I Love Muhammad" विवाद के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सार्वजनिक चेतावनियां जैसे “छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं” और “डेंटिंग-पेंटिंग जरूरी है” जल्दी ही जमीनी कार्रवाई में बदलती दिखीं। इन बयानों के तुरंत बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुईं, संपत्तियों की तोड़फोड़ और इंटरनेट सेवाओं का बंद होना शुरू हो गया। यह पूरा सिलसिला कानूनी वैधता और सरकारी बयानबाज़ी के सामाजिक असर को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।

सितंबर 2025 में शुरू हुए “आई लव मुहम्मद” विवाद के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार-बार सार्वजनिक बयान दिए। विशेष रूप से 28 सितंबर को अपने बयान में सार्वजनिक व्यवस्था को “परेशान” करने वालों के लिए सख्त, स्पष्ट सजा का वादा करते हुए कहा कि, “छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं”, “पीढ़ियां याद रखेंगी”, “गजवा-ए-हिंद सफल नहीं होगा और इसके बजाय उसे नरक का टिकट दिया जाएगा” और “डेंटिंग और पेंटिंग की जानी चाहिए” जैसी बातें की।
हालांकि यह भाषण बरेली विरोध प्रदर्शन पर स्थानीय कार्यकारी प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन इसका प्रचार और प्रसार मुख्यतः राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया, खासकर टाइम्स नाउ नवभारत, जी न्यूज़ हिंदी और न्यूज़18 हिंदी जैसे हिंदी टेलीविजन चैनलों के माध्यम से हुआ, जिन्होंने मुख्यमंत्री के शब्दों को विरोध प्रदर्शनों, पुलिस कार्रवाई और संपत्ति तोड़फोड़ के तस्वीरों के साथ जोड़ा। सोशल मीडिया पर छोटे-छोटे क्लिप खूब वायरल हुए, जिससे एक फीडबैक लूप बना जिसने बयानबाजी और राज्य की प्रतिक्रिया, दोनों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया।
मीडिया द्वारा किए गए इस प्रचार ने स्थानीय कानून-व्यवस्था के मुद्दे को दंडात्मक शासन के राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देने वाले तमाशे में बदल दिया, जिसमें बलपूर्वक लागू करना और एक धार्मिक समुदाय को निशाना बनाना सामान्य बात हो गई। प्रचार के समय और पैमाने का राजनीतिक महत्व भी हो सकता है, खासकर आगामी बिहार चुनावों के संदर्भ में, क्योंकि हिंदी भाषी मीडिया नेटवर्क ने यह तय किया कि मुख्यमंत्री की बयानबाजी व्यापक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दर्शकों तक पहुंचे।
कुछ ही दिनों में बरेली में सरकारी कार्रवाई तेज हो गई: बड़े पैमाने पर गिरफ़्तारियां, संपत्तियां सील करने और तोड़फोड़ की कार्रवाई, 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद, आपराधिक एफआईआर (कुछ मामलों में सैकड़ों या हजारों तक) और बरेली में विरोध प्रदर्शन का आह्वान करने वाले मौलवी के सहयोगियों के खिलाफ प्रशासनिक नोटिस जारी किए गए। 'विरोध फिर मुख्यमंत्री की बयानबाजी फिर सख्त कार्रवाई' का यह क्रम तीन जुड़े हुए सवाल खड़े करता है जिनकी इस लेख के बाकी हिस्से में गहराई से पड़ताल की गई है:
● क्या मुख्यमंत्री के भाषण ने उकसावे या गैरकानूनी भेदभाव जैसी कानूनी सीमाओं को पार किया?
● क्या राज्य की प्रतिक्रिया में उचित प्रक्रिया और सर्वोच्च न्यायालय के अपने सुरक्षा उपायों (नफरत फैलाने वाले भाषण की स्वतः जांच करने के ड्यूटी सहित) का पालन किया गया?
● उस राजनीतिक बयानबाजी के सामाजिक, कानूनी और मीडिया पर क्या मापा जा सकने वाला परिणाम हैं?
जो कुछ हुआ उसकी टाइमलाइन
प्रारंभिक घटना (4–9 सितंबर, 2025): यह विवाद 4 सितंबर से शुरू हुआ, जब कानपुर के कुछ इलाकों (सैयद नगर/रावतपुर) में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी की जुलूस के दौरान “I Love Muhammad” लिखा हुआ बोर्ड या बैनर देखा गया। कुछ हिंदुत्ववादी समूहों ने इसे “परंपरा से भटकाव” बताया और स्थानीय स्तर पर इसका विरोध किया। इस विवाद के बाद पुलिस ने 9 सितंबर को 24 लोगों (9 नामजद और 15 अज्ञात) के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द भंग करने के आरोप में FIR दर्ज की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, शिकायत का मुख्य आधार यह था कि टेंट और बैनर को राम नवमी के जुलूसों के मार्ग के नजदीक एक आम सड़क पर स्थानांतरित किया गया था। यह मामूली बदलाव जल्द ही खबरों और सोशल मीडिया के जरिए दूसरे जिलों तक फैल गया।
विवाद में वृद्धि और बरेली प्रदर्शन (26–27 सितंबर, 2025): 26 सितंबर को बरेली में एक सार्वजनिक सभा हुई, जिसे “I Love Muhammad” अभियान के समर्थन में बुलाया गया था और जिसका संबंध धर्मगुरु तौकीर रजा खान से था। इस सभा के बाद शुक्रवार की नमाज के बाद पुलिस के साथ झड़पें हुईं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पत्थरबाजी की घटनाएं भी हुईं, जिसमें कई अधिकारी घायल हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों का कहना है कि यह प्रदर्शन बिना अनुमति के किया गया था। पुलिस ने यह भी कहा कि यह सभा सोशल मीडिया समूहों के माध्यम से पूर्व योजना के संकेत देती थी। इसके बाद कई FIR दर्ज की गईं और दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया गया। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक दर्जनों लोग हिरासत में हैं और सैकड़ों के खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं - जबकि कुछ मीडिया सूत्रों के अनुसार, कई थानों में FIR की संख्या हजारों तक पहुंच गई है। झड़पों के तुरंत बाद धर्मगुरु और उनके कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया (28 सितंबर, 2025): ‘विकसित यूपी’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग “धर्म के नाम पर तोड़फोड़ करते हैं… पुलिस पर हमला करते हैं… उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे… छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं और छोड़ेंगे नहीं तो फिर छूटोगे भी नहीं।” उन्होंने कहा कि “डेंटिंग और पेंटिंग तो करनी ही पड़ेगी” और इस प्रतिक्रिया को त्योहारों और सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा के लिए जरूरी बताया। ये बयान नेशनल न्यूज आउटलेट में उसी दिन और अगले दिन और उसके बाद भी व्यापक रूप से प्रकाशित किए गए।




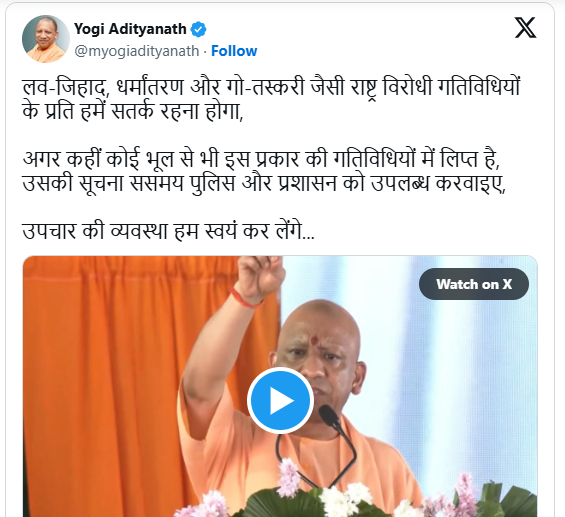
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा दिए गए भाषण:
2025 में हिंसा और भाषणों के बाद जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गईं और FIR दर्ज की गईं। आरोपी व्यक्तियों से जुड़े संपत्तियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा सील किया गया या तोड़ दिया गया, जिसमें एक बैंक्वेट हॉल और अन्य संरचनाएं भी शामिल थीं, जिनका कथित रूप से गिरफ्तार लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। प्रशासन ने तौकीर रजा खान के सहयोगियों के खिलाफ विद्युत चोरी जैसे नोटिस भी जारी किए। इकॉनोमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, बरेली जिले में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट और SMS सेवाएं 48 घंटे के लिए निलंबित कर दी गईं। कई मानवाधिकार और कानूनी कार्यकर्ताओं ने पहले ही बिना पूर्व सूचना के संपत्तियों के ध्वस्त किए जाने और संभावित सामूहिक दंड के खिलाफ याचिकाएं और शिकायतें दर्ज करवाई हैं। राजनीतिक पार्टियां और नागरिक समाज के प्रतिनिधिमंडल शहर का दौरा करना शुरू कर चुके हैं। विपक्षी नेता जांच की मांग कर रहे हैं।
भाषण की मूल समस्या
1. निशाना बनाना और व्यक्तिगत संदर्भ: मुख्यमंत्री ने खास तौर पर एक धर्मगुरु तौकीर रजा खान और उनके द्वारा लोगों के बीच की गई बातों पर हमला किया, यह कहते हुए कि "मौलाना भूल गए हैं कि सत्ता किसके पास है" और "ऐसा बदला दिया जाएगा जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी।" किसी पहचाने जाने वाले नेता को निशाना बनाना और उसे तथा उनके समर्थकों को हिंसा से जोड़ना, भाषण को केवल सामान्य कानून-व्यवस्था की भाषा से कहीं आगे ले जाता है।
2. सजा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति को शाब्दिक रूप में लेना: "डेंटिंग और पेंटिंग" के बार-बार इस्तेमाल और "बुलडोजर" का उल्लेख, जो हाल के यूपी अभियानों में तोड़फोड़ के साथ जुड़े हैं, केवल प्रतीकात्मक नहीं हैं। वर्तमान यूपी के संदर्भ में यह एक संस्थागत इतिहास है - दंड के सार्वजनिक प्रदर्शन के रूप में एक राज्य का तमाशा, जिसके वास्तविक परिणाम होते हैं। इसलिए यह वाक्यांश नीतिगत संकेत और सार्वजनिक चेतावनी दोनों के रूप में पढ़ा जाता है।
3. समुदाय के प्रति शक्ति और रोकथाम का संदेश: हालांकि तत्काल कारण हिंसा थी, मुख्यमंत्री का वाक्य -“अगर तुम हमें परेशान करोगे, तो हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं” - विशेष रूप से एक विशिष्ट प्रकार की अभिव्यक्ति को रोकने के लिए था, जैसे कि “I Love Muhammad” पोस्टर दिखाना, जिसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं और कुछ नागरिक समाज के लोगों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माना और उसकी रक्षा की थी। इस तरह की बातों को अवैध ठहराना, नारे को बच्चों की मनमानी या अराजकता के रूप में दिखाना, साथ ही सामूहिक अनुशासन का वादा करना, इसके गंभीर परिणाम होते हैं।
वे तीन विशेषताएं - नाम लेना, सजा की सांकेतिक भाषा और सामान्यीकृत रोकथाम - ऐसी बातें हैं जो कानूनी और मानक विश्लेषण को बेहद जरूरी बनाती हैं।
मीडिया: किसने बढ़ावा दिया और किस प्रकार इस बढ़ावा ने कहानी को बदला
मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों को स्थानीय राजनीतिक प्रतिक्रिया से राष्ट्रीय स्तर पर एक शक्तिपूर्ण प्रदर्शन में बदलने में निर्णायक भूमिका निभाई। उनके भाषण के कुछ ही घंटों के भीतर, टेलीविजन और प्रिंट मीडिया दोनों ने उनके सबसे आक्रामक बयानों - “छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं” और “डेंटिंग और पेंटिंग तो करनी ही पड़ेगी” - को पहले पन्ने पर प्रमुखता से जगह दी, जिससे ये प्रतिशोध के धमकी वाले बयान वायरल हो गए।
राष्ट्रीय और क्षेत्रीय ब्रॉडकास्टर्स जैसे टाइम्स नाउ नवभारत, जी न्यूज़ हिंदी, और न्यूज18 हिंदी ने ऐसे न्यूज प्रसारित किए जिनमें मुख्यमंत्री के बयानों को प्रदर्शनों, लाठीचार्ज और संपत्तियों के ध्वस्तीकरण के तस्वीरों के साथ जोड़ा गया। यूट्यूब थंबनेल और स्क्रीन पर चलने वाले टिकर स्वयं राज्य की संदेशवाहक प्रक्रिया का हिस्सा बन गए - “मौलाना भूल गया कौन सरकार में है” या “बरेली में दंगा, सरकार की कठोर कार्रवाई” जैसे टेक्स्ट ने मुख्यमंत्री की चेतावनी को एक तमाशा और नारे के रूप में पेश किया।
मीडिया की इस प्रस्तुति का दोहरा प्रभाव पड़ा। पहला, इसने मुख्यमंत्री की भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया, जिससे जो शुरूआत में एक स्थानीय सांप्रदायिक अशांति थी, वह पूरे राज्य में कानून-व्यवस्था की सफलता के रूप में पेश की गई। दूसरा, उनके बयानों का बार-बार प्रसारण - अक्सर संदर्भ से अलग और पुलिस कार्रवाई के वीडियो के साथ - दंड और रोकथाम की भाषा को सामान्य कर दिया। यहां तक कि ऐसे प्लेटफॉर्म जिन्होंने भाषण को संपादकीय रूप से समर्थन नहीं दिया वे भी पुनरावृत्ति के जरिए इसके प्रसार में योगदान देते रहे।
कुछ मीडिया संस्थान जैसे द वायर और द इंडियन एक्सप्रेस ने एक विपरीत दृष्टिकोण पेश किया: विस्तृत टाइमलाइन, “ऑनलाइन टूलकिट” के बारे में पुलिस के दावों की जांच और प्रशासन के अत्यधिक बल प्रयोग की आलोचनात्मक समीक्षा की। लेकिन ये अपवाद थे जो प्रदर्शनकारी कानून-व्यवस्था कवरेज की भारी लहर में घिरे हुए थे। फ्रेमिंग में यह विभाजन - कानून-व्यवस्था की नैरेटिव और नागरिक स्वतंत्रता की जांच - दर्शाता है कि कैसे संपादकीय रुख सांप्रदायिक घटनाओं की नैतिकता को सीधे प्रभावित करता है।
इन चैनलों के शॉर्ट-फॉर्म वीडियो, जो यूट्यूब शॉर्ट्स और ट्विटर/एक्स रील्स के रूप में निकाले गए थे, सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर प्रसारित हुए। ये क्लिप - मुख्यमंत्री की चेतावनी को हिंसा और पुलिस तैनाती के तस्वीरों के साथ जोड़ा गया - एक फीडबैक लूप बनाते हैं: जितना ज्यादा यह तस्वीर वायरल होता गया, उतना ही प्रशासनिक कार्रवाईयों जैसे इंटरनेट बंद करना और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी होती गई। प्रभावी रूप से, मीडिया पारिस्थितिकी और राज्य की जबरदस्ती की मशीन एक-दूसरे को सशक्त बनाते रहे।
यह सब एक संवैधानिक सवाल भी उठाता है जो मध्यस्थ शासन से जुड़ा है। जब कार्यकारी भाषण, पत्रकारिता द्वारा प्रचार और प्रशासनिक दबाव एक साथ काम करते हैं तो राज्य के संदेश और स्वतंत्र रिपोर्टिंग के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। नतीजा केवल सूचना का प्रसार नहीं बल्कि एक “नियंत्रण का प्रदर्शन” बन जाता है, जहां निर्णायक शासन का दिखावा कानूनी प्रक्रिया के पालन की जगह ले लेता है।
टाइम्स नाउ नवभारत, जी न्यूज हिंदी, और न्यूज18 हिंदी के यूट्यूब थंबनेल्स का एक संग्रह यहां पर दिया गया है जो इसे बखूबी दर्शाता है -ऐसे शीर्षकों का एक मोंटाज जो न्यूज कवरेज और स्टोरी नैरेटिव के बीच की सीमा को धुंधला कर देता है और दंडात्मक कार्रवाई को राजनीतिक गुण के रूप में पेश करता है।
कानूनी दृष्टिकोण: कानून क्या कहता है और न्यायालयों ने सीमा कहां खींची है
यहां तीन परस्पर जुड़े कानूनी नियम महत्वपूर्ण हैं:
● “नफरत”/सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित भाषण के लिए कानूनी प्रावधान: भारत के दंड संहिता में ऐसे भाषणों को दंडनीय ठहराया गया है जो समूहों के बीच वैमनस्य या नफरत को बढ़ावा देते हैं (जैसे, IPC धारा 153A/धारा 198 बीएनएस), राष्ट्रीय एकता के खिलाफ आरोप लगाना (IPC धारा 153B/धारा 197 बीएनएस), धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य (IPC धारा 295A/धारा 298 बीएनएस), और ऐसे बयान जो आतंक या सार्वजनिक डर पैदा करने की संभावना रखते हों (IPC धारा 505/धारा 356 बीएनएस)। ये वे प्रावधान हैं जिनका पुलिस और अदालतें आमतौर पर सांप्रदायिक भाषण के मामलों में इस्तेमाल करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जोर दिया है कि कानूनी प्रतिबंध सटीक और अनुपातिक होने चाहिए।
● सर्वोच्च न्यायालय का नफरती भाषण पर कार्रवाई का दायित्व: शाहीन अब्दुल्ला और बाद के आदेश: शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ (2022) में, सर्वोच्च न्यायालय ने “नफरत के बढ़ते माहौल” को रेखांकित किया और पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे नफरती भाषण की घटनाओं में स्वतः संज्ञान लें - विशेष रूप से IPC की धारा 153A, 295A और 505 के तहत FIR दर्ज करने और जांच करने का आदेश दिया, बिना किसी निजी शिकायत के इंतजार किए। ये निर्देश बाद में सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों तक लागू किए गए। न्यायालय ने यह माना कि सक्रिय पुलिसिंग से ही संविधान के प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को सुरक्षित रखा जा सकता है। इस न्यायशास्त्र के तहत राज्य पुलिस पर जिम्मेदारी आती है: यदि सार्वजनिक वक्तव्य संभवतः नफरती भाषण का स्वरूप रखता हो, तो पुलिस को स्वतः ही उसकी जांच करनी चाहिए।
● संविधानिक सीमा: हिंसा भड़काने की मंशा और उससे प्रत्यक्ष संबंध: भारतीय न्यायालयों ने हमेशा संदर्भ-आधारित परीक्षण पर जोर दिया है। इसका एक प्रमुख उदाहरण है केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962), जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने देशद्रोह कानून को केवल उन्हीं मामलों में वैध ठहराया जहां शब्दों में “सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति या मंशा” हो या वे हिंसा के लिए उकसाते हों। केवल अपमानजनक या आलोचनात्मक अभिव्यक्ति को अपराध नहीं माना जा सकता। आधुनिक न्यायिक निर्णय भी इसी सिद्धांत को दोहराते हैं: किसी भाषण को दंडित करने के लिए राज्य को यह साबित करना होता है कि उस अभिव्यक्ति में या तो अवैध कृत्य करवाने की स्पष्ट मंशा थी या वह तत्काल और प्रत्यक्ष रूप से कानून तोड़ने की प्रवृत्ति रखता था - सिर्फ अप्रिय या उत्तेजक शब्दों के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह कठोर मानदंड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तीव्र राजनीतिक अभिव्यक्ति की रक्षा करता है, जबकि वास्तव में खतरनाक बयान को दंडित करने की गुंजाइश भी देता है।
कानूनी प्रावधानों को वास्तविक घटनाओं पर लागू करना : क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीमा लांघी?
यही वह महत्वपूर्ण और असहज प्रश्न है। आमतौर पर न्यायालय ताकतवर लोगों के राजनीतिक भाषण पर दो-चरणीय विश्लेषण लागू करते हैं:
● क्या भाषण की सामग्री में ऐसे तत्व हैं जो कानूनन अपराध की श्रेणी में आते हैं?
मुख्यमंत्री का भाषण केवल शासन संबंधी सामान्य बयानबाजी तक सीमित नहीं था। उन्होंने एक विशेष मौलाना और उनके समर्थकों को निशाना बनाया, जिससे परोक्ष रूप से एक पूरे धार्मिक समुदाय पर सामूहिक दोषारोपण का संकेत गया। “डेंटिंग-पेंटिंग” या “बरेली जैसी पिटाई” जैसे दंड और अपमान से जुड़े शब्द केवल आकस्मिक मेटाफर नहीं थे-इसने एक ऐसी दृश्य और ऐतिहासिक शैली को पुनर्जीवित किया जो राज्य की दमनकारी कार्रवाइयों से जुड़ी रही है। उत्तर प्रदेश की हालिया राजनीतिक शब्दावली में ये शब्द गहराई से जुड़े हैं - विशेष रूप से ध्वस्तीकरण अभियानों, पुलिस की पिटाई और ऐसी कार्रवाइयों के प्रतीक के रूप में जो मुस्लिम बस्तियों को असमान रूप से प्रभावित करती रही हैं।
इसके अलावा, यह कहना कि “आने वाली पीढ़ियों को सबक सिखाया जाएगा”, सामूहिक प्रतिशोध की एक स्पष्ट चेतावनी है, जो मौजूदा आरोपियों से आगे बढ़कर पूरे समुदाय को समय की धारा में साजा देने की मंशा को दर्शाती है। ऐसी भाषा मुसलमानों को कानून के अधीन नागरिक के रूप में नहीं, बल्कि एक स्थायी विरोधी वर्ग के रूप में प्रस्तुत करती है - एक ऐसा ‘पराया’ जिसके खिलाफ उदाहरण स्वरूप बल प्रयोग को न्यायसंगत ठहराया जा सके।
भारतीय दंड संहिता की धारा 153A (अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 196) और धारा 295A (अब बीएनएस की धारा 298) के तहत, किसी भाषण को आपराधिक ठहराने की कसौटी केवल खुले उकसावे पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह भी देखना होता है कि क्या वह भाषण नफरत को बढ़ावा देता है, किसी समुदाय को निशाना बनाता है, या सार्वजनिक शांति को भंग करने की संभावना पैदा करता है।
उत्तर प्रदेश में हाल ही की पुलिस कार्रवाइयों - जैसे मुस्लिम स्वामित्व वाली संपत्तियों का तोड़फोड़, हिरासत में हिंसक कार्रवाई और पक्षपातपूर्ण प्राथमिकी दर्ज करना - के संदर्भ में देखें तो मुख्यमंत्री के शब्दों को राज्य की भेदभावपूर्ण नीतियों के समर्थन और प्रोत्साहन के रूप में तर्कसंगत रूप से समझा जा सकता है।
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या, जैसे अमिश देवगन बनाम भारत संघ (2020) जैसे मामलों में, स्पष्ट करती है कि जब प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा ऐसे बयान दिए जाते हैं जो नफरत फैलाने की क्षमता रखते हैं, तो उकसावे की संभावना को केवल अलग से नहीं, बल्कि संदर्भ के अनुसार आंका जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से, योगी आदित्यनाथ के बयान प्रशासकीय दावे से आगे बढ़कर ऐसे भाषण बन जाते हैं जो भेदभाव को वैधता देते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं।
संक्षेप में, भले ही भाषण में सीधे हिंसा का आह्वान न हो, लेकिन यह एक ‘डॉग-व्हिसल’ (संकेतात्मक) भूमिका निभाता है: यह राज्य-समर्थित नफरत को सामान्य बनाता है और लक्षित धार्मिक समूह के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई की अनुमति का संकेत देता है। कानूनी दृष्टि से, यह भाषण आईपीसी की धाराओं 153A, 295A और 505(2) के तहत प्रारंभिक जांच के लिए उपयुक्त माना जा सकता है, विशेषकर वक्ता की संवैधानिक स्थिति और उसके बाद हुई हिंसा के प्रमाणित स्वरूप को देखते हुए।
● भाषण के बाद क्या बदला? (राज्य की कार्रवाई और न्यायसंगत सीमाएं)
संविधानिक मुद्दे केवल बोले गए शब्दों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उससे आगे की कार्रवाई में निहित होते हैं। जब मुख्यमंत्री की सार्वजनिक भाषा के तुरंत बाद प्रशासनिक कदम उठाए जाते हैं - बुलडोज़र चलाए जाते हैं, रातोंरात एफआईआर की संख्या बढ़ जाती है, और प्रभावित जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है - तब मामला केवल भाषण का नहीं, बल्कि भाषण द्वारा प्रेरित राज्य की शक्ति का होता है।
योगी आदित्यनाथ के भाषण के तुरंत बाद, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नगरपालिका और पुलिस प्रशासन ने अभियान चलाए: मुस्लिम युवाओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी, “अतिक्रमण” बताकर संपत्तियों का ध्वस्तीकरण और बड़े पैमाने पर इंटरनेट सेवा का निलंबन किया गया। ये केवल सामान्य कानून-व्यवस्था की कार्रवाई नहीं बल्कि बिना उचित नोटिस, सुनवाई या न्यायिक निरीक्षण के की गई बदले की एक योजनाबद्ध कार्रवाई थी।
न्यायालयों ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि कार्यपालिका की कार्रवाई उचित प्रक्रिया (due process) का विकल्प नहीं हो सकता। "बुलडोजर न्याय" (bulldozer justice) से संबंधित टिप्पणियों में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी आरोप के जवाब में यदि बिना नोटिस, जवाब देने का अवसर और नगर निगम कानूनों के पालन के बिना तुरंत तोड़फोड़ की जाती है, तो वह असंवैधानिक है (जमीयत उलमा-ए-हिंद बनाम उत्तर दिल्ली नगर निगम, 2022)। कानून एक स्पष्ट सीमा खींचता है कि शहरी नियोजन (urban planning) को दंडात्मक नाटक (penal theatre) के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं देखी गई - उग्र भाषण के तुरंत बाद कठोर कार्रवाई - वह यह संकेत देती है कि इसे कानून-व्यवस्था लागू करने के बजाय प्रतिशोध के इरादे से अंजाम दिया गया, जिसे कानून का अमल बताकर पेश किया गया।
शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ (2022) का सिद्धांत भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो पुलिस पर एक सकारात्मक दायित्व डाला गया है, उन्हें अभद्र भाषा के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, चाहे वक्ता का राजनीतिक कद कुछ भी हो। इस फैसले में इस बात पर जोर दिया गया है कि निष्क्रियता मौन सहमति के बराबर है और चुनिंदा कार्रवाई भेदभाव को और गहरा करता है। इस मामले में, कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कथित प्रदर्शनकारियों का तत्काल पीछा किया, लेकिन आईपीसी की धारा 153ए, 295ए और 505(2) के तहत स्पष्ट वैधानिक आधारों के बावजूद, मुख्यमंत्री की भड़काऊ टिप्पणियों पर कार्रवाई करने में विफल रहीं।
संवैधानिक अनुपातिकता के सिद्धांत (doctrine of proportionality) के अनुसार, प्रशासनिक कार्रवाइयां तभी वैध मानी जाती हैं जब उनका किसी वैध उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध हो, वे न्यूनतम प्रतिबंधात्मक उपाय अपनाएं, और उनका प्रभाव भेदभावपूर्ण न हो। परंतु मुख्यमंत्री के भाषण के बाद जो कार्रवाइयां हुईं-जैसे कि मुस्लिम-बहुल इलाकों में तोड़फोड़, विशेष समुदाय के युवाओं पर पुलिस छापे और आत्मघोषित ‘रक्षक’ समूहों की जवाबदेही की पूरी तरह अनुपस्थिति-वे इन संवैधानिक मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन लगती हैं। यह सब एक संतुलित और लक्षित कानून-प्रवर्तन के बजाय एक सामूहिक दंड की तैयार रणनीति की ओर संकेत करता है जो न केवल न्याय के सिद्धांतों का हनन है बल्कि लोकतंत्र और समानता के मूल मूल्यों के भी विपरीत है।
जैसा कि कई विश्लेषकों ने उल्लेख किया है, जब कार्यपालिका की भाषा एक संकेत के रूप में कार्य करती है और नौकरशाही तंत्र उस संकेत के जवाब में दमनात्मक अतिक्रमण करता है, तब राजनीतिक बयानबाजी और राज्य की वैधानिक स्वीकृति के बीच की सीमा ध्वस्त हो जाती है। ऐसे में राज्य एक निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका छोड़कर अपने ही नैतिक तमाशे का अभिनेता बन जाता है, जहां कानून का पालन कराने की बजाय वह भय के जरिए अनुशासन और प्रतिरोध का दमन प्रदर्शित करता है।
योगी आदित्यनाथ के भाषण को अगर अकेले राजनीतिक अभिव्यक्ति के तौर पर देखा जाए तो वह सुरक्षित ठहराया जा सकता है, लेकिन इसके बाद हुई घटनाओं की तेजी -जैसे तत्काल गिरफ्तारियां, व्यापक स्तर पर एफआईआर दर्ज करना और दंड स्वरूप संपत्तियों की तोड़फोड़-स्पष्ट करती है कि राज्य की ताकत न्याय के बजाय एक सशक्त राजनीतिक संदेश देने के लिए इस्तेमाल की गई। यह मामला संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत गंभीर संवैधानिक सवाल खड़ा करता है, हालांकि भाषण के सीधे आपराधिक दायित्व को साबित करना कानूनी रूप से जटिल है।
वास्तविक स्थिति: कठोर कार्रवाई और उसके समुदाय पर प्रभाव के सबूत
बरेली हिंसा के बाद की घटनाएं केवल पारंपरिक कानून-व्यवस्था के दायरे में नहीं रुकतीं, बल्कि यह एक बहु-स्तरीय दबावकारी राज्य शक्ति के प्रयोग का दर्शाती हैं। यह शक्ति मुख्यमंत्री के भाषण के तुरंत बाद सक्रिय हुई और औपचारिक तथा अनौपचारिक दंड के माध्यम से निरंतर जारी रखी गई।
● सामूहिक गिरफ्तारियां और बड़े पैमाने पर एफआईआर: बरेली और आस-पास के जिलों में तुरंत बाद पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई। खबरों में बताया गया कि कुछ ही घंटों में दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया और सैकड़ों-कभी-कभी तो हजारों-लोगों के नाम एफआईआर में शामिल किए गए। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, कई थानों में लगभग 2,000 लोगों के नाम दर्ज हुए, हालांकि अलग-अलग स्रोतों में संख्या में फर्क था। इन एफआईआर में अक्सर बड़े-बड़े और आम आरोप थे, जिससे ये सवाल उठते हैं कि क्या पुलिस सबको एक साथ दोषी ठहरा रही है और रोकथाम के नाम पर लोगों को डराने-धमकाने के लिए पकड़ रही है, ना कि सही तरीके से जांच कर रही है।
● संपत्तियों की सीलिंग और तोड़फोड़: नगरपालिका और विकास प्राधिकरणों ने आरोपियों से जुड़ी बताई गई संपत्तियों-जैसे कि एक बैंक्वेट हॉल और अन्य व्यावसायिक इमारतों-के खिलाफ तेजी से तोड़फोड़ और सीलिंग अभियान चलाए। परिवारों ने शिकायत की कि उन्हें कोई पूर्व सूचना या सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, जिसके कारण उन्होंने उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग से शिकायत की। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, ये कदम राज्य की बुलडोजर से जुड़ी दंडात्मक कार्रवाइयों की हालिया प्रवृत्ति की पुनरावृत्ति हैं, जिन्हें मानवाधिकार समूह ‘दिखावटी बदला’ मानते हुए आलोचना करते रहे हैं जो नियमों के पालन की बजाय दबदबे का संदेश देने के लिए किए जाते हैं। सांप्रदायिक घटनाओं के तुरंत बाद इस तरह की तोड़फोड़ यह संकेत देती है कि अपराधी उत्तरदायित्व को संपत्ति के स्वामित्व और समुदाय की पहचान से जोड़कर एक जानबूझकर मिलान किया जा रहा है।
● प्रशासनिक और नियामक जवाबी कार्रवाई: पुलिस की कार्रवाई के साथ-साथ प्रशासन ने भी कई “पूरक दंडात्मक कार्रवाई” किए-जिनमें बिजली चोरी के नोटिस, आय वसूली के दावे और प्रदर्शन के केंद्र में रहे मौलवी से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ नियामक प्रतिबंध शामिल थे। ये अर्ध-नागरिक दंड प्रभावित परिवारों पर आर्थिक और मानसिक बोझ को और बढ़ा गए। ये सभी कदम अलग-अलग तो कानूनी हो सकते हैं, लेकिन एक साथ मिलकर ये कार्रवाई अनुपातहीन और बोझिल दंड के रूप में दिखती है, जो नौकरशाही उपकरणों के जरिए लगातार दंडित करने की रणनीति का हिस्सा लगती है।
● इंटरनेट बंद करना: अफवाहें फैलने और लोगों के इकट्ठा होने को रोकने के लिए अधिकारियों ने बरेली जिले में 48 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और मैसेजिंग सेवाएं बंद कर दीं। द इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, यह हाल के कई उदाहरणों में से एक है जहां सांप्रदायिक तनाव के समय इंटरनेट बंद करना प्रशासन की आम प्रतिक्रिया बन गया है। हालांकि ये कदम सावधानी के नाम पर लिए जाते हैं, पर अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) के फैसले के अनुसार, इस तरह के प्रतिबंध केवल सीमित समय के लिए और विशेष रूप से आवश्यक होने पर ही लगाना चाहिए, साथ ही समय-समय पर समीक्षा भी होनी चाहिए।
● सामाजिक प्रभाव और बहिष्कार की प्रवृत्तियां: घटनाओं के बाद समाज में भी गहरा असर देखने को मिला। सिविल सोसायटी और मीडिया, जैसे कि LiveMint, ने रिपोर्ट किया कि उस घटना के बाद सामाजिक सीमाओं में स्पष्ट सख्ती आ गई। बताया गया कि मुस्लिम समुदाय पर गरबा और अन्य सार्वजनिक उत्सवों में हिस्सा न लेने का दबाव डाला गया और कुछ जगहों पर हिन्दुत्ववादी समूहों ने सांस्कृतिक आयोजनों में मुस्लिमों की मौजूदगी पर निगरानी रखने या उन्हें बाहर करने की कोशिश की। भले ही इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो, लेकिन ये घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे प्रशासनिक बयान और कड़ी कार्रवाई मिलकर समुदायों के बीच बहिष्कार को वैधता देते हैं और रोजमर्रा के सामाजिक संबंधों में राज्य समर्थित पक्षपात को गहराते हैं।
कुल मिलाकर देखें तो ये घटनाएं सिर्फ कानून-व्यवस्था का एक अलगाव नहीं बल्कि एक सुनियोजित क्रम दर्शाती हैं: बयानबाजी, दमन, और सामाजिक दंड। भाषण, कार्रवाई, प्रदर्शन और बहिष्कार का यह चक्र शासन का एक विशेष मॉडल बन जाता है-जहां प्रशासनिक कदम राजनीतिक मंचन बन जाता है और दंड सार्वजनिक संदेश का एक जरिया।
सख्त बयानबाजी की राजनीति: भाषण से सत्ता तक का सफर
चाहे यह सोची-समझी रणनीति हो या अनजाने में हुआ असर, योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं के कड़े सार्वजनिक बयान राजनीतिक हाशिए पर काम करने वाले बहुलवादी या विजिलेंट समूहों के लिए तीन बड़े फायदे लेकर आते हैं। ये भाषण को कार्रवाई में बयानबाजी को वैधता में और जबरदस्ती को तमाशे में बदल देते हैं।
1. विजिलेंट पुलिसिंग को अप्रत्यक्ष मंजूरी: जब सरकार का बड़ा अधिकारी खुलेआम सख्त कार्रवाई का वादा करता है और बदले की बातें करता है-जैसे “डेंटिंग और पेंटिंग करना” या “हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं”—तो ये बात सिर्फ सरकारी दफ्तर तक सीमित नहीं रहती। इससे स्थानीय लोग, विजिलेंट ग्रुप और अपने जैसे सोच वाले इसे कार्रवाई का संकेत समझ लेते हैं। ये लोग इसे ‘नागरिक पुलिसिंग’ या धर्म और देश की रक्षा के नाम पर लोगों को डराने-धमकाने का सही ठहराव मान लेते हैं। सिविल सोसायटी की रिपोर्ट्स में भी दिखता है कि ऐसे बयान आने के बाद हिंदुत्ववादी संगठन मुस्लिमों की गरबा या जुलूस जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा देते हैं। इस तरह की बातों से विजिलेंट बनने की हिम्मत बढ़ती है और लोग सोचते हैं कि उन्हें सत्ता की छूट मिली है।
2. नैरेटिव पर नियंत्रण और उलटफेर: नेता के बयान घटनाओं की नैतिक कड़ी को भी बदल देते हैं। जैसे “I Love Muhammad” जैसे भावनात्मक या धार्मिक कामों को “उकसावे” के तौर पर पेश किया जाता है, जिससे राज्य खुद को व्यवस्था का निष्पक्ष रक्षक दिखाता है और प्रदर्शनकारियों को समस्या पैदा करने वाला बताता है। इस तरह की कहानी उलटफेर से किसी समुदाय के धर्म का प्रदर्शन कानून-व्यवस्था की समस्या बन जाता है, जिससे प्रशासन को बिना ज्यादा विरोध के दमन करने का मौका मिल जाता है।
जैसा कि The Wire और अन्य आलोचनात्मक मीडिया ने रिपोर्ट किया है, मीडिया की फ्रेमिंग बहुत अहम भूमिका निभाती है। वे चैनल जो “दंगों” और “अनुशासन” को प्रमुखता देते हैं, वे सरकार की पसंदीदा नैरेटिव को बढ़ावा देते हैं, जबकि जो लोग उचित प्रक्रिया या अत्यधिक सख्ती पर सवाल उठाते हैं, उन्हें “अव्यवस्था के प्रति नरम” कहकर किनारे कर दिया जाता है। इसका नतीजा एक ऐसा चक्र बनना है जहां राजनीतिक बयान और मीडिया की रिपोर्टिंग मिलकर सरकार की वैधता को मजबूत करते हैं।
3. चुनावी संकेत और समर्थन जुटाने की रणनीति: तत्काल प्रशासनिक इस्तेमाल से परे, कड़े बयानों का काम राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करना होता है जो खासतौर पर एक राजनीतिक वर्ग को ध्यान में रखकर किया जाता है। बुलडोजर की तस्वीरें, तेज गिरफ्तारियां और सामूहिक दंड एक निर्णायक शासन का तमाशा बन जाते हैं, जो नियंत्रण और दबदबे का संदेश देते हैं। साउथ एशियन पोपुलिज्म के शोधकर्ताओं ने बताया है कि ये सख्त कार्रवाई “सजात्मक लोकलुभावनवाद” कहलाती है, जो बहुसंख्यकों को भरोसा दिलाने के लिए न्याय प्रणाली को एक भावनात्मक साधन बना देती है। हर कार्रवाई राजनीतिक पहचान को मजबूत करने का हिस्सा बन जाती है, जिससे कानून-व्यवस्था और चुनावी प्रदर्शन के बीच की हदें मिट जाती हैं।
कुल मिलाकर देखें तो ये तीनों पहलू-बयानबाजी, मीडिया और कार्रवाई-कैसे मिलकर बहुसंख्यक सत्ता का एक पूरा तंत्र बनाते हैं। इस मॉडल में दंड सिर्फ लागू नहीं होता, बल्कि उसे प्रदर्शन के तौर पर दिखाया जाता है, टीवी पर दिखाया जाता है और चुनावों में वोट भी मिलता है।
जवाबदेही के अंतराल और कानूनी उपाय
बरेली की घटना के बाद सिर्फ टिप्पणी करना काफी नहीं है बल्कि जवाबदेही भी जरूरी है। जब सरकारी बयान, प्रशासनिक कार्रवाई और मीडिया प्रचार मिलकर दबाव वाली कार्रवाई करते हैं, तो संविधान व्यवस्था को उचित सुधार सुनिश्चित करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की मान्यताओं और मानवाधिकार प्रथाओं के आधार पर निम्नलिखित कानूनी और संस्थागत प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं:
1. मुख्यमंत्री के भाषण पर शाहीन अब्दुल्ला निर्देशों के तहत स्वतः संज्ञान: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस पर नफरत भरे भाषणों के मामलों में स्वतः FIR दर्ज करने की निरंतर जिम्मेदारी है, चाहे वक्ता किसी भी राजनीतिक पद पर हो। उच्च पदस्थ अधिकारियों के संभावित उकसावे वाले बयान पर कार्रवाई न करना कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना माना जाएगा। अगर अभी तक कोई जांच शुरू नहीं हुई है, तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अनुपालन के लिए आवेदन करना कानूनी रूप से सही होगा।
2. तोड़-फोड़ और सीलिंग अभियानों की मनमानी और अनुचित कठोरता पर न्यायिक समीक्षा: सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में “बुलडोजर न्याय” पर दिए अपने निर्णय में साफ कहा है कि तत्काल सजा के तौर पर की गई तोड़-फोड़ उचित प्रक्रिया का उल्लंघन है। प्रभावित हर व्यक्ति को पहले से सूचना मिलने, अपनी बात रखने और स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा का अधिकार होता है, इससे पहले कि उनकी संपत्ति पर कोई कार्रवाई हो। जब नगरपालिका या डेवलपमेंट अफसर सांप्रदायिक घटनाओं के तुरंत बाद ऐसी कार्रवाइयां करते हैं, तो उन तोड़-फोड़ को वैध शहरी नियमन की बजाय दंडात्मक कार्रवाई के रूप में देखकर न्यायालयीय जांच की जरूरत होती है।
3. मानवाधिकार शिकायतें और जनहित याचिकाएं जो पूरे घटनाक्रम को दर्ज करें: कानपुर में दर्ज एफआईआर से लेकर बरेली में हुई झड़पों, मुख्यमंत्री के भाषणों और प्रशासनिक दमन तक की पूरी टाइमलाइन अपने आप में राज्य की मनमानी और चयनात्मक कार्रवाई का अहम सबूत बनती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), राज्य मानवाधिकार आयोग या संबंधित हाईकोर्ट में की गई शिकायतों और याचिकाओं के जरिए स्वतंत्र जांच, पीड़ितों को मुआवजा और रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की जा सकती है। पहले के उदाहरण दिखाते हैं कि इस तरह की याचिकाओं ने न सिर्फ राज्य को जवाब देने के लिए मजबूर किया है बल्कि कई बार दमनात्मक कार्रवाई पर रोक भी लगवाई है।
4. मीडिया की जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग: चूंकि टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दंडात्मक बयानों को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए पारदर्शिता के उपाय बेहद जरूरी हैं। ब्रॉडकास्ट चैनलों और सोशल मीडिया कंपनियों को चाहिए कि वे अपने सभी फुटेज, थंबनेल और मेटाडेटा को सुरक्षित रखें ताकि भविष्य में जांच की जा सके। जिन मीडिया आउटलेट्स ने सनसनीखेज प्रोमो या भ्रामक हेडलाइन का इस्तेमाल किया है, उनसे NBDSA (न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी) के तहत स्पष्टीकरण या सुधार जारी करने की मांग की जा सकती है। साथ ही, पुलिस और स्थानीय प्रशासन को यह सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए कि सामूहिक FIR, तोड़फोड़ आदेश और इंटरनेट बंदी का कानूनी आधार क्या था। इस तरह की पारदर्शिता, बिना रोक-टोक के हो रही कार्यपालिका की सख्ती पर लगाम लगाने की दिशा में पहला कदम बन सकती है।
निष्कर्ष - कानूनी जोखिम और लोकतांत्रिक कीमत
बरेली की "I Love Muhammad" विवाद और उसके बाद की घटनाएं आज के भारत में सत्ता और अभिव्यक्ति के टकराव के एक बेहद अहम मोड़ पर खड़ी हैं। जो शुरुआत में एक अभिव्यक्तिपूर्ण क़दम था -एक नारा, एक बैनर, या धार्मिक पहचान की पुष्टि -वह राजनीतिक और प्रशासनिक ताकत के दबाव में जल्दी ही "उकसावे" की नैरेटिव बना दी गई और फिर उसे राज्य की दंडात्मक कार्रवाइयों की एक कड़ी में बदल दिया गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बयानबाजी महज़ चेतावनी तक सीमित नहीं रही -बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने राज्य की सख्त कार्रवाइयों के लिए एक तरह का कानूनी और नैतिक आधार तैयार किया। ऐसे कदम -जैसा कि विश्वसनीय रिपोर्टों में सामने आया -प्रक्रियात्मक नियमों को पीछे छोड़ते हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को खतरे में डालते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी को दबाते हैं और आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन को अस्त-व्यस्त कर देते हैं। हालांकि ऐसे मामलों में कानूनी राहत पाना मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। हमारे संविधान की व्यवस्था, विधिक प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट की पहले की गई टिप्पणियां ऐसे अतिक्रमणों को चुनौती देने का स्पष्ट आधार प्रदान करती हैं।
इस लिहाज से बरेली की घटना सिर्फ एक स्थानीय मामला नहीं है बल्कि यह एक पड़ताल की घड़ी है। अगर न्याय व्यवस्था, सिविल सोसायटी और मीडिया मिलकर भाषण और उसके बाद की कार्रवाई की गंभीर जांच करने में असफल रहते हैं, तो जो उदाहरण बनता है वह बेहद खतरनाक होगा: ऐसा राजनीतिक भाषण जो पहचान, आस्था, दंडात्मक वादा और तमाशे को घालमेल कर देता है, तो वह हाशिए पर डालने का एक लाइसेंस बन जाता है। लोकतंत्र ऐसे मौकों पर तभी टिक सकता है जब “कानून-व्यवस्था” और राज्य की मनमानी कार्रवाई के बीच की वह बारीक व अदृश्य रेखा भी उतनी ही गंभीरता से जांची जाए जितनी हम किसी खुले विरोध प्रदर्शन की करते हैं।
References
https://www.livelaw.in/top-stories/take-suo-motu-action-against-hate-spe...
https://www.indiatoday.in/india/story/what-is-i-love-muhammad-row-and-wh...
https://timesofindia.indiatimes.com/city/meerut/bareilly-cleric-among-8-...
https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/i-love-muhammad-row-up-...
https://economictimes.indiatimes.com/news/india/internet-suspended-in-ba...
https://www.livemint.com/news/india/yogi-adityanath-warns-i-love-mohamma...
https://thepolisproject.com/research/sc-verdict-demolitions-statecraft/
https://thewire.in/politics/i-love-muhammad-banner-controversy-how-routi...
https://www.scobserver.in/journal/bulldozer-demolitions-remind-of-a-lawl...
https://timesofindia.indiatimes.com/city/meerut/i-love-muhammad-row-plea...
https://timesofindia.indiatimes.com/city/bareilly/i-love-muhammad-row-rs...
https://theloop.ecpr.eu/bulldozer-justice-punitive-populism-in-india/
https://indianexpress.com/article/cities/lucknow/i-love-muhammad-row-cle...
https://theprint.in/politics/cleric-who-once-said-modi-should-learn-from...
https://kmsnews.org/kms/2025/09/20/muslims-protest-across-india-against-...
https://sabrangindia.in/register-prosecute-hate-speech-offences-promptly...
https://sabrangindia.in/hate-crime-hate-speech-scs-scrutiny-continue
https://sabrangindia.in/free-speech-even-in-bad-taste-is-protected-if-no...
https://www.toaep.org/pbs-pdf/138-lokur-damojipurapu
https://timesofindia.indiatimes.com/india/tension-in-bareilly-drones-are...
https://timesofindia.indiatimes.com/india/one-can-say-i-love-modi-but-no...
https://timesofindia.indiatimes.com/india/i-love-mohammad-march-violence...
https://cjp.org.in/bns-2023-does-nothing-to-bring-in-a-nuanced-effective...
https://cjp.org.in/cjp-files-complaints-against-the-hate-speeches-delive...
https://cjp.org.in/the-sentinel-and-the-shift-free-speech-in-the-supreme...
https://thelogicalindian.com/chedhoge-to-chodhenge-nahi-yogi-adityanaths...
https://www.ndtv.com/india-news/internet-cut-for-48-hours-in-ups-bareill...
https://article-14.com/post/govt-whataboutery-inaction-why-hate-speech-p...

सितंबर 2025 में शुरू हुए “आई लव मुहम्मद” विवाद के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार-बार सार्वजनिक बयान दिए। विशेष रूप से 28 सितंबर को अपने बयान में सार्वजनिक व्यवस्था को “परेशान” करने वालों के लिए सख्त, स्पष्ट सजा का वादा करते हुए कहा कि, “छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं”, “पीढ़ियां याद रखेंगी”, “गजवा-ए-हिंद सफल नहीं होगा और इसके बजाय उसे नरक का टिकट दिया जाएगा” और “डेंटिंग और पेंटिंग की जानी चाहिए” जैसी बातें की।
हालांकि यह भाषण बरेली विरोध प्रदर्शन पर स्थानीय कार्यकारी प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन इसका प्रचार और प्रसार मुख्यतः राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया, खासकर टाइम्स नाउ नवभारत, जी न्यूज़ हिंदी और न्यूज़18 हिंदी जैसे हिंदी टेलीविजन चैनलों के माध्यम से हुआ, जिन्होंने मुख्यमंत्री के शब्दों को विरोध प्रदर्शनों, पुलिस कार्रवाई और संपत्ति तोड़फोड़ के तस्वीरों के साथ जोड़ा। सोशल मीडिया पर छोटे-छोटे क्लिप खूब वायरल हुए, जिससे एक फीडबैक लूप बना जिसने बयानबाजी और राज्य की प्रतिक्रिया, दोनों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया।
मीडिया द्वारा किए गए इस प्रचार ने स्थानीय कानून-व्यवस्था के मुद्दे को दंडात्मक शासन के राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देने वाले तमाशे में बदल दिया, जिसमें बलपूर्वक लागू करना और एक धार्मिक समुदाय को निशाना बनाना सामान्य बात हो गई। प्रचार के समय और पैमाने का राजनीतिक महत्व भी हो सकता है, खासकर आगामी बिहार चुनावों के संदर्भ में, क्योंकि हिंदी भाषी मीडिया नेटवर्क ने यह तय किया कि मुख्यमंत्री की बयानबाजी व्यापक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दर्शकों तक पहुंचे।
कुछ ही दिनों में बरेली में सरकारी कार्रवाई तेज हो गई: बड़े पैमाने पर गिरफ़्तारियां, संपत्तियां सील करने और तोड़फोड़ की कार्रवाई, 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद, आपराधिक एफआईआर (कुछ मामलों में सैकड़ों या हजारों तक) और बरेली में विरोध प्रदर्शन का आह्वान करने वाले मौलवी के सहयोगियों के खिलाफ प्रशासनिक नोटिस जारी किए गए। 'विरोध फिर मुख्यमंत्री की बयानबाजी फिर सख्त कार्रवाई' का यह क्रम तीन जुड़े हुए सवाल खड़े करता है जिनकी इस लेख के बाकी हिस्से में गहराई से पड़ताल की गई है:
● क्या मुख्यमंत्री के भाषण ने उकसावे या गैरकानूनी भेदभाव जैसी कानूनी सीमाओं को पार किया?
● क्या राज्य की प्रतिक्रिया में उचित प्रक्रिया और सर्वोच्च न्यायालय के अपने सुरक्षा उपायों (नफरत फैलाने वाले भाषण की स्वतः जांच करने के ड्यूटी सहित) का पालन किया गया?
● उस राजनीतिक बयानबाजी के सामाजिक, कानूनी और मीडिया पर क्या मापा जा सकने वाला परिणाम हैं?
जो कुछ हुआ उसकी टाइमलाइन
प्रारंभिक घटना (4–9 सितंबर, 2025): यह विवाद 4 सितंबर से शुरू हुआ, जब कानपुर के कुछ इलाकों (सैयद नगर/रावतपुर) में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी की जुलूस के दौरान “I Love Muhammad” लिखा हुआ बोर्ड या बैनर देखा गया। कुछ हिंदुत्ववादी समूहों ने इसे “परंपरा से भटकाव” बताया और स्थानीय स्तर पर इसका विरोध किया। इस विवाद के बाद पुलिस ने 9 सितंबर को 24 लोगों (9 नामजद और 15 अज्ञात) के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द भंग करने के आरोप में FIR दर्ज की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, शिकायत का मुख्य आधार यह था कि टेंट और बैनर को राम नवमी के जुलूसों के मार्ग के नजदीक एक आम सड़क पर स्थानांतरित किया गया था। यह मामूली बदलाव जल्द ही खबरों और सोशल मीडिया के जरिए दूसरे जिलों तक फैल गया।
विवाद में वृद्धि और बरेली प्रदर्शन (26–27 सितंबर, 2025): 26 सितंबर को बरेली में एक सार्वजनिक सभा हुई, जिसे “I Love Muhammad” अभियान के समर्थन में बुलाया गया था और जिसका संबंध धर्मगुरु तौकीर रजा खान से था। इस सभा के बाद शुक्रवार की नमाज के बाद पुलिस के साथ झड़पें हुईं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पत्थरबाजी की घटनाएं भी हुईं, जिसमें कई अधिकारी घायल हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों का कहना है कि यह प्रदर्शन बिना अनुमति के किया गया था। पुलिस ने यह भी कहा कि यह सभा सोशल मीडिया समूहों के माध्यम से पूर्व योजना के संकेत देती थी। इसके बाद कई FIR दर्ज की गईं और दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया गया। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक दर्जनों लोग हिरासत में हैं और सैकड़ों के खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं - जबकि कुछ मीडिया सूत्रों के अनुसार, कई थानों में FIR की संख्या हजारों तक पहुंच गई है। झड़पों के तुरंत बाद धर्मगुरु और उनके कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया (28 सितंबर, 2025): ‘विकसित यूपी’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग “धर्म के नाम पर तोड़फोड़ करते हैं… पुलिस पर हमला करते हैं… उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे… छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं और छोड़ेंगे नहीं तो फिर छूटोगे भी नहीं।” उन्होंने कहा कि “डेंटिंग और पेंटिंग तो करनी ही पड़ेगी” और इस प्रतिक्रिया को त्योहारों और सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा के लिए जरूरी बताया। ये बयान नेशनल न्यूज आउटलेट में उसी दिन और अगले दिन और उसके बाद भी व्यापक रूप से प्रकाशित किए गए।




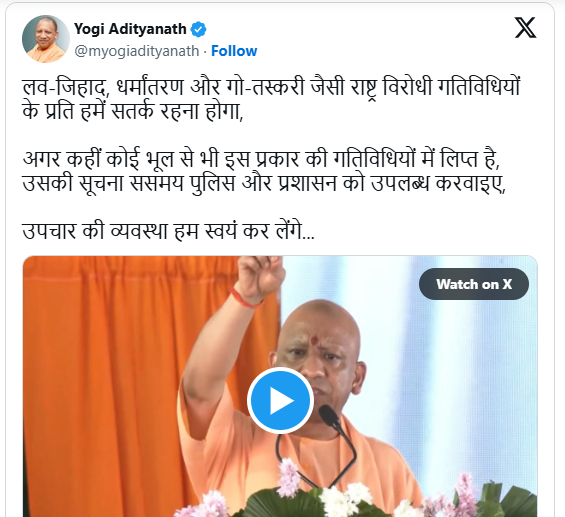
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा दिए गए भाषण:
2025 में हिंसा और भाषणों के बाद जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गईं और FIR दर्ज की गईं। आरोपी व्यक्तियों से जुड़े संपत्तियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा सील किया गया या तोड़ दिया गया, जिसमें एक बैंक्वेट हॉल और अन्य संरचनाएं भी शामिल थीं, जिनका कथित रूप से गिरफ्तार लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। प्रशासन ने तौकीर रजा खान के सहयोगियों के खिलाफ विद्युत चोरी जैसे नोटिस भी जारी किए। इकॉनोमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, बरेली जिले में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट और SMS सेवाएं 48 घंटे के लिए निलंबित कर दी गईं। कई मानवाधिकार और कानूनी कार्यकर्ताओं ने पहले ही बिना पूर्व सूचना के संपत्तियों के ध्वस्त किए जाने और संभावित सामूहिक दंड के खिलाफ याचिकाएं और शिकायतें दर्ज करवाई हैं। राजनीतिक पार्टियां और नागरिक समाज के प्रतिनिधिमंडल शहर का दौरा करना शुरू कर चुके हैं। विपक्षी नेता जांच की मांग कर रहे हैं।
भाषण की मूल समस्या
1. निशाना बनाना और व्यक्तिगत संदर्भ: मुख्यमंत्री ने खास तौर पर एक धर्मगुरु तौकीर रजा खान और उनके द्वारा लोगों के बीच की गई बातों पर हमला किया, यह कहते हुए कि "मौलाना भूल गए हैं कि सत्ता किसके पास है" और "ऐसा बदला दिया जाएगा जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी।" किसी पहचाने जाने वाले नेता को निशाना बनाना और उसे तथा उनके समर्थकों को हिंसा से जोड़ना, भाषण को केवल सामान्य कानून-व्यवस्था की भाषा से कहीं आगे ले जाता है।
2. सजा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति को शाब्दिक रूप में लेना: "डेंटिंग और पेंटिंग" के बार-बार इस्तेमाल और "बुलडोजर" का उल्लेख, जो हाल के यूपी अभियानों में तोड़फोड़ के साथ जुड़े हैं, केवल प्रतीकात्मक नहीं हैं। वर्तमान यूपी के संदर्भ में यह एक संस्थागत इतिहास है - दंड के सार्वजनिक प्रदर्शन के रूप में एक राज्य का तमाशा, जिसके वास्तविक परिणाम होते हैं। इसलिए यह वाक्यांश नीतिगत संकेत और सार्वजनिक चेतावनी दोनों के रूप में पढ़ा जाता है।
3. समुदाय के प्रति शक्ति और रोकथाम का संदेश: हालांकि तत्काल कारण हिंसा थी, मुख्यमंत्री का वाक्य -“अगर तुम हमें परेशान करोगे, तो हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं” - विशेष रूप से एक विशिष्ट प्रकार की अभिव्यक्ति को रोकने के लिए था, जैसे कि “I Love Muhammad” पोस्टर दिखाना, जिसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं और कुछ नागरिक समाज के लोगों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माना और उसकी रक्षा की थी। इस तरह की बातों को अवैध ठहराना, नारे को बच्चों की मनमानी या अराजकता के रूप में दिखाना, साथ ही सामूहिक अनुशासन का वादा करना, इसके गंभीर परिणाम होते हैं।
वे तीन विशेषताएं - नाम लेना, सजा की सांकेतिक भाषा और सामान्यीकृत रोकथाम - ऐसी बातें हैं जो कानूनी और मानक विश्लेषण को बेहद जरूरी बनाती हैं।
मीडिया: किसने बढ़ावा दिया और किस प्रकार इस बढ़ावा ने कहानी को बदला
मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों को स्थानीय राजनीतिक प्रतिक्रिया से राष्ट्रीय स्तर पर एक शक्तिपूर्ण प्रदर्शन में बदलने में निर्णायक भूमिका निभाई। उनके भाषण के कुछ ही घंटों के भीतर, टेलीविजन और प्रिंट मीडिया दोनों ने उनके सबसे आक्रामक बयानों - “छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं” और “डेंटिंग और पेंटिंग तो करनी ही पड़ेगी” - को पहले पन्ने पर प्रमुखता से जगह दी, जिससे ये प्रतिशोध के धमकी वाले बयान वायरल हो गए।
राष्ट्रीय और क्षेत्रीय ब्रॉडकास्टर्स जैसे टाइम्स नाउ नवभारत, जी न्यूज़ हिंदी, और न्यूज18 हिंदी ने ऐसे न्यूज प्रसारित किए जिनमें मुख्यमंत्री के बयानों को प्रदर्शनों, लाठीचार्ज और संपत्तियों के ध्वस्तीकरण के तस्वीरों के साथ जोड़ा गया। यूट्यूब थंबनेल और स्क्रीन पर चलने वाले टिकर स्वयं राज्य की संदेशवाहक प्रक्रिया का हिस्सा बन गए - “मौलाना भूल गया कौन सरकार में है” या “बरेली में दंगा, सरकार की कठोर कार्रवाई” जैसे टेक्स्ट ने मुख्यमंत्री की चेतावनी को एक तमाशा और नारे के रूप में पेश किया।
मीडिया की इस प्रस्तुति का दोहरा प्रभाव पड़ा। पहला, इसने मुख्यमंत्री की भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया, जिससे जो शुरूआत में एक स्थानीय सांप्रदायिक अशांति थी, वह पूरे राज्य में कानून-व्यवस्था की सफलता के रूप में पेश की गई। दूसरा, उनके बयानों का बार-बार प्रसारण - अक्सर संदर्भ से अलग और पुलिस कार्रवाई के वीडियो के साथ - दंड और रोकथाम की भाषा को सामान्य कर दिया। यहां तक कि ऐसे प्लेटफॉर्म जिन्होंने भाषण को संपादकीय रूप से समर्थन नहीं दिया वे भी पुनरावृत्ति के जरिए इसके प्रसार में योगदान देते रहे।
कुछ मीडिया संस्थान जैसे द वायर और द इंडियन एक्सप्रेस ने एक विपरीत दृष्टिकोण पेश किया: विस्तृत टाइमलाइन, “ऑनलाइन टूलकिट” के बारे में पुलिस के दावों की जांच और प्रशासन के अत्यधिक बल प्रयोग की आलोचनात्मक समीक्षा की। लेकिन ये अपवाद थे जो प्रदर्शनकारी कानून-व्यवस्था कवरेज की भारी लहर में घिरे हुए थे। फ्रेमिंग में यह विभाजन - कानून-व्यवस्था की नैरेटिव और नागरिक स्वतंत्रता की जांच - दर्शाता है कि कैसे संपादकीय रुख सांप्रदायिक घटनाओं की नैतिकता को सीधे प्रभावित करता है।
इन चैनलों के शॉर्ट-फॉर्म वीडियो, जो यूट्यूब शॉर्ट्स और ट्विटर/एक्स रील्स के रूप में निकाले गए थे, सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर प्रसारित हुए। ये क्लिप - मुख्यमंत्री की चेतावनी को हिंसा और पुलिस तैनाती के तस्वीरों के साथ जोड़ा गया - एक फीडबैक लूप बनाते हैं: जितना ज्यादा यह तस्वीर वायरल होता गया, उतना ही प्रशासनिक कार्रवाईयों जैसे इंटरनेट बंद करना और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी होती गई। प्रभावी रूप से, मीडिया पारिस्थितिकी और राज्य की जबरदस्ती की मशीन एक-दूसरे को सशक्त बनाते रहे।
यह सब एक संवैधानिक सवाल भी उठाता है जो मध्यस्थ शासन से जुड़ा है। जब कार्यकारी भाषण, पत्रकारिता द्वारा प्रचार और प्रशासनिक दबाव एक साथ काम करते हैं तो राज्य के संदेश और स्वतंत्र रिपोर्टिंग के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। नतीजा केवल सूचना का प्रसार नहीं बल्कि एक “नियंत्रण का प्रदर्शन” बन जाता है, जहां निर्णायक शासन का दिखावा कानूनी प्रक्रिया के पालन की जगह ले लेता है।
टाइम्स नाउ नवभारत, जी न्यूज हिंदी, और न्यूज18 हिंदी के यूट्यूब थंबनेल्स का एक संग्रह यहां पर दिया गया है जो इसे बखूबी दर्शाता है -ऐसे शीर्षकों का एक मोंटाज जो न्यूज कवरेज और स्टोरी नैरेटिव के बीच की सीमा को धुंधला कर देता है और दंडात्मक कार्रवाई को राजनीतिक गुण के रूप में पेश करता है।
कानूनी दृष्टिकोण: कानून क्या कहता है और न्यायालयों ने सीमा कहां खींची है
यहां तीन परस्पर जुड़े कानूनी नियम महत्वपूर्ण हैं:
● “नफरत”/सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित भाषण के लिए कानूनी प्रावधान: भारत के दंड संहिता में ऐसे भाषणों को दंडनीय ठहराया गया है जो समूहों के बीच वैमनस्य या नफरत को बढ़ावा देते हैं (जैसे, IPC धारा 153A/धारा 198 बीएनएस), राष्ट्रीय एकता के खिलाफ आरोप लगाना (IPC धारा 153B/धारा 197 बीएनएस), धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य (IPC धारा 295A/धारा 298 बीएनएस), और ऐसे बयान जो आतंक या सार्वजनिक डर पैदा करने की संभावना रखते हों (IPC धारा 505/धारा 356 बीएनएस)। ये वे प्रावधान हैं जिनका पुलिस और अदालतें आमतौर पर सांप्रदायिक भाषण के मामलों में इस्तेमाल करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जोर दिया है कि कानूनी प्रतिबंध सटीक और अनुपातिक होने चाहिए।
● सर्वोच्च न्यायालय का नफरती भाषण पर कार्रवाई का दायित्व: शाहीन अब्दुल्ला और बाद के आदेश: शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ (2022) में, सर्वोच्च न्यायालय ने “नफरत के बढ़ते माहौल” को रेखांकित किया और पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे नफरती भाषण की घटनाओं में स्वतः संज्ञान लें - विशेष रूप से IPC की धारा 153A, 295A और 505 के तहत FIR दर्ज करने और जांच करने का आदेश दिया, बिना किसी निजी शिकायत के इंतजार किए। ये निर्देश बाद में सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों तक लागू किए गए। न्यायालय ने यह माना कि सक्रिय पुलिसिंग से ही संविधान के प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को सुरक्षित रखा जा सकता है। इस न्यायशास्त्र के तहत राज्य पुलिस पर जिम्मेदारी आती है: यदि सार्वजनिक वक्तव्य संभवतः नफरती भाषण का स्वरूप रखता हो, तो पुलिस को स्वतः ही उसकी जांच करनी चाहिए।
● संविधानिक सीमा: हिंसा भड़काने की मंशा और उससे प्रत्यक्ष संबंध: भारतीय न्यायालयों ने हमेशा संदर्भ-आधारित परीक्षण पर जोर दिया है। इसका एक प्रमुख उदाहरण है केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962), जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने देशद्रोह कानून को केवल उन्हीं मामलों में वैध ठहराया जहां शब्दों में “सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति या मंशा” हो या वे हिंसा के लिए उकसाते हों। केवल अपमानजनक या आलोचनात्मक अभिव्यक्ति को अपराध नहीं माना जा सकता। आधुनिक न्यायिक निर्णय भी इसी सिद्धांत को दोहराते हैं: किसी भाषण को दंडित करने के लिए राज्य को यह साबित करना होता है कि उस अभिव्यक्ति में या तो अवैध कृत्य करवाने की स्पष्ट मंशा थी या वह तत्काल और प्रत्यक्ष रूप से कानून तोड़ने की प्रवृत्ति रखता था - सिर्फ अप्रिय या उत्तेजक शब्दों के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह कठोर मानदंड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तीव्र राजनीतिक अभिव्यक्ति की रक्षा करता है, जबकि वास्तव में खतरनाक बयान को दंडित करने की गुंजाइश भी देता है।
कानूनी प्रावधानों को वास्तविक घटनाओं पर लागू करना : क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीमा लांघी?
यही वह महत्वपूर्ण और असहज प्रश्न है। आमतौर पर न्यायालय ताकतवर लोगों के राजनीतिक भाषण पर दो-चरणीय विश्लेषण लागू करते हैं:
● क्या भाषण की सामग्री में ऐसे तत्व हैं जो कानूनन अपराध की श्रेणी में आते हैं?
मुख्यमंत्री का भाषण केवल शासन संबंधी सामान्य बयानबाजी तक सीमित नहीं था। उन्होंने एक विशेष मौलाना और उनके समर्थकों को निशाना बनाया, जिससे परोक्ष रूप से एक पूरे धार्मिक समुदाय पर सामूहिक दोषारोपण का संकेत गया। “डेंटिंग-पेंटिंग” या “बरेली जैसी पिटाई” जैसे दंड और अपमान से जुड़े शब्द केवल आकस्मिक मेटाफर नहीं थे-इसने एक ऐसी दृश्य और ऐतिहासिक शैली को पुनर्जीवित किया जो राज्य की दमनकारी कार्रवाइयों से जुड़ी रही है। उत्तर प्रदेश की हालिया राजनीतिक शब्दावली में ये शब्द गहराई से जुड़े हैं - विशेष रूप से ध्वस्तीकरण अभियानों, पुलिस की पिटाई और ऐसी कार्रवाइयों के प्रतीक के रूप में जो मुस्लिम बस्तियों को असमान रूप से प्रभावित करती रही हैं।
इसके अलावा, यह कहना कि “आने वाली पीढ़ियों को सबक सिखाया जाएगा”, सामूहिक प्रतिशोध की एक स्पष्ट चेतावनी है, जो मौजूदा आरोपियों से आगे बढ़कर पूरे समुदाय को समय की धारा में साजा देने की मंशा को दर्शाती है। ऐसी भाषा मुसलमानों को कानून के अधीन नागरिक के रूप में नहीं, बल्कि एक स्थायी विरोधी वर्ग के रूप में प्रस्तुत करती है - एक ऐसा ‘पराया’ जिसके खिलाफ उदाहरण स्वरूप बल प्रयोग को न्यायसंगत ठहराया जा सके।
भारतीय दंड संहिता की धारा 153A (अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 196) और धारा 295A (अब बीएनएस की धारा 298) के तहत, किसी भाषण को आपराधिक ठहराने की कसौटी केवल खुले उकसावे पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह भी देखना होता है कि क्या वह भाषण नफरत को बढ़ावा देता है, किसी समुदाय को निशाना बनाता है, या सार्वजनिक शांति को भंग करने की संभावना पैदा करता है।
उत्तर प्रदेश में हाल ही की पुलिस कार्रवाइयों - जैसे मुस्लिम स्वामित्व वाली संपत्तियों का तोड़फोड़, हिरासत में हिंसक कार्रवाई और पक्षपातपूर्ण प्राथमिकी दर्ज करना - के संदर्भ में देखें तो मुख्यमंत्री के शब्दों को राज्य की भेदभावपूर्ण नीतियों के समर्थन और प्रोत्साहन के रूप में तर्कसंगत रूप से समझा जा सकता है।
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या, जैसे अमिश देवगन बनाम भारत संघ (2020) जैसे मामलों में, स्पष्ट करती है कि जब प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा ऐसे बयान दिए जाते हैं जो नफरत फैलाने की क्षमता रखते हैं, तो उकसावे की संभावना को केवल अलग से नहीं, बल्कि संदर्भ के अनुसार आंका जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से, योगी आदित्यनाथ के बयान प्रशासकीय दावे से आगे बढ़कर ऐसे भाषण बन जाते हैं जो भेदभाव को वैधता देते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं।
संक्षेप में, भले ही भाषण में सीधे हिंसा का आह्वान न हो, लेकिन यह एक ‘डॉग-व्हिसल’ (संकेतात्मक) भूमिका निभाता है: यह राज्य-समर्थित नफरत को सामान्य बनाता है और लक्षित धार्मिक समूह के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई की अनुमति का संकेत देता है। कानूनी दृष्टि से, यह भाषण आईपीसी की धाराओं 153A, 295A और 505(2) के तहत प्रारंभिक जांच के लिए उपयुक्त माना जा सकता है, विशेषकर वक्ता की संवैधानिक स्थिति और उसके बाद हुई हिंसा के प्रमाणित स्वरूप को देखते हुए।
● भाषण के बाद क्या बदला? (राज्य की कार्रवाई और न्यायसंगत सीमाएं)
संविधानिक मुद्दे केवल बोले गए शब्दों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उससे आगे की कार्रवाई में निहित होते हैं। जब मुख्यमंत्री की सार्वजनिक भाषा के तुरंत बाद प्रशासनिक कदम उठाए जाते हैं - बुलडोज़र चलाए जाते हैं, रातोंरात एफआईआर की संख्या बढ़ जाती है, और प्रभावित जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है - तब मामला केवल भाषण का नहीं, बल्कि भाषण द्वारा प्रेरित राज्य की शक्ति का होता है।
योगी आदित्यनाथ के भाषण के तुरंत बाद, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नगरपालिका और पुलिस प्रशासन ने अभियान चलाए: मुस्लिम युवाओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी, “अतिक्रमण” बताकर संपत्तियों का ध्वस्तीकरण और बड़े पैमाने पर इंटरनेट सेवा का निलंबन किया गया। ये केवल सामान्य कानून-व्यवस्था की कार्रवाई नहीं बल्कि बिना उचित नोटिस, सुनवाई या न्यायिक निरीक्षण के की गई बदले की एक योजनाबद्ध कार्रवाई थी।
न्यायालयों ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि कार्यपालिका की कार्रवाई उचित प्रक्रिया (due process) का विकल्प नहीं हो सकता। "बुलडोजर न्याय" (bulldozer justice) से संबंधित टिप्पणियों में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी आरोप के जवाब में यदि बिना नोटिस, जवाब देने का अवसर और नगर निगम कानूनों के पालन के बिना तुरंत तोड़फोड़ की जाती है, तो वह असंवैधानिक है (जमीयत उलमा-ए-हिंद बनाम उत्तर दिल्ली नगर निगम, 2022)। कानून एक स्पष्ट सीमा खींचता है कि शहरी नियोजन (urban planning) को दंडात्मक नाटक (penal theatre) के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं देखी गई - उग्र भाषण के तुरंत बाद कठोर कार्रवाई - वह यह संकेत देती है कि इसे कानून-व्यवस्था लागू करने के बजाय प्रतिशोध के इरादे से अंजाम दिया गया, जिसे कानून का अमल बताकर पेश किया गया।
शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ (2022) का सिद्धांत भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो पुलिस पर एक सकारात्मक दायित्व डाला गया है, उन्हें अभद्र भाषा के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, चाहे वक्ता का राजनीतिक कद कुछ भी हो। इस फैसले में इस बात पर जोर दिया गया है कि निष्क्रियता मौन सहमति के बराबर है और चुनिंदा कार्रवाई भेदभाव को और गहरा करता है। इस मामले में, कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कथित प्रदर्शनकारियों का तत्काल पीछा किया, लेकिन आईपीसी की धारा 153ए, 295ए और 505(2) के तहत स्पष्ट वैधानिक आधारों के बावजूद, मुख्यमंत्री की भड़काऊ टिप्पणियों पर कार्रवाई करने में विफल रहीं।
संवैधानिक अनुपातिकता के सिद्धांत (doctrine of proportionality) के अनुसार, प्रशासनिक कार्रवाइयां तभी वैध मानी जाती हैं जब उनका किसी वैध उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध हो, वे न्यूनतम प्रतिबंधात्मक उपाय अपनाएं, और उनका प्रभाव भेदभावपूर्ण न हो। परंतु मुख्यमंत्री के भाषण के बाद जो कार्रवाइयां हुईं-जैसे कि मुस्लिम-बहुल इलाकों में तोड़फोड़, विशेष समुदाय के युवाओं पर पुलिस छापे और आत्मघोषित ‘रक्षक’ समूहों की जवाबदेही की पूरी तरह अनुपस्थिति-वे इन संवैधानिक मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन लगती हैं। यह सब एक संतुलित और लक्षित कानून-प्रवर्तन के बजाय एक सामूहिक दंड की तैयार रणनीति की ओर संकेत करता है जो न केवल न्याय के सिद्धांतों का हनन है बल्कि लोकतंत्र और समानता के मूल मूल्यों के भी विपरीत है।
जैसा कि कई विश्लेषकों ने उल्लेख किया है, जब कार्यपालिका की भाषा एक संकेत के रूप में कार्य करती है और नौकरशाही तंत्र उस संकेत के जवाब में दमनात्मक अतिक्रमण करता है, तब राजनीतिक बयानबाजी और राज्य की वैधानिक स्वीकृति के बीच की सीमा ध्वस्त हो जाती है। ऐसे में राज्य एक निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका छोड़कर अपने ही नैतिक तमाशे का अभिनेता बन जाता है, जहां कानून का पालन कराने की बजाय वह भय के जरिए अनुशासन और प्रतिरोध का दमन प्रदर्शित करता है।
योगी आदित्यनाथ के भाषण को अगर अकेले राजनीतिक अभिव्यक्ति के तौर पर देखा जाए तो वह सुरक्षित ठहराया जा सकता है, लेकिन इसके बाद हुई घटनाओं की तेजी -जैसे तत्काल गिरफ्तारियां, व्यापक स्तर पर एफआईआर दर्ज करना और दंड स्वरूप संपत्तियों की तोड़फोड़-स्पष्ट करती है कि राज्य की ताकत न्याय के बजाय एक सशक्त राजनीतिक संदेश देने के लिए इस्तेमाल की गई। यह मामला संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत गंभीर संवैधानिक सवाल खड़ा करता है, हालांकि भाषण के सीधे आपराधिक दायित्व को साबित करना कानूनी रूप से जटिल है।
वास्तविक स्थिति: कठोर कार्रवाई और उसके समुदाय पर प्रभाव के सबूत
बरेली हिंसा के बाद की घटनाएं केवल पारंपरिक कानून-व्यवस्था के दायरे में नहीं रुकतीं, बल्कि यह एक बहु-स्तरीय दबावकारी राज्य शक्ति के प्रयोग का दर्शाती हैं। यह शक्ति मुख्यमंत्री के भाषण के तुरंत बाद सक्रिय हुई और औपचारिक तथा अनौपचारिक दंड के माध्यम से निरंतर जारी रखी गई।
● सामूहिक गिरफ्तारियां और बड़े पैमाने पर एफआईआर: बरेली और आस-पास के जिलों में तुरंत बाद पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई। खबरों में बताया गया कि कुछ ही घंटों में दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया और सैकड़ों-कभी-कभी तो हजारों-लोगों के नाम एफआईआर में शामिल किए गए। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, कई थानों में लगभग 2,000 लोगों के नाम दर्ज हुए, हालांकि अलग-अलग स्रोतों में संख्या में फर्क था। इन एफआईआर में अक्सर बड़े-बड़े और आम आरोप थे, जिससे ये सवाल उठते हैं कि क्या पुलिस सबको एक साथ दोषी ठहरा रही है और रोकथाम के नाम पर लोगों को डराने-धमकाने के लिए पकड़ रही है, ना कि सही तरीके से जांच कर रही है।
● संपत्तियों की सीलिंग और तोड़फोड़: नगरपालिका और विकास प्राधिकरणों ने आरोपियों से जुड़ी बताई गई संपत्तियों-जैसे कि एक बैंक्वेट हॉल और अन्य व्यावसायिक इमारतों-के खिलाफ तेजी से तोड़फोड़ और सीलिंग अभियान चलाए। परिवारों ने शिकायत की कि उन्हें कोई पूर्व सूचना या सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, जिसके कारण उन्होंने उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग से शिकायत की। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, ये कदम राज्य की बुलडोजर से जुड़ी दंडात्मक कार्रवाइयों की हालिया प्रवृत्ति की पुनरावृत्ति हैं, जिन्हें मानवाधिकार समूह ‘दिखावटी बदला’ मानते हुए आलोचना करते रहे हैं जो नियमों के पालन की बजाय दबदबे का संदेश देने के लिए किए जाते हैं। सांप्रदायिक घटनाओं के तुरंत बाद इस तरह की तोड़फोड़ यह संकेत देती है कि अपराधी उत्तरदायित्व को संपत्ति के स्वामित्व और समुदाय की पहचान से जोड़कर एक जानबूझकर मिलान किया जा रहा है।
● प्रशासनिक और नियामक जवाबी कार्रवाई: पुलिस की कार्रवाई के साथ-साथ प्रशासन ने भी कई “पूरक दंडात्मक कार्रवाई” किए-जिनमें बिजली चोरी के नोटिस, आय वसूली के दावे और प्रदर्शन के केंद्र में रहे मौलवी से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ नियामक प्रतिबंध शामिल थे। ये अर्ध-नागरिक दंड प्रभावित परिवारों पर आर्थिक और मानसिक बोझ को और बढ़ा गए। ये सभी कदम अलग-अलग तो कानूनी हो सकते हैं, लेकिन एक साथ मिलकर ये कार्रवाई अनुपातहीन और बोझिल दंड के रूप में दिखती है, जो नौकरशाही उपकरणों के जरिए लगातार दंडित करने की रणनीति का हिस्सा लगती है।
● इंटरनेट बंद करना: अफवाहें फैलने और लोगों के इकट्ठा होने को रोकने के लिए अधिकारियों ने बरेली जिले में 48 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और मैसेजिंग सेवाएं बंद कर दीं। द इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, यह हाल के कई उदाहरणों में से एक है जहां सांप्रदायिक तनाव के समय इंटरनेट बंद करना प्रशासन की आम प्रतिक्रिया बन गया है। हालांकि ये कदम सावधानी के नाम पर लिए जाते हैं, पर अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) के फैसले के अनुसार, इस तरह के प्रतिबंध केवल सीमित समय के लिए और विशेष रूप से आवश्यक होने पर ही लगाना चाहिए, साथ ही समय-समय पर समीक्षा भी होनी चाहिए।
● सामाजिक प्रभाव और बहिष्कार की प्रवृत्तियां: घटनाओं के बाद समाज में भी गहरा असर देखने को मिला। सिविल सोसायटी और मीडिया, जैसे कि LiveMint, ने रिपोर्ट किया कि उस घटना के बाद सामाजिक सीमाओं में स्पष्ट सख्ती आ गई। बताया गया कि मुस्लिम समुदाय पर गरबा और अन्य सार्वजनिक उत्सवों में हिस्सा न लेने का दबाव डाला गया और कुछ जगहों पर हिन्दुत्ववादी समूहों ने सांस्कृतिक आयोजनों में मुस्लिमों की मौजूदगी पर निगरानी रखने या उन्हें बाहर करने की कोशिश की। भले ही इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो, लेकिन ये घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे प्रशासनिक बयान और कड़ी कार्रवाई मिलकर समुदायों के बीच बहिष्कार को वैधता देते हैं और रोजमर्रा के सामाजिक संबंधों में राज्य समर्थित पक्षपात को गहराते हैं।
कुल मिलाकर देखें तो ये घटनाएं सिर्फ कानून-व्यवस्था का एक अलगाव नहीं बल्कि एक सुनियोजित क्रम दर्शाती हैं: बयानबाजी, दमन, और सामाजिक दंड। भाषण, कार्रवाई, प्रदर्शन और बहिष्कार का यह चक्र शासन का एक विशेष मॉडल बन जाता है-जहां प्रशासनिक कदम राजनीतिक मंचन बन जाता है और दंड सार्वजनिक संदेश का एक जरिया।
सख्त बयानबाजी की राजनीति: भाषण से सत्ता तक का सफर
चाहे यह सोची-समझी रणनीति हो या अनजाने में हुआ असर, योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं के कड़े सार्वजनिक बयान राजनीतिक हाशिए पर काम करने वाले बहुलवादी या विजिलेंट समूहों के लिए तीन बड़े फायदे लेकर आते हैं। ये भाषण को कार्रवाई में बयानबाजी को वैधता में और जबरदस्ती को तमाशे में बदल देते हैं।
1. विजिलेंट पुलिसिंग को अप्रत्यक्ष मंजूरी: जब सरकार का बड़ा अधिकारी खुलेआम सख्त कार्रवाई का वादा करता है और बदले की बातें करता है-जैसे “डेंटिंग और पेंटिंग करना” या “हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं”—तो ये बात सिर्फ सरकारी दफ्तर तक सीमित नहीं रहती। इससे स्थानीय लोग, विजिलेंट ग्रुप और अपने जैसे सोच वाले इसे कार्रवाई का संकेत समझ लेते हैं। ये लोग इसे ‘नागरिक पुलिसिंग’ या धर्म और देश की रक्षा के नाम पर लोगों को डराने-धमकाने का सही ठहराव मान लेते हैं। सिविल सोसायटी की रिपोर्ट्स में भी दिखता है कि ऐसे बयान आने के बाद हिंदुत्ववादी संगठन मुस्लिमों की गरबा या जुलूस जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा देते हैं। इस तरह की बातों से विजिलेंट बनने की हिम्मत बढ़ती है और लोग सोचते हैं कि उन्हें सत्ता की छूट मिली है।
2. नैरेटिव पर नियंत्रण और उलटफेर: नेता के बयान घटनाओं की नैतिक कड़ी को भी बदल देते हैं। जैसे “I Love Muhammad” जैसे भावनात्मक या धार्मिक कामों को “उकसावे” के तौर पर पेश किया जाता है, जिससे राज्य खुद को व्यवस्था का निष्पक्ष रक्षक दिखाता है और प्रदर्शनकारियों को समस्या पैदा करने वाला बताता है। इस तरह की कहानी उलटफेर से किसी समुदाय के धर्म का प्रदर्शन कानून-व्यवस्था की समस्या बन जाता है, जिससे प्रशासन को बिना ज्यादा विरोध के दमन करने का मौका मिल जाता है।
जैसा कि The Wire और अन्य आलोचनात्मक मीडिया ने रिपोर्ट किया है, मीडिया की फ्रेमिंग बहुत अहम भूमिका निभाती है। वे चैनल जो “दंगों” और “अनुशासन” को प्रमुखता देते हैं, वे सरकार की पसंदीदा नैरेटिव को बढ़ावा देते हैं, जबकि जो लोग उचित प्रक्रिया या अत्यधिक सख्ती पर सवाल उठाते हैं, उन्हें “अव्यवस्था के प्रति नरम” कहकर किनारे कर दिया जाता है। इसका नतीजा एक ऐसा चक्र बनना है जहां राजनीतिक बयान और मीडिया की रिपोर्टिंग मिलकर सरकार की वैधता को मजबूत करते हैं।
3. चुनावी संकेत और समर्थन जुटाने की रणनीति: तत्काल प्रशासनिक इस्तेमाल से परे, कड़े बयानों का काम राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करना होता है जो खासतौर पर एक राजनीतिक वर्ग को ध्यान में रखकर किया जाता है। बुलडोजर की तस्वीरें, तेज गिरफ्तारियां और सामूहिक दंड एक निर्णायक शासन का तमाशा बन जाते हैं, जो नियंत्रण और दबदबे का संदेश देते हैं। साउथ एशियन पोपुलिज्म के शोधकर्ताओं ने बताया है कि ये सख्त कार्रवाई “सजात्मक लोकलुभावनवाद” कहलाती है, जो बहुसंख्यकों को भरोसा दिलाने के लिए न्याय प्रणाली को एक भावनात्मक साधन बना देती है। हर कार्रवाई राजनीतिक पहचान को मजबूत करने का हिस्सा बन जाती है, जिससे कानून-व्यवस्था और चुनावी प्रदर्शन के बीच की हदें मिट जाती हैं।
कुल मिलाकर देखें तो ये तीनों पहलू-बयानबाजी, मीडिया और कार्रवाई-कैसे मिलकर बहुसंख्यक सत्ता का एक पूरा तंत्र बनाते हैं। इस मॉडल में दंड सिर्फ लागू नहीं होता, बल्कि उसे प्रदर्शन के तौर पर दिखाया जाता है, टीवी पर दिखाया जाता है और चुनावों में वोट भी मिलता है।
जवाबदेही के अंतराल और कानूनी उपाय
बरेली की घटना के बाद सिर्फ टिप्पणी करना काफी नहीं है बल्कि जवाबदेही भी जरूरी है। जब सरकारी बयान, प्रशासनिक कार्रवाई और मीडिया प्रचार मिलकर दबाव वाली कार्रवाई करते हैं, तो संविधान व्यवस्था को उचित सुधार सुनिश्चित करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की मान्यताओं और मानवाधिकार प्रथाओं के आधार पर निम्नलिखित कानूनी और संस्थागत प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं:
1. मुख्यमंत्री के भाषण पर शाहीन अब्दुल्ला निर्देशों के तहत स्वतः संज्ञान: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस पर नफरत भरे भाषणों के मामलों में स्वतः FIR दर्ज करने की निरंतर जिम्मेदारी है, चाहे वक्ता किसी भी राजनीतिक पद पर हो। उच्च पदस्थ अधिकारियों के संभावित उकसावे वाले बयान पर कार्रवाई न करना कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना माना जाएगा। अगर अभी तक कोई जांच शुरू नहीं हुई है, तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अनुपालन के लिए आवेदन करना कानूनी रूप से सही होगा।
2. तोड़-फोड़ और सीलिंग अभियानों की मनमानी और अनुचित कठोरता पर न्यायिक समीक्षा: सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में “बुलडोजर न्याय” पर दिए अपने निर्णय में साफ कहा है कि तत्काल सजा के तौर पर की गई तोड़-फोड़ उचित प्रक्रिया का उल्लंघन है। प्रभावित हर व्यक्ति को पहले से सूचना मिलने, अपनी बात रखने और स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा का अधिकार होता है, इससे पहले कि उनकी संपत्ति पर कोई कार्रवाई हो। जब नगरपालिका या डेवलपमेंट अफसर सांप्रदायिक घटनाओं के तुरंत बाद ऐसी कार्रवाइयां करते हैं, तो उन तोड़-फोड़ को वैध शहरी नियमन की बजाय दंडात्मक कार्रवाई के रूप में देखकर न्यायालयीय जांच की जरूरत होती है।
3. मानवाधिकार शिकायतें और जनहित याचिकाएं जो पूरे घटनाक्रम को दर्ज करें: कानपुर में दर्ज एफआईआर से लेकर बरेली में हुई झड़पों, मुख्यमंत्री के भाषणों और प्रशासनिक दमन तक की पूरी टाइमलाइन अपने आप में राज्य की मनमानी और चयनात्मक कार्रवाई का अहम सबूत बनती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), राज्य मानवाधिकार आयोग या संबंधित हाईकोर्ट में की गई शिकायतों और याचिकाओं के जरिए स्वतंत्र जांच, पीड़ितों को मुआवजा और रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की जा सकती है। पहले के उदाहरण दिखाते हैं कि इस तरह की याचिकाओं ने न सिर्फ राज्य को जवाब देने के लिए मजबूर किया है बल्कि कई बार दमनात्मक कार्रवाई पर रोक भी लगवाई है।
4. मीडिया की जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग: चूंकि टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दंडात्मक बयानों को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए पारदर्शिता के उपाय बेहद जरूरी हैं। ब्रॉडकास्ट चैनलों और सोशल मीडिया कंपनियों को चाहिए कि वे अपने सभी फुटेज, थंबनेल और मेटाडेटा को सुरक्षित रखें ताकि भविष्य में जांच की जा सके। जिन मीडिया आउटलेट्स ने सनसनीखेज प्रोमो या भ्रामक हेडलाइन का इस्तेमाल किया है, उनसे NBDSA (न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी) के तहत स्पष्टीकरण या सुधार जारी करने की मांग की जा सकती है। साथ ही, पुलिस और स्थानीय प्रशासन को यह सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए कि सामूहिक FIR, तोड़फोड़ आदेश और इंटरनेट बंदी का कानूनी आधार क्या था। इस तरह की पारदर्शिता, बिना रोक-टोक के हो रही कार्यपालिका की सख्ती पर लगाम लगाने की दिशा में पहला कदम बन सकती है।
निष्कर्ष - कानूनी जोखिम और लोकतांत्रिक कीमत
बरेली की "I Love Muhammad" विवाद और उसके बाद की घटनाएं आज के भारत में सत्ता और अभिव्यक्ति के टकराव के एक बेहद अहम मोड़ पर खड़ी हैं। जो शुरुआत में एक अभिव्यक्तिपूर्ण क़दम था -एक नारा, एक बैनर, या धार्मिक पहचान की पुष्टि -वह राजनीतिक और प्रशासनिक ताकत के दबाव में जल्दी ही "उकसावे" की नैरेटिव बना दी गई और फिर उसे राज्य की दंडात्मक कार्रवाइयों की एक कड़ी में बदल दिया गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बयानबाजी महज़ चेतावनी तक सीमित नहीं रही -बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने राज्य की सख्त कार्रवाइयों के लिए एक तरह का कानूनी और नैतिक आधार तैयार किया। ऐसे कदम -जैसा कि विश्वसनीय रिपोर्टों में सामने आया -प्रक्रियात्मक नियमों को पीछे छोड़ते हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को खतरे में डालते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी को दबाते हैं और आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन को अस्त-व्यस्त कर देते हैं। हालांकि ऐसे मामलों में कानूनी राहत पाना मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। हमारे संविधान की व्यवस्था, विधिक प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट की पहले की गई टिप्पणियां ऐसे अतिक्रमणों को चुनौती देने का स्पष्ट आधार प्रदान करती हैं।
इस लिहाज से बरेली की घटना सिर्फ एक स्थानीय मामला नहीं है बल्कि यह एक पड़ताल की घड़ी है। अगर न्याय व्यवस्था, सिविल सोसायटी और मीडिया मिलकर भाषण और उसके बाद की कार्रवाई की गंभीर जांच करने में असफल रहते हैं, तो जो उदाहरण बनता है वह बेहद खतरनाक होगा: ऐसा राजनीतिक भाषण जो पहचान, आस्था, दंडात्मक वादा और तमाशे को घालमेल कर देता है, तो वह हाशिए पर डालने का एक लाइसेंस बन जाता है। लोकतंत्र ऐसे मौकों पर तभी टिक सकता है जब “कानून-व्यवस्था” और राज्य की मनमानी कार्रवाई के बीच की वह बारीक व अदृश्य रेखा भी उतनी ही गंभीरता से जांची जाए जितनी हम किसी खुले विरोध प्रदर्शन की करते हैं।
References
https://www.livelaw.in/top-stories/take-suo-motu-action-against-hate-spe...
https://www.indiatoday.in/india/story/what-is-i-love-muhammad-row-and-wh...
https://timesofindia.indiatimes.com/city/meerut/bareilly-cleric-among-8-...
https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/i-love-muhammad-row-up-...
https://economictimes.indiatimes.com/news/india/internet-suspended-in-ba...
https://www.livemint.com/news/india/yogi-adityanath-warns-i-love-mohamma...
https://thepolisproject.com/research/sc-verdict-demolitions-statecraft/
https://thewire.in/politics/i-love-muhammad-banner-controversy-how-routi...
https://www.scobserver.in/journal/bulldozer-demolitions-remind-of-a-lawl...
https://timesofindia.indiatimes.com/city/meerut/i-love-muhammad-row-plea...
https://timesofindia.indiatimes.com/city/bareilly/i-love-muhammad-row-rs...
https://theloop.ecpr.eu/bulldozer-justice-punitive-populism-in-india/
https://indianexpress.com/article/cities/lucknow/i-love-muhammad-row-cle...
https://theprint.in/politics/cleric-who-once-said-modi-should-learn-from...
https://kmsnews.org/kms/2025/09/20/muslims-protest-across-india-against-...
https://sabrangindia.in/register-prosecute-hate-speech-offences-promptly...
https://sabrangindia.in/hate-crime-hate-speech-scs-scrutiny-continue
https://sabrangindia.in/free-speech-even-in-bad-taste-is-protected-if-no...
https://www.toaep.org/pbs-pdf/138-lokur-damojipurapu
https://timesofindia.indiatimes.com/india/tension-in-bareilly-drones-are...
https://timesofindia.indiatimes.com/india/one-can-say-i-love-modi-but-no...
https://timesofindia.indiatimes.com/india/i-love-mohammad-march-violence...
https://cjp.org.in/bns-2023-does-nothing-to-bring-in-a-nuanced-effective...
https://cjp.org.in/cjp-files-complaints-against-the-hate-speeches-delive...
https://cjp.org.in/the-sentinel-and-the-shift-free-speech-in-the-supreme...
https://thelogicalindian.com/chedhoge-to-chodhenge-nahi-yogi-adityanaths...
https://www.ndtv.com/india-news/internet-cut-for-48-hours-in-ups-bareill...
https://article-14.com/post/govt-whataboutery-inaction-why-hate-speech-p...



